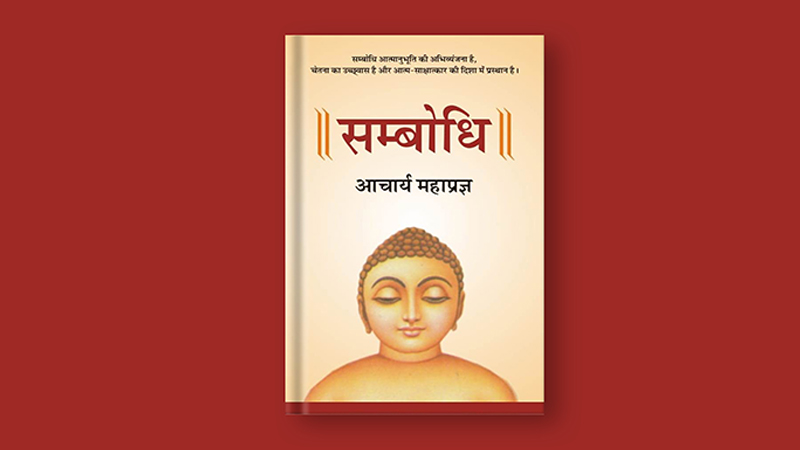
संस्थाएं
संबोधि
गीता का अनासक्ति योग और जैन के अनासक्त योग में साम्य नहीं है। अनासक्तिपूर्वक किया गया कोई भी और कैसा भी कार्य बंधन-रहित है, यह जैन धर्म को स्वीकार नहीं है। स्थितप्रज्ञ और अनासक्त के लक्षणों को देखने से लगता है, वह एक उच्च सीमा की अनासक्ति है, जहां राग, द्वेष, मोह आदि को स्थान नहीं है। मन और इन्द्रियों का भी बहिर्मुखता में अवकाश नहीं है। आत्मा क्रमशः स्वयं में ही विलीन हो जाती है। 'परमाप्नोति पुरुषः' आत्मा परमात्मा बन जाती है। परमात्मदशा वीतराग दशा है, वहां कर्म का प्रवाह मंदतम होता है। शरीर-त्याग की स्थिति में वह सर्वथा रुक जाता है।
२६. सम्यग्दृष्टेरिदं सारं, नानर्थ यत्प्रवर्तत।
प्रयोजनवशाद् यत्र, तत्र तद्वान्न मूच्छति।।
सम्यग्दृष्टि बनने का यह सार है कि वह अनर्थ प्रयोजन बिना प्रवृत्ति नहीं करता और प्रयोजनवश जो प्रवृत्ति करता है, उसमें भी सम्यग्दृष्टि वाला आसक्त नहीं होता।
२७. सम्मतानि समाजेन, कुर्वन् कर्माणि मानसम्।
अनासक्तं निदधीत, स्याल्लेपो न यतो दृढः॥
समाज द्वारा सम्मत कर्म को करता हुआ व्यक्ति मन को अनासक्त रखे, जिससे वह उसके दृढ़ लेप से लिप्त न हो।
२८. अविरतिः प्रवृत्तिश्च, द्विविधं बन्धनं भवेत्।
प्रवृत्तिस्तु कदाचित् स्यादविरतिर्निरन्तरम्।।
बंधन के दो प्रकार हैं-अविरति और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति कभी-कभी होती है, अविरति निरंतर रहती है।
२९. दुष्प्रवृत्तिमकुर्वाणो, लोकः सर्वोऽप्यहिंसकः।
परन्त्वविरतेस्त्यागान्, मानवः स्यादहिंसकः।।
दुष्प्रवृत्ति नहीं करने वाला यदि अहिंसक हो तो सारा संसार ही अहिंसक हो सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति निरंतर दुष्प्रवृत्ति नहीं करता। परन्तु अहिंसक वह होता है, जो अविरति का त्याग करे अर्थात् कभी और किसी प्रकार की हिंसा न करने का दृढ़ संकल्प करे।
३०. दुष्प्रवृत्तः क्वचित् साधुर्नाऽव्रती स्यान्मुनिः क्वचित्।
सत्प्रवृत्तोऽपि नो साधुव्रती जायते क्वचित्॥
साधु कहीं-कहीं प्रमादवश दुष्प्रवृत्त हो सकता है पर अव्रती कहीं भी मुनि नहीं हो सकता। अव्रती सत्प्रवृत्ति करने पर भी कभी साधु नहीं बनता। अनासक्ति और आसक्ति के परिणामों के कर्मफल में भेद होता है। लेकिन प्रश्न यह होता है कि अनासक्त व्यक्ति के बंधन का हेतु क्या है, जबकि वह निःस्वार्थ वृत्ति से कार्य करता है। बंधन का मुख्य हेतु है अविरति। हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह की सूक्ष्म या स्थूल जो प्रवृत्ति है या अत्यागवृत्ति है उसका नाम अविरति है। व्यक्ति जब तक अविरति से मुक्त नहीं होता तब तक कर्म का आगमन निरुद्ध नहीं होता।
अविरति आत्मा की बहिर्दशा है और विरति अंतर्दशा। विरत व्यक्ति किसी भी परिस्थिति, में हिंसा आदि न करता है, न कराता है और न करते हुए व्यक्तियों का अनुमोदन ही करता है। हिंसा आदि कार्यों में व्यक्ति अनवरत प्रवृत्त नहीं रहता, किन्तु अविरति का प्रवाह सतत चलता रहता है। तन्द्रा और मूर्च्छित स्थिति में भी वह बंद नहीं होता। प्रवृत्ति को ही यदि हिंसा आदि का कारण मानें तो वह सबके सदा नहीं होती। व्यक्ति उसके अभाव में अहिंसक बन सकता है। यह स्थूल सत्य है, वास्तविक नहीं। सूक्ष्म सत्य वही है जहां अविरति का त्याग है। अविरति के त्याग में सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही प्रवृत्तियां विशुद्ध हो जाती हैं।

