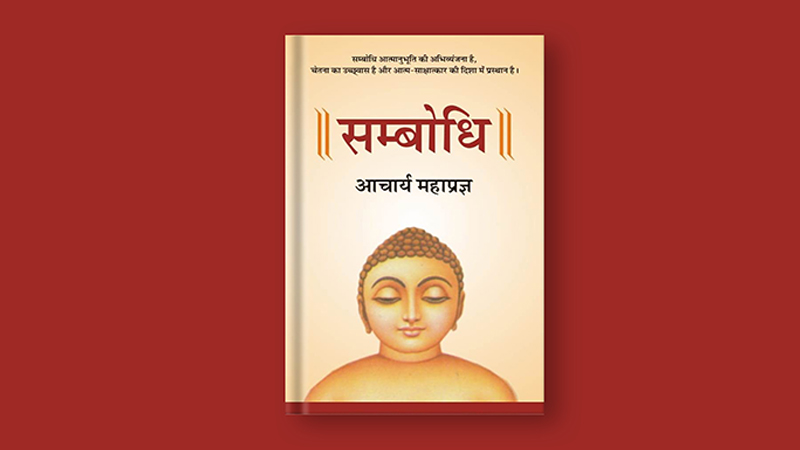
स्वाध्याय
संबोधि
श्रमण-भूत
यह ग्यारहवीं प्रतिमा है। इसका कालमान ग्यारह महीनों का है। इसमें पूर्वोक्त उपलब्धियों के अतिरिक्त प्रतिमाधारी उपासक सिर को क्षुर से मुंडवा लेता है या लुंचन करता है। वह साधु का वेश धारण कर ईर्यासमिति आदि साधु-कर्मों का अनुपालन करता हुआ विचरण करता है। वह भिक्षा के लिए गृहस्थों के घरों में प्रवेश कर 'प्रतिमा सम्पन्न श्रमणोपासक को भिक्षा दो' ऐसा कहता है। यदि कोई उससे पूछे कि 'तुम कौन हो?' तो वह यह कहता है-'मैं प्रतिमा सम्पन्न श्रमणोपासक हूं।'
प्रायः वे लोग इनका स्वीकरण करते हैं :
१. जो अपने आपको श्रमण बनने के योग्य नहीं पाते किन्तु जीवन के अंतिम काल में श्रमण-जैसा जीवन बिताने के इच्छुक होते हैं।
२. जो श्रमण जीवन बिताने का पूर्वाभ्यास करते हैं।
साधक गृहस्थ जैसे-जैसे अपने साधना अभ्यास में सफल, प्रसन्न और आनंदित हो जाता है वैसे-वैसे ममत्व, आसक्ति और भ्रांति के क्षीण होने पर सत्य की दिशा में तीव्रगति से बढ़ने को आतुर हो जाता है। साध्य-धर्म के अतिरिक्त फिर उसका मन अन्यत्र रमण नहीं करता। वह चलता है-मंजिल, लक्ष्य को प्राप्त करना। इस दृष्टि से जो कुछ बाह्य रूप में स्वीकृत किया था अब उसे प्रत्यक्ष अनुभूति के रूप में देखना चाहता है। अनुभूति समय सापेक्ष है। प्रतिमाओं के अभ्यास-काल में बाह्य क्रियाओं से निवृत्त होकर वह सत्य की आराधना में जीवन समर्पित करता है और सारा समय साधना की प्रक्रियाओं में योजित करता है। सफलता समय, श्रद्धा, धैर्य और निरंतरता पर आधारित है।
आनंद श्रावक भगवान् का प्रमुख उपासक था। उसने चौदह वर्षों तक बारहव्रती का जीवन बिताया। पन्द्रहवें वर्ष के अंतराल में एक दिन उसके मन में धर्म-चिंता उत्पन्न हुई और वह आत्मा या सत्य की खोज तथा उसके लिए समर्पित जीवन बिताने के लिए कृतसंकल्प हुआ। दूसरे दिन अपने ज्येष्ठपुत्र को घर का भार सौंपकर भगवान् महावीर के पास उपासक की ग्यारह प्रतिमाएं स्वीकारं कर लीं। इनके प्रतिपूर्ण पालन में साढ़े पांच वर्ष लगे। तत्पश्चात् उसने अपश्चिम-मारणांतिक संलेखना की और अंत में एक मास का अनशन किया।
उपासक आनंद के इस वर्णन से यही फलित होता है कि उपासक की ग्यारह प्रतिमाओं का स्वीकरण जीवन के अंतिम भाग में किया जाता था। उसकी पूर्व-भूमिका के रूप में वर्षों तक बारह व्रतों का पालन करना होता था और ये प्रतिमाएं भावी अनशन के लिए भी पृष्ठभूमि बनाती थीं।
४३. असंयमं परित्यज्य, संयमस्तेन सेव्यताम्।
असंयमो महद् दुःखं, संयमः सुखमुत्तमम् ।।
इसलिए असंयम को छोड़कर संयम का सेवन करना चाहिए। असंयम महान् दुःख है। संयम उत्तम सुख है।
असंयम बहिर्मुखता है और संयम स्व-मुखता (अंतर्मुखता) है। स्वभाव संयम है और विभाव असंयम। आत्म-विस्मृति असंयम है और आत्मस्मृति संयम। दुःख विस्मृति है और सुख स्व-स्मृति। जिसे सुख प्रिय है उसे संयम प्रिय होना चाहिए। संयम का फल सुख है और असंयम का दुःख। संयम के सिवाय सुख की आकांक्षा करना मृग मरीचिका में पानी की तलाश करना है। बाहर से सुख नहीं मिला, किंतु सुखाभास अवश्य मिलता है। मनुष्य उसी सुखाभास में मुग्ध होकर पुनः पुनः दुःख, अशांति और कष्टों का अनुभव करता चला जा रहा है। इसीलिए महावीर कहते हैं अपने अंतश्चक्षुओं को उद्घाटित कर देखो, यहां क्या मिला है? यदि दुःख के सिवा कुछ नहीं मिला तो अब उसे छोड़कर सत्य के पथ का अनुसरण करो।
इति आचार्यमहाप्रज्ञविरचिते संबोधिप्रकरणे
गृहस्थधर्मप्रबोधननामा चतुर्दशोऽध्यायः ।

