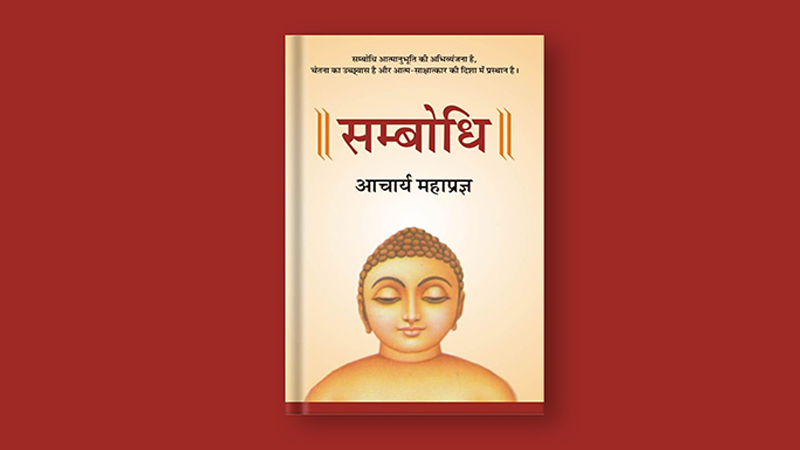
स्वाध्याय
संबोधि
धर्म जीवन का एक आवश्यक अंग है। इसे जो भूलता है, वह अपने आपको भूलता है। जीवन के लिए अन्य कार्य आवश्यक हैं, वैसे धर्म भी। जो इसे जानता है और विश्वास करता है, वह धर्म का आचरण भी करता है। धर्म केवल जानने का ही विषय नहीं है, वह आचरण का भी विषय है। प्रत्येक कार्य में धर्म को सामने रखा जाए तो मनुष्य अनैतिक और अधार्मिक नहीं हो सकता।
आत्मा का एक शरीर में नियत-वास नहीं है। आस्तिक इसे स्वीकार करते हैं इसलिए वे यह भी स्वीकार करते हैं कि हिंसा किसी अन्य की नहीं, अपनी ही होती है। हिंसा के निमित्त हैं-राग, द्वेष, मोह, प्रमाद आदि।
श्रुत और आचार की उपासना आत्म-धर्म है। श्रुत और आचार से भिन्न धर्म कर्त्तव्य और स्वभाव की दृष्टि से है। आत्म-विकास में वे सहयोगी नहीं बनते। मोक्ष श्रुत और आचरण का योग है। आत्मा का विकास इन्हीं के द्वारा होता है। इस अध्याय में ये ही विवेच्य विषय हैं।
भगवान् प्राह
१. यावद् देहो भवेत् पुंसां, तावत्कर्मापि जायते।
कुर्वन्नावश्यकं कर्म, धर्ममप्याचरेद् गृही॥
भगवान् ने कहा-जब तक मनुष्य के शरीर होता है तब तक
क्रिया होती है। आवश्यक क्रिया को करता हुआ मनुष्य धर्म का भी आचरण करे।
'किं कर्म किमकर्म च कवयोप्यत्रमोहिताः।' गीता में कहा है-'कर्म क्या है और अकर्म क्या है? इस निर्णय में बड़े-बड़े विद्वान भी मूढ़ हो जाते हैं।' कर्म वस्तु का स्वभाव है। जो स्वभाव है वह किया नहीं जाता, प्रतिक्षण होता रहता है। इसलिए उसे अकर्म-अक्रिया कहा जाता है। अकर्म को कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। 'अकम्मुणा कम्म खवेंति धीरा' धीर व्यक्ति अकर्म के द्वारा कर्म (विजातीय) को नष्ट कर स्वभाव में प्रतिष्ठित होते हैं। कुछ कर्म निषिद्ध हैं और कुछ विहित, किन्तु अकर्म की दृष्टि से दोनों ही अविहित हैं। अकर्म की स्थिति प्राप्त न हो तब विहित कर्म व्यक्ति करता है, किन्तु जो अकर्म के मर्म को जानता है वह कर्म करता हुआ भी अकर्म रहता है। सामान्यतया यह कठिन है। मनुष्य कर्म करता है अकर्म को भूलकर। कर्तृत्व का अहंकार और बाह्य प्रेरणाएं कर्म के लिए प्रेरित करती है। जिसे अकर्म का बोध नहीं है, वह कर्म के फल से भी सहजतया मुक्त नहीं हो सकता। यश, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि में वह प्रसन्न हो जाता है और विपरीत में अप्रसन्न। अहंकार को रस प्रदर्शन में आता है, अपनी विशिष्टता का बोध दूसरों को हो वह बताना चाहता है। अकर्म का साधक कर्म में रस नहीं लेता। वह सिर्फ अपने को एक निमित्त समझेगा और कर्म का साक्षी, द्रष्टा रहेगा। अकर्म की साधना है-आप स्वयं कुछ करें नहीं, आप सिर्फ जो पीछे अकर्मक खड़ा है, उसे देखते रहें। जेन साधक लिंची ने अपने शिष्यों से कहा अगर चित्र बनाने में तुम्हें जरा भी श्रम मालूम पड़े तो समझना अभी कलाकार नहीं हुए हो। जिस दिन श्रम का पता न लगे उसी दिन कलाकार बनोगे।'
जर्मन विचारक हैरीगेली धनुर्विद्या सीखने जापान आया। तीन साल श्रम किया। अचूक निशानेबाज हो गया। फिर भी गुरु ने कहा-अभी कुछ नहीं हुआ। अभी तू चलाता है, तीर चलता नहीं। थक गया। कहा-अब मैं आज जाता हूं। उसने घर जाने की सब तैयारी कर ली। विदा लेने आया। गुरु सिखा रहे थे। बैठ गया। अचानक उठा और तीर उठाकर चल दिया। गुरु ने कहा-हो गया काम। इतने दिन प्रयत्न में था, आज अप्रयत्न में।' साधक के लिए यह बहुत बड़ा पाठ है जो उसे पढ़ना है।
२. यथाहारादि कर्माणि, भवन्त्यावश्यकानि च।
तथात्माराधनं चापि, भवेदावश्यकं परम्॥
जिस प्रकार भोजन आदि क्रियाएं आवश्यक होती हैं, उसी प्रकार आत्मा की साधना करना भी अत्यंत आवश्यक है।

