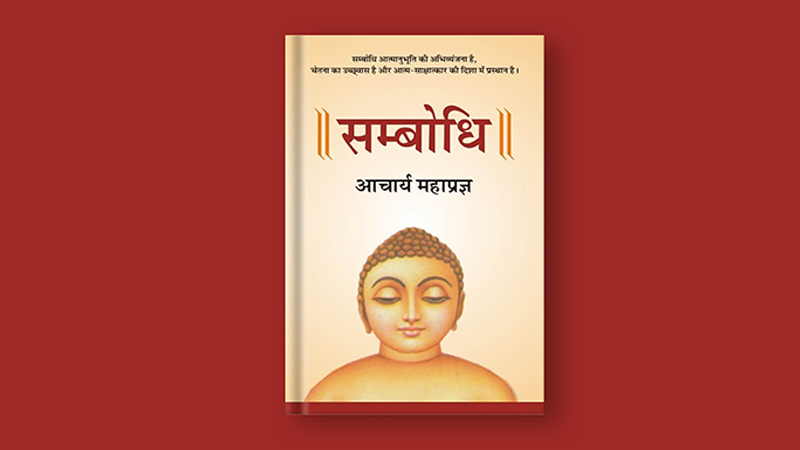
स्वाध्याय
संबोधि
चैतन्य आत्मा का अनन्य सहचारी धर्म है। वह कभी पृथक् नहीं हो सकता। आत्मा अजर और अमर है। गीता में भी कहा है- 'वह कभी जन्म नहीं लेता और न कभी मरता ही है। उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। वह अजन्मा, शाश्वत, नित्य और प्राचीन है। शरीर के मर जाने पर भी वह नहीं मरता।
२४. नासौ नवो नवा जीर्णो, नवोपि च पुरातनः।
आद्या द्रव्यार्थिकी दृष्टिः, पर्यायार्थगता परा॥
आत्मा न नया है और न पुराना यह द्रव्यार्थिक दृष्टि है। आत्मा नया भी है और पुराना भी यह पर्यायार्थिक दृष्टि है।
२५. नवोऽपि च पुराणोऽपि, देहो भवति देहिनाम्।
शैशवं यौवनं तत्र, वार्धक्यञ्चापि जायते।।
जीवों का शरीर नया भी होता है और पुराना भी। शरीर में शैशव, यौवन और वार्धक्य बुढ़ापा भी होता है।
आत्मा पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। नये और पुराने का व्यवहार आत्मा में इसलिए नहीं होता कि वह सर्वकालिक है। न उसका स्वरूप पुराना होना है न नया। दोनों शब्द सापेक्ष हैं। एक रूप को छोड़कर दूसरे रूप में आना नया है और जिसे छोड़ा जाता है वह पुराना है। आत्मा में वैसा नहीं होता। द्रव्यार्थिकदृष्टि से वस्तु का स्वभाव-धर्म अपरिवर्तित होता है।
पर्यायार्थिकदृष्टि भिन्न है। वह पदार्थों की अवस्थाओं को देखती है। अवस्थाएं बदलती हैं अतः नये और पुराने शब्दों का व्यवहार इसमें हो जाता है। आत्मा एक अवस्था का त्याग कर दूसरी अवस्था में आती है तब वह पहले की अपेक्षा नयी है और नये की अपेक्षा पुरानी।
शैशव, यौवन और बुढ़ापा एक ही शरीर की तीन अवस्थाओं से आत्मा में बालक, युवक और वृद्ध शब्दों का व्यवहार हो जाता है।
गीता कहती है-'इस शरीर में आत्मा बचपन, यौवन और वार्धक्य में से गुजरती है। यह शरीर की दशा है। आत्मा उसमें वही है। शरीर का अंत हो जाता है। तब आत्मा नये शरीर को बना लेती है। यह क्रम मुक्ति के अनंतर रुक जाता है। प्राणों के वियोजन से धीर मनुष्य खिन्न नहीं होते। वे सत्य को जानते हैं।

