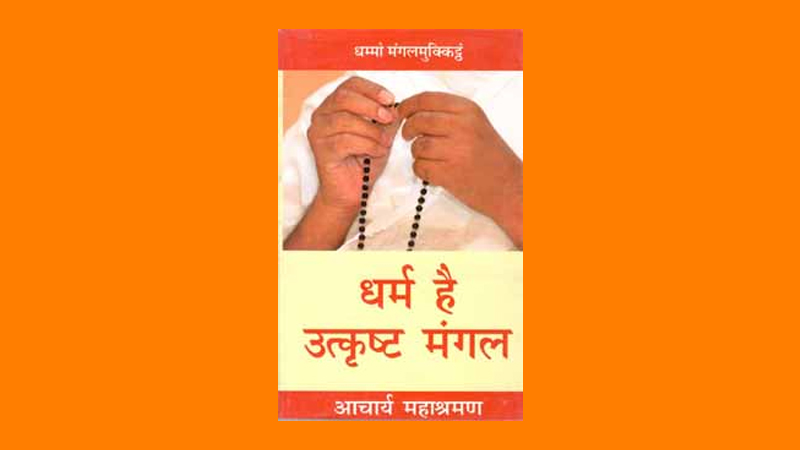
स्वाध्याय
धर्म है उत्कृष्ट मंगल
तप भावना
क्षुधाविजय अथवा क्षुधा-परीषह को सहन करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए तपस्या का अभ्यास करना। पौरुषी, पूर्वार्ध (दो प्रहर), निर्विकृतिक आदि का अभ्यास कर उनके साथ सात्यीभाव करना, उन्हें अपने लिए सहज और सह्य बना लेना। जब तक सात्यीभाव स्थापित नहीं होता है वह साधु उस अभ्यास को छोड़ता नहीं है। तपस्या के अभ्यास को इतना परिपक्व बना लेता है कि विशेष परिस्थिति में शुद्ध आहार न मिलने पर छह महीने तक का उपवास कर लेता है किन्तु अनेषणीय आहार ग्रहण नहीं करता।
सत्त्व भावना
निद्रा विजय का अभ्यास। धीरे-धीरे नींद को कम कर निद्राजय करना।
अभय का अभ्यास करना। इस साधना के लिए वह पांच प्रतिमाओं की साधना से गुजरता है। पहली प्रतिमा में अपने उपाश्रय में ही कोई ऐसा प्रकोष्ठ, जिसको काम में न लिया जा रहा हो, अन्धकार से परिपूर्ण हो, वहां अन्य साधुओं के सो जाने के बाद कायोत्सर्गस्थित हो जाता है और भय को जीतता है। चूहा, बिल्ली आदि रात्रि में घूमने वाले प्राणियों के द्वारा स्पृष्ट होने पर और उनके द्वारा खाए जाने पर भी रोमाञ्च न हो, वहां से भागना न पड़े, ऐसा अभ्यास कर अपने आपको सत्त्व भावना से भावित करता है।
दूसरी प्रतिमा में उपाश्रय से बाहर साधना करता है। वहां पर चौर, आरक्षिक, श्वापद (हिंस्रपशु) आदि के भय पर विजय प्राप्त करता है। तीसरी प्रतिमा में चौराहे में, चौथी प्रतिमा में शून्यगृह में और पांचवीं प्रतिमा में शमशान में जाकर देवसंबंधी, मनुष्यसंबंधी और पशुसंबंधी भय को जीतता है। इस प्रकार सत्त्व भावना का अच्छा अभ्यास हो जाने पर उसमें इतना अभय का विकास हो जाता है कि वह देवता आदि के द्वारा डराने पर भी डरता नहीं और निर्भीकता से जिनकल्प का भार वहन करने में सक्षम बन जाता है।
श्रुत भावना
यद्यपि उस साधु के लिए अपने नाम की भांति श्रुत परिचित होता है फिर भी काल-परिमाण के लिए श्रुत का अभ्यास करता है। श्रुत की परावर्तना के आधार पर काल (समय) का ज्ञान हो सकता है। इतना श्रुत-परावर्तन किया है तो इतना समय हुआ है, ऐसा निश्चय हो जाता है। मेघ से आच्छन्न होने पर भी श्रुत-परावर्तन के द्वारा प्रतिलेखन, प्रतिक्रमण, भिक्षा, विहार के समय का ज्ञान उसे हो जाता है। श्रुत की परावर्तना से चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। स्वाध्याय के कारण महान कर्म निर्जरा होती है। पौरुषी आदि काल के ज्ञान में पराधीनता नहीं रहती जैसे कि अन्य छद्मस्थ साधुओं का ज्ञान सूर्य पर आधारित होता है। श्रुत-भावना से अपने आपको भावित करने वाला शुद्ध ज्ञान, दर्शन और तपः प्रधान संयम को सम्यक् परिणत कर लेता है और श्रुतोपयोग मात्र से काल का परज्ञान करने वाला बन जाता है।
एकत्व भावना
यद्यपि साधु गृहस्थ-काल में होने वाले स्त्री, पुत्र आदि के ममत्व भाव को छिन्न कर डालता है फिर भी दीक्षा के बाद आचार्य आदि में ममत्व भाव हो जाता है। उस ममत्व को भी छोड़ना होता है, उनके साथ बातचीत, परस्पर आहार-पानी, देना-लेना आदि को छोड़ देता है। इस प्रकार अपने साधर्मिक साधु एवं आचार्य आदि के प्रति होने वाले बाह्य प्रेम को क्षीण कर डालने पर उपधि एवं शरीर के प्रति होने वाले ममत्व भाव को भी छोड़ देता है। किसी भी जीव को अपना अथवा पराया नहीं मानता। इस प्रकार की भावना से वह प्रेम-बन्धन को तोड़ डालता है और फिर जिनकल्प स्वीकार करने के बाद अपने स्वजनों का हनन देखकर भी वह क्षुब्ध नहीं होता। ध्यान से विचलित नहीं होता।
बल भावना
बल दो प्रकार का होता है। शारीरिक बल और भाव बल। राग भी दो प्रकार का है-प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। भौतिक पदार्थ, संतान, पत्नी आदि में जो स्नेह जनित राग है वह अप्रशस्त राग है और आचार्य, उपाध्याय आदि के प्रति उनके गुणोत्कर्ष के बहुमान के कारण जो राग होता है वह प्रशस्त राग है। इस दोनों प्रकार के भाव का परित्याग करना भाव बल है। शारीरिक बल भी जिनकल्पिक मुनि का अन्य साधारण जनों की अपेक्षा विशिष्ट होता है। इस प्रकार साधना के विभिन्न प्रयोगों से अपने आपको परिपक्व बनना, पूर्वाभ्यास कर व्यक्ति जिनकल्प साधना के लिए अपने आपको अर्ह बना लेता है।

