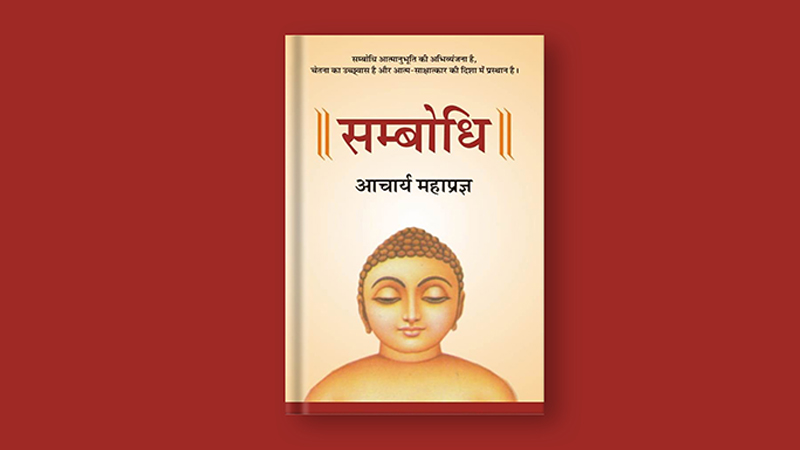
स्वाध्याय
संबोधि
बंध-मोक्षवाद
मिथ्या-सम्यग्-ज्ञान-मीमांसा
भगवान् प्राह
(51) यदा धूतं कर्मरजः भवत्यबोधिना कृतम्।
तदा सर्वगं ज्ञानं, दर्शनं चाऽभिगच्छति।।
जब मनुष्य अबोधि द्वारा संचित कर्मरज को प्रकंपित कर देता है तब वह सर्वत्र-गामी ज्ञान और दर्शन-केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है।
(52) यदा सर्वत्रगं ज्ञानं, दर्शनं चाभिगच्छति।
तदा लोकमलोक×च, जिनो जानाति केवली।।
जब मनुष्य सर्वत्र-गामी ज्ञान और दर्शन-केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है तब वह जिन और केवली होकर लोक-अलोक को जान लेता है।
(53) यदा लोकमलोकं च, जिनो जानाति केवली।
आयुषोऽन्ते निरुन्धानः, योगान् कृत्वा रजः क्षयम्।।
(54) अनन्तामचलां पुण्यां, सिद्धिं गच्छति नीरजाः।
तदा लोकमस्तकस्थः, सिद्धो भवति शाश्वतः।। (युग्मम्)
केवलज्ञान की उपलब्धि होने पर जिन अथवा केवली लोक और अलोक को जान लेता है। वह आयु के अंत में मन, वचन और काय-तीनों योगों का निरोध कर, कर्मरज को सर्वथा क्षीण कर अनंत, अचल और कल्याणकारी सिद्धिगति को प्राप्त कर, शाश्वत सिद्ध होकर लोक के अग्रभाग में अवस्थित हो जाता है।
साधना का प्रथम चरण संयम है और अंतिम भी संयम है। जितने भी साधक हैं संयम उनके लिए अनिवार्य है, इसे यों भी कह सकते हैं कि साधना की चिंतन और उसकी क्रियान्विति संयम से अनुबंध है। संयम के अभाव में जीवन का कोई भी क्षेत्र सुखद, सफल नहीं होता। असंयम पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों के लिए अभिशाप है। शारीरिक दृष्टि से भी असंयमी व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता। स्वास्थ्य भी संयम सापेक्ष है। इसलिए यह उद्घोष मुखर हुआ कि ‘संयमः खलु जीवनम्’ संयम ही जीवन है। इसका विपरीत असंयम मृत्यु है।
संयम का अर्थ है-निरोध। इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का समन्वय है-असत् प्रवृत्ति का पिरोध और सत् में प्रवर्तन। सत् और असत् दोनों का संयम चेतना का पूर्ण विकास है। प्रस्तुत श्लोकों में इसी का दिग्दर्शन है। संयम के माध्यम से ही चेतना का विकास होता है। संयम पूर्ण विकास से पूर्व साधन के रूप में प्रयुक्त होता है और विकास की पूर्णता में साध्य बन जाता है। संयम की साधना के लिए जीव और अजीव के बोध की भी अपेक्षा है। इन्हें नहीं जानने वाला संयम को कैसे जान सकेगा? किसका संयम करेगा? कौन करेगा? क्यों करेगा?
पुरुष अलग है प्रकृति अलग है, किंतु दोनों के अनुबंध से संसार होता है। वैसे ही आत्मा और कर्म दोनों भिन्न-भिन्न होते हुए भी परस्पर में गहरे गूँथे हुए हैं। जब तक ये दोनों विभक्त नहीं होते तब तक संसार का प्रवाह, दुःख-सुख का चक्र, अधोगमन-ऊर्ध्वागमन की यात्रा निराबाध चलती रहती है। प्रकृति-कर्म के इस प्रवाह का अवरोध किए बिना सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति कठिन है। अजीव की माया को समझना भी बहुत दुरूह है। अनेक ज्ञानी भी कर्म-जाल से सहजतया मुक्त नहीं हो सकते। ‘विचित्रा कर्मणां गतिः’ कर्म की गति बड़ी विचित्र है। कर्म का उदय उन्हें भी कहाँ से कहाँ ले जाकर छोड़ देता है। असंख्य उदाहरणों से यह संसार भरा है। आत्मा अनेक उतार-चढ़ाव, सुख-दुःखों की अनुभूति इसी के प्रभाव से करती है। जीव और अजीव की इस संस्कृति की समझ आवश्यक है। संयम की साधना में इनका बोध करणीय है।
(क्रमशः)

