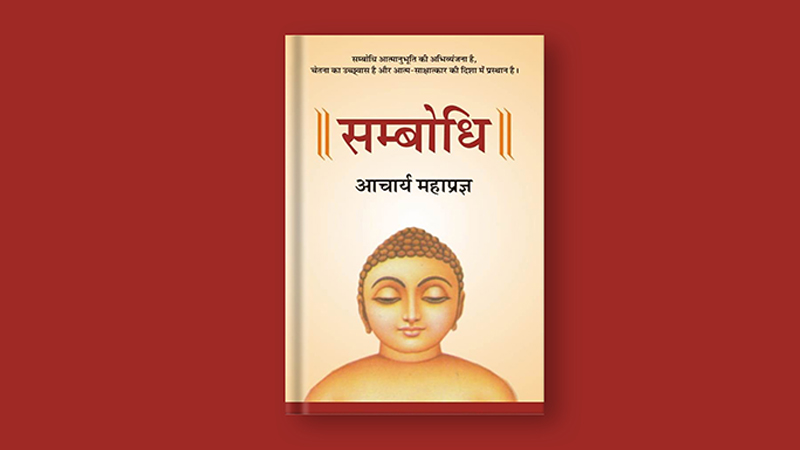
स्वाध्याय
संबोधि
बंध-मोक्षवाद
मिथ्या-सम्यग्-ज्ञान-मीमांसा
भगवान् प्राह
(43) स्वयंबुद्ध! मया बुद्धं, बोधितत्त्वं सुदुर्लभम्।
शरण्य! शरणं देहि, येन बोधिर्विशुद्ध्यति।।
हे स्वयंबुद्ध! मैंने सुदुर्लभ बोधितत्त्व को जान लिया है। हे शरण्य! मुझे शरण दो, जिससे मेरी बोधि विशुद्ध बन जाए।
बोधि सुदुर्लभ है, किंतु स्वयंबुद्ध भगवान महावीर के सहवास, सान्निध्य से उसके लिए सुलभ बन गई। ‘सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्’ सत्य को उपलब्ध पुरुषों की संगति क्या नहीं करती है? वह क्षुद्र को महान् बना देती है, भ्रांत को अभ्रांत बना देती है, पथ-भ्रष्ट को मार्ग में सुस्थिर कर देती है और नर को नारायण, अशिव को शिव बना देती है। मेघ शिव की कोटि में आ गया। उसके रोम-रोम से आनंद का स्रोत फूट पड़ा। उसने कहा-प्रभो! मैं अब आपकी शरण में हूँ, मेरी पतवार आपके हाथों में है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरी बोधि सदा विशुद्ध बनी रहे। उसमें कहीं कोई मलिनता प्रविष्ट न हो जाए। बस, मेरा आपसे यही अनुनय है।
इति आचार्यमहाप्रज्ञविरचिते संबोधिप्रकरणे
संयतचर्यानामा दशमोऽध्यायः।
आत्ममूलकधर्म-प्रतिपादन
भगवान् प्राह
(1) अस्त्यात्मा चेतनारूपो, भिन्नः पौद्गलिकैर्गुणैः।
स्वतंत्रः करणे भोगे, परतंत्रश्च कर्मणाम्।।
आत्मा का स्वरूप चेतन है। वह पौद्गलिक गुणों से भिन्न है। वह कर्म करने में स्वतंत्र और उसका फल भोगने में परतंत्र है।
आत्मा और पुद्गल (डंजजमत) दोनों भिन्न हैं। दोनों में कुछ सामान्य गुणों का एकत्व होते हुए भी चेतन का स्व-बोध, ज्ञान-गुण उससे सर्वथा भिन्न है। पुद्गल में अपना कोई बोध नहीं है। वह जड़ है। निर्जीव और सजीव के बीच एक भेद-रेखा विज्ञान भी स्पष्ट देखने लगा है। शरीर से निकलने वाला वलय चेतना का ही विशेष गुण-धर्म है। प्राणी की प्राणशक्ति क्षीण होने पर आभावलय भी क्षीण होता हुआ देखा गया है। इससे दोनों की भिन्नता स्पष्ट प्रतीत होती है। जड़ और चेतन की भिन्नता के द्योतक और भी कुछ लक्षण हैं।
‘अप्पा कत्ता विकत्ता य सुहाण य दुहाण य’-आत्मा ही सुख की कर्त्ता और विकर्त्ता है। यह वाक्य आत्म-स्वतंत्र्य का पूर्ण परिचायक है। यदि परतंत्र हो तो फिर उसके वश में कुछ नहीं होगा, फिर वह दूसरों के हाथ की कठपुतली होगी। मुक्ति या निर्वाण की बात कोई तथ्य-संगत नहीं होगी। सुख-दुःख के निर्माण में उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। परतंत्रता है तो सिर्फ इतनी ही कि कर्म का भोग न चाहने पर भी उसे भोगना पड़ता है, क्योंकि स्वयं उसने तथानुरूप कर्मों का संग्रह किया है। यह भी स्पष्ट है कि चेतन आत्मा अचेतन कर्म का संग्रह कैसे करे? कर्म ही कर्म को आकृष्ट करता है। संस्कार अन्य संस्कार के लिए द्वार खुला रखता है। उसी मार्ग से वे आते हैं और आत्मा को बाँधते हैं। वे जब आत्मा से अलग होते हैं। तब स्व-बोध के कारण आत्मा रागात्मक, द्वेषात्मक और मोहात्मक रूप में परिणत नहीं होती। जिस दिन अज्ञान का आवरण मंद, मंदतर और मंदतम हो जाता है, उसी दिन स्वबोध, आवरण क्षय और दुःख क्षय के लिए वह सहज हो जाता है। संस्कार (कर्म) उखड़ते हैं किंतु वह उन्हें सहारा नहीं देती, उनके साथ प्रवाहित नहीं होती। शनैः-शनैः संस्कारों का पथ उखड़ जाता है और आत्मा अपने मूलरूप में विराजमान हो जाती है। यही पूर्ण स्वातंत्र्य है। (क्रमशः)

