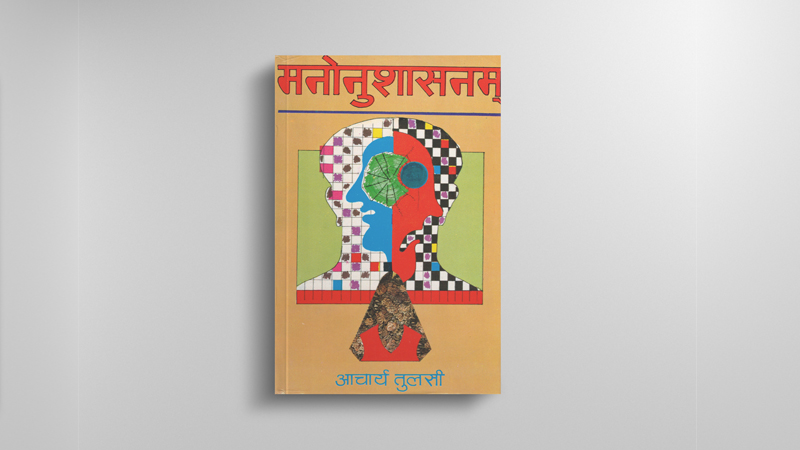
स्वाध्याय
मनोनुशासनम्
शरीर-प्रेक्षा
साधना की दृष्टि से शरीर का बहुत महत्त्व है। यह आत्मा का केन्द्र है। इसी के माध्यम से चैतन्य अभिव्यक्त होता है। चैतन्य पर आए हुए आवरण को दूर करने के लिए इसे सशक्त माध्यम बनाया जा सकता है। इसीलिए गौतम ने केशी से कहा था- ‘यह शरीर नौका है। जीव नाविक है और संसार समुद्र है।’
इस नौका के द्वारा संसार का पार पाया जा सकता है। शरीर को समग्र दृष्टि से देखने की साधना-पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के तीन भाग हैं:
१- अधोभाग-आंख का गढ्ढा, गले का गढ्ढा, मुख के बीच का भाग।
२-ऊर्ध्वभाग- घुटना, छाती, ललाट, उभरे हुए भाग
3- तिर्यंग् भाग- समतल भाग।
शरीर के अधोभाग में स्रोत है, ऊर्ध्वभाग में स्रोत हैं और मध्य भाग में स्रोत-नाभि है।
साधक चक्षु को संयत कर शरीर की विपश्यना करे। उसकी विपश्यना करने वाला उसके अधोभाग को जान लेता है, उसके ऊर्ध्व भाग को जान लेता है और उसके मध्य भाग को जान लेता है।
जो साधक वर्तमान क्षण में शरीर में घटित होने वाली सुख-दुःख की वेदना को देखता है, वर्तमान क्षण का अन्वेषण करता है, वह अप्रमत्त हो जाता है।
शरीर-दर्शन की यह प्रक्रिया अन्तर्मुख होने की प्रक्रिया है। सामान्यतः बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली चैतन्य की धारा को अन्तर की ओर प्रवाहित करने का प्रथम साधन स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर के भीतर तैजस और कर्म- ये दो सूक्ष्म शरीर हैं। उनके भीतर आत्मा है। स्थूल शरीर की क्रियाओं और संवेदनों को देखने का अभ्यास करने वाला क्रमशः तेजस और कर्म शरीर को देखने लग जाता है। शरीर-दर्शन का दृढ़ अभ्यास और मन के सुशिक्षित होने पर शरीर में प्रवाहित होने वाली चैतन्य की धारा का साक्षात्कार होने लग जाता है। जैसे-जैसे साधक स्थूल से सूक्ष्म दर्शन की ओर आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे उसका अप्रमाद बढ़ता जाता है ।
स्थूल शरीर के वर्तमान क्षण को देखने वाला जागरूक हो जाता है। कोई क्षण सुख-रूप होता है और कोई क्षण दुःख-रूप। क्षण को देखने वाला सुखात्मक क्षण के प्रति राग नहीं करता और दुःखात्मक क्षण के प्रति द्वेष नहीं करता। वह केवल देखता और जानता है।
शरीर की प्रेक्षा करने वाला शरीर के भीतर से भीतर पहुंचकर शरीर- धातुओं को देखता है और झरते हुए विविध स्रोतों (अन्तरों) को भी देखता है।
देखने का प्रयोग बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। उसका महत्त्व तभी अनुभूत होता है, जब मन की स्थिरता, दृढ़ता और स्पष्टता से दृश्य को देखा जाए। शरीर के प्रकम्पनों को देखना, उसके भीतर प्रवेश कर भीतरी प्रकम्पनों को देखना, मन को बाहर से भीतर में ले जाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से मूर्च्छा टूटती है और सुप्त चैतन्य जागृत होता है। शरीर का जितना आयतन है, उतना ही आत्मा का आयतन है। जितना आत्मा का आयतन है, उतना ही चेतना का आयतन है। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर के कण-कण में चैतन्य व्याप्त है। इसीलिए शरीर के प्रत्येक कण में संवेदन होता है। उस संवेदन से मनुष्य अपने स्वरूप को देखता है, अपने अस्तित्व को जानता है और अपने स्वभाव का अनुभव करता है। शरीर में होने वाले संवेदन को देखना चैतन्य को देखना है, उसके माध्यम से आत्मा को देखना है।
4- वर्तमान क्षण की प्रेक्षा
अतीत बीत जाता है, भविष्य अनागत होता है, जीवित क्षण वर्तमान होता है । भगवान् महावीर ने कहा- ‘खणं जाणाहि पंडिए!’ साधक तुम क्षण को जानो। अतीत के संस्कारों की स्मृति से भविष्य की कल्पनाएं और वासनाएं होती हैं। वर्तमान क्षण का अनुभव करने वाला स्मृति और कल्पना दोनों से बच जाता है। स्मृति और कल्पना राग-द्वेषयुक्त चित्त का निर्माण करती हैं। जो वर्तमान क्षण का अनुभव करता है, वह सहज ही राग-द्वेष से बच जाता है। यह राग-द्वेषशून्य वर्तमान क्षण ही संवर है। राग-द्वेषशून्य वर्तमान क्षण को जीने वाला अतीत में अर्जित कर्म-संस्कार के बंध का निरोध करता है। इस प्रकार वर्तमान क्षण में जीने वाला अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान का संवरण और भविष्य का प्रत्याख्यान करता है।
तथागत अतीत और भविष्य के अर्थ को नहीं देखते। कल्पना को छोड़ने वाला महर्षि वर्तमान का अनुपश्यी हो, कर्म शरीर का शोषण कर उसे क्षीण कर डालता है।
भगवान् महावीर ने कहा- ‘इस क्षण को जानो।’ वर्तमान को जानना और वर्तमान में जीना ही भाव क्रिया है। यांत्रिक जीवन जीना, काल्पनिक जीवन जीना और कल्पना लोक में उड़ान भरना द्रव्य क्रिया है। वह चित्त का विक्षेप है और साधना का विघ्न है। भाव-क्रिया स्वयं साधना और स्वयं ध्यान है। हम चलते हैं और चलते समय हमारी चेतना जागृत रहती है, ‘हम चल रहे हैं’- इसकी स्मृति रहती है- यह गति की भावक्रिया है। इसका सूत्र है कि साधक चलते समय पांचों इन्द्रियों के विषयों पर मन को केन्द्रित न करे। आंखों से कुछ दिखाई देता है, शब्द कानों से टकराते हैं, गंध के परमाणु आते हैं, ठंडी या गरम हवा शरीर को छूती है इन सबके साथ मन को न जोड़ें। रस की स्मृति न करें।
साधक चलते समय पांचों प्रकार का स्वाध्याय न करे- न पढ़ाए, न प्रश्न पूछे, न पुनरावर्तन करे, न अर्थ का अनुचिन्तन करे और न धर्म-चर्चा करे। मन को पूरा खाली रखे। साधक चलने वाला न रहे। किन्तु चलना बन जाए, तन्मूर्ति (मूर्तिमान् गति) हो जाए। उसका ध्यान चलने में ही केन्द्रित रहे., चेतना गति का पूरा साथ दे। यह गमनयोग है।
शरीर और वाणी की प्रत्येक क्रिया भाव-क्रिया बन जाती है, जब मन की क्रिया उसके साथ होती है, चेतना उसमें व्याप्त होती है।
भाव-क्रिया का सूत्र है- चित्त और मन क्रियमाण क्रियामय हो जाएं, इन्द्रियां उस क्रिया के प्रति समर्पित हों, हृदय उसकी भावना से भावित हो, मन उसके अतिरिक्त किसी अन्य विषय में न जाए, इस स्थिति में क्रिया भाव-क्रिया बनती है।
5- समता
आत्मा सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है, इसलिए वह परोक्ष है। चैतन्य उसका गुण है? उसका कार्य है- जानना और देखना। मन और शरीर के माध्यम से जानने और देखने की क्रिया होती है, इसलिए चैतन्य हमारे प्रत्यक्ष है। हम जानते हैं, देखते हैं, तब चैतन्य की क्रिया होती है। समग्र साधना का यही उद्देश्य है कि हम चैतन्य की स्वाभाविक क्रिया करें। केवल जानें और केवल देखें। इस स्थिति में अबाध आनन्द और अप्रतिहत शक्ति की धारा प्रवाहित रहती है, किन्तु मोह के द्वारा हमारा दर्शन निरुद्ध और ज्ञान आवृत रहता है, इसलिए हम केवल जानने और केवल देखने की स्थिति में नहीं रहते। हम प्रायः संवेदन की स्थिति में होते हैं। केवल जानना ज्ञान है। प्रियता और अप्रियता के भाव से जानना संवेदन है। हम पदार्थ को या तो प्रियता की दृष्टि से देखते हैं या अप्रियता की दृष्टि से। पदार्थ को केवल पदार्थ की दृष्टि से नहीं देख पाते। पदार्थ को केवल पदार्थ की दृष्टि से देखना ही समता है। वह केवल जानने और देखने से सिद्ध होती है। यह भी कहा जा सकता है कि केवल जानना और देखना ही समता है। जिसे समता प्राप्त होती है, वही ज्ञानी होता है। जो ज्ञानी होता है, उसी को समता प्राप्त होती है । ज्ञानी और साम्ययोगी- दोनों एकार्थक होते हैं।
हम इन्द्रियों के द्वारा देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा मन के द्वारा संकल्प-विकल्प या विचार करते हैं। प्रिय लगने वाले इन्द्रिय-विषय और मनोभाव राग उत्पन्न करते हैं और अप्रिय लगने वाले इन्द्रिय- विषय और मनोभाव द्वेष उत्पन्न करते हैं। जो प्रिय और अप्रिय लगने वाले विषयों और मनोभावों के प्रति सम होता है, उसके अन्तःकरण में वे प्रियता और अप्रियता का भाव उत्पन्न नहीं करते। प्रिय और अप्रिय तथा राग और द्वेष से परे वही हो सकता है, जो केवल ज्ञाता और द्रष्टा होता है। जो केवल ज्ञाता और द्रष्टा होता है, वही वीतराग होता है।
जैस-जैसे जानने और देखने का अभ्यास बढ़ता है, वैसे वैसे इंद्रियां-विषय और मनोभाव, प्रियता और अप्रियता उत्पन्न करना बंद कर देते हैं। फलतः राग और द्वेष, शांत और क्षीण होने लगते हैं। हमारी जानने और देखने की शक्ति अधिक प्रस्फुट हो जाती है। मन में कोई संकल्प उठे, उसे हम देखें। विचार का प्रवाह चल रहा हो, उसे हम देखें। इसे देखने का अर्थ होता है कि हम अपने अस्तित्व को संकल्प से भिन्न देख लेते हैं। संकल्प दृश्य है और ‘मैं दृष्टा हूं’- इस भेद का स्पष्ट अनुभव हो जाता है। जब संकल्प के प्रवाह को देखते जाते हैं, तब धीमे-धीमे उसका प्रवाह रूक जाता है। संकल्प के प्रवाह को देखते-देखते हमारी दर्शन की शक्ति इतनी पटु हो जाती है कि हम दूसरे के संकल्प-प्रवाह को भी देखने लग जाते हैं।
हमारी आत्मा में अखंड चैतन्य है। उसमें जानने-देखने की असीम शक्ति है, फिर भी हम बहुत सीमित जानते-देखते हैं। इसका कारण है कि हमारा ज्ञान आवृत है, हमारा दर्शन आवृत है। इस आवरण की सृष्टि मोह ने की है। मोह को राग और द्वेष का पोषण मिल रहा है- प्रियता और अप्रियता मनोभाव से। यदि हम जानने देखने की शक्ति का विकास चाहते हैं तो हमें सबसे पहले प्रियता और अप्रियता के मनोभावों को छोड़ना होगा। उन्हें छोड़ने का जानने और देखने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमारे भीतर जानने और देखने की जो शक्ति बची हुई है, हमारा चैतन्य जितना अनावृत है, उसका हम उपयोग करें। केवल जानने और देखने का जितना अभ्यास कर सकें, करें। इससे प्रियता और अप्रियता के मनोभाव पर चोट होगी। उससे राग-द्वेष का चक्रव्यूह टूटेगा। उससे मोह की पकड़ कम होगी। फलस्वरूप ज्ञान और दर्शन का आवरण क्षीण होने लगेगा। इसलिए वीतराग-साधना का आधार जानना और देखना ही हो सकता है। इसीलिए इस सूत्र की रचना हुई है कि समूचे ज्ञान का सार सामयिक है - समता है।
6- संयम - संकल्प शक्ति का विकास
हमारे भीतर शक्ति का अनन्त कोष है। उस शक्ति का बहुत बड़ा भाग ढ़का हुआ है, प्रतिहत है। कुछ भाग सत्ता में है और कुछ भाग उपयोग में आ रहा है। हम अपनी शक्ति के प्रति जागरूक हों तो सत्ता में रही हुई शक्ति और प्रतिहत शक्ति को उपयोग की भूमिका तक ला सकते हैं। (क्रमशः)

