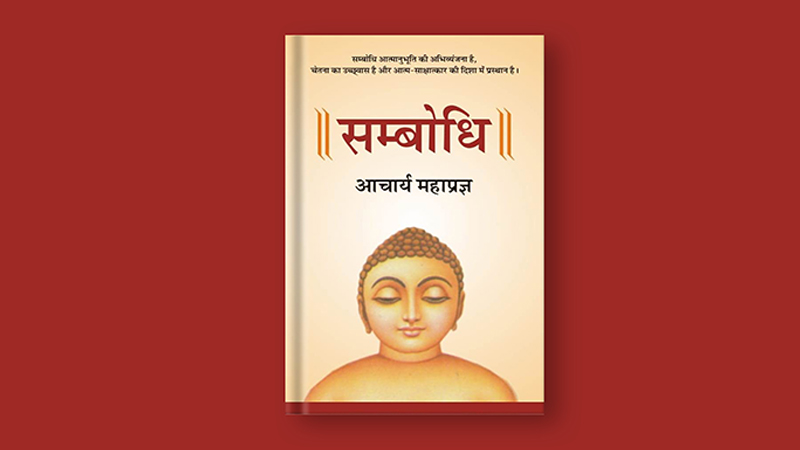
स्वाध्याय
संबोधि
बंध मोक्षवाद
मिथ्या-सम्यग्-ज्ञान-मीमांसा
मेघ का कथन ठीक है कि धर्म व्यक्ति के जीवन में बड़ा हस्तक्षेप करता है। लोक-जीवन का भवन झूठ पर खड़ा होता है। धार्मिक होने का अर्थ है- सत्य की दिशा में चलना। धार्मिक व्यक्ति के समस्त व्यवहारों में सत्य का प्रतिबिम्ब झलकने लगता है। अब वह पहले की तरह चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेना-देना नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता। उसे कोई भी कार्य करते हुए यह सोचना होगा कि इससे धर्म की हानि होगी या वृद्धि धीरे-धीरे जीवन की असत् प्रवृत्तियां विदा होने लगेंगी। वर्षा से स्नात वनराजि की तरह एक दिन उसका जीवन दीप्तिमान हो उठेगा।
किन्तु पहले ही क्षण में धर्म के इस परिणाम की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। उसके लिए बड़े उत्साह, धैर्य, त्याग और संघर्षों की आवश्यकता होती है। धर्म का जीवन प्रारंभ करते ही घर, परिवार, समाज आदि से संघर्ष का सूत्रपात भी हो जाता है। लोग नहीं चाहते कि आप सबसे उदासीन हो जाएं। आपकी उदासी भी दूसरों को पीड़ाकारक बन जाती है। लोक-भय से ही अनेक व्यक्ति उस मार्ग पर चलना छोड़ देते हैं। धर्म की तेजस्विता में कोई संदेह नहीं है, संदेह है व्यक्ति की क्षमता पर।
धर्म का विकास सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यग् आचरण (चारित्र) पर निर्भर है। इनके अभाव में विकास नहीं, ह्रास होता है। धर्म के जीवंत सूत्रों की उपेक्षा कर धर्म के कलेवर को जीवित रखा जा सकता है, किन्तु धर्म की आत्मा को नहीं। जितने भी अर्हत्, बुद्ध और परम प्रज्ञा-प्राप्त साधक हुए हैं, उन्होंने मूल पर बल दिया है, गौण पर नहीं।
आनंद ने बुद्ध से पूछा- ‘निर्वाण के बाद आपके शरीर का क्या किया जाए? बुद्ध ने कहा-‘आनंद! इसमें सिर मत खपाओ, मैंने जो साधना-धर्म बताया है, उसका अभ्यास करो।’
वक्कलि भिक्षु से बुद्ध कहते हैं- ‘जैसे यह तुम्हारा अशुचिमय शरीर है, वैसा ही बुद्ध का है। वक्कलि! मेरे इस शरीर को मत देखो, धर्म-शरीर को देखो। जो मेरे धर्म-शरीर को देखता है वह मुझे देखता है और जो मुझे देखता है वह मेरे धर्म-शरीर को देखता है।’
महावीर गौतम से कहते हैं- गौतम! सत्य की शोध में प्रमाद मत कर। मेरे से स्नेह मत कर। सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना कर मुक्त हो।’
जब बाह्य क्रियाएं और चमक-दमक व्यक्ति को प्रभावित करने लगते हैं तब धर्म का मौलिक ध्येय गौण हो जाता है या मौलिक धर्म के प्रति अनुत्साह होने से बाह्य क्रियाओं का महत्त्व बढ़ जाता है। मूल छूट जाता है और बाहरी पकड़ सुदृढ़ हो जाती है। मूल छिप जाता है और गौण ऊपर आ जाता है। जिसकी सुरक्षा के लिए जो होता है, उसकी सुरक्षा प्रमुख हो जाती है और मूल धूमिल हो जाता है।
धर्म की सुरक्षा प्रमुख है। इसी में प्राणिमात्र का हित है। उसके प्रति सजग होना जरूरी है। सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्र जितने पुष्ट और सशक्त होंगे, धर्म उतना ही शक्तिशाली होगा। इनके बाहर धर्म नहीं है।
इति आचार्यमहाप्रज्ञविरचिते संबोधिप्रकरणे
आत्ममूलकधर्मप्रतिपादननामा एकादशोऽध्यायः।

