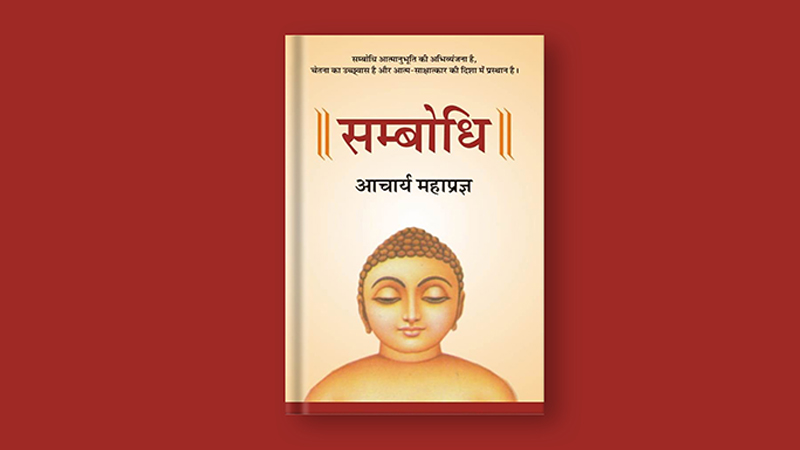
स्वाध्याय
संबोधि
बंध-मोक्षवाद
ज्ञेय-हेय-उपादेय
भगवान् प्राह
(6) निरोधः कर्मणामस्ति, संवरो निर्जरा तथा।
कर्मणां प्रक्षयश्चैषोपादेयदृष्टिरिष्यते।।
कर्मों का निरोध करना संवर है और कर्मों के क्षय से होने वाली आत्मशुद्धि निर्जरा है-यह उपादेयदृष्टि है।
साधना-पथ पर अग्रसर होने से पूर्व साधक के लिए यह जानना जरूरी है कि वह क्यों इस मार्ग का चुनाव कर रहा है? पहले या पीछे यह विवेक किए बिना साधना का शुभारंभ फलदायी नहीं होता। सामान्य जन भी बिना किसी उद्देश्य के प्रवृत्त नहीं होते। दिशाहीन गति का कोई अर्थ नहीं रहता। हेय, ज्ञेय और उपादेय-इस तत्त्वत्रयी का बोध साधक को भटकने नहीं देता। वह सतत ध्येय की दिशा में बढ़ता रहता है।
जो जानने का है उसे जानें, छोड़ने का है उसे छोड़ें और जो उपादेय है उसके ग्रहण में संलग्न रहे। अकुशल प्रवृत्तियों से बचना, जो हैं उन्हें हटाना और कुशल प्रवृत्ति की संरक्षा करना तथा जो नहीं है वह कैसे संप्राप्त हो इसमें सचेष्ट रहना। साधना का यह प्रथम चरण है। इसलिए जितने भी साधक हुए हैं उन्होंने अशुभ से बचने का प्रथम सूत्र दिया है। महावीर ने कहा है-‘सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णा फला, दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णा फला-अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल होता है। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध ने कहा है-भिक्षुओ! जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। अच्छा कर्म करने वाला अच्छा फल पाता है और बुरा कर्म करने वाला बुरा। भिक्षुओ! जिसकी दृष्टि मिथ्या होती है, संकल्प मिथ्या होते हैं, वाणी, कर्मान्त, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि, ज्ञान तथा विमुक्ति मिथ्या होती है, उसके कारण उसका शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक-सभी कर्म अनिष्ट दुःख के लिए होते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि ही बुरी होती है।
पुण्य, पाप, आश्रव और बंध हेय हैं, क्योंकि इनका कार्य संसार है। पुण्य का फल अच्छा है, किंतु अच्छा होने से संसार-विच्छेद नहीं होता। निर्वाण की अपेक्षा वह हेय है। पुण्य और पाप दोनों से मुक्त होना है। सुख-वेदन या दुःख-वेदन दोनों का क्षय करना है। संवर, निर्जरा और मोक्ष उपादेय हैं। मोक्ष की उपादेयता निर्बाध है। क्योंकि वहाँ पुण्य-पाप दोनों ही नहीं हैं। वह भव का अंत है। संवर और निर्जरा मोक्ष की पृष्ठभूमि का काम करते हैं। साधक एक साथ निर्वाण को उपलब्ध नहीं कर सकता। संवर-निर्जरा की क्रमिक साधना निर्वाण को निकट करती है। उपयोगिता की दृष्टि से इनका विवेक कर योग-मार्ग में आरूढ़ होना चाहिए।
(7) अमूढं आत्मगं चित्तं, योगो योगिभिरिष्यते।
मनोगुप्तिः समाधिश्च, साम्यं सामायिकं तथा।।
जो चित्त आत्म-लीन एवं अमूढ़-मूच्र्छाग्रस्त नहीं है, उसे योगी योग कहते हैं। मनोगुप्ति, समाधि, साम्य और सामायिक-ये सब योग के ही रूप हैं।
(8) ऐकाग्र्यं मनसश्चाद्ये, भवेच्चान्ते निरोधनम्।
मनःसमितिगुप्त्योश्च, सर्वो योगो विलीयते।।
ध्यान की दो अवस्थाएँ होती हैं। एकाग्रता और निरोध। प्रारंभिक दशा में मन की एकाग्रता होती है और अंतिम अवस्था में उसका निरोध होता है। मन की समिति-सम्यक् प्रवर्तन और मन की गुप्ति-निरोध में सारा योग समा जाता है।
(9) मोक्षेण योजनाद् योगः, समाधिर्योग इष्यते।
स तपो विद्यते द्वैधा, बाह्येनाभ्यन्तरेण च।।
जो आत्मा को मोक्ष से जोड़े, वह योग कहलाता है। आत्मा और मोक्ष का संबंध समाधि से होता है इसलिए समाधि को योग कहा जाता है। योग तप है। उसके दो भेद हैं-बाह्य तप और आभ्यंतर तप।
(10) चतुर्विधस्याहारस्य, त्यागोऽनशनमुच्यते।
आहारस्याल्पतामाहुः, अवमौदर्यमुत्तमम्।।
अन्न, पानी, खाद्य-मेवा आदि, स्वाद्य-लवंग आदि-इस चार प्रकार के आहार के त्याग को अनशन कहते हैं। आहार, पानी की अल्पता करने को अवमौदर्य-ऊनोदरिका कहते हैं।
(11) अभिग्रहो हि वृत्तीनां, वृत्तिसंक्षेप इष्यते।
भवेद् रसपरित्यागो, रसादीनां विसर्जनम्।।
वृत्ति-आजीविका के लिए अभिग्रह-प्रतिज्ञा करने को वृत्ति-संक्षेप कहते हैं। घी, तेल, दूध, दही, चीनी और मिठाई-इन विकृतियों के त्याग करने को रस-परित्याग कहते हैं।
(क्रमशः)

