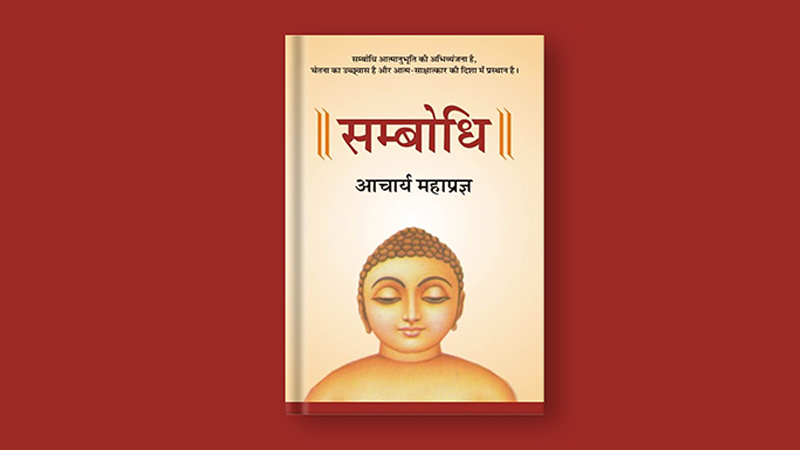
स्वाध्याय
संबोधि
बंध-मोक्षवाद
ज्ञेय-हेय-उपादेय
भगवान् प्राह
(16) चेतना विषयासक्ता, हिंसां समनुधावति।
आत्मानं प्रति संहृत्य, तामहिंसापदं नयेत्।।
जो चेतना विषयों में आसक्त है, वह हिंसा की ओर दौड़ती है। इसलिए साधक उस चेतना को आत्मा की ओर मोड़कर उसे अहिंसा में प्रतिष्ठित करे।
(17) सति देहे सेन्द्रियेऽस्मिन्, सति चेतसि च×चले।
इंद्रियार्थाः प्रकृत्येष्टाः, नेष्टं तेषां विसर्जनम्।।
जब तक शरीर और इंद्रियाँ हैं, जब तक मन चंचल है, तब तक स्वभावतः इंद्रियों के विषय अच्छे लगते हैं, उनका परित्याग अच्छा नहीं लगता।
(18) अहिंसार्थं मया प्रोक्तं, आत्मसाम्यं चिराध्वनि।
तदर्थं प्राप्तदुःखानि, सोढव्यानि मुमुक्षुभिः।।
साधना की चिर परंपरा में मैंने आत्म-साम्य का निरूपण अहिंसा के विकास के लिए किया है। मुमुक्षु व्यक्तियों को अहिंसा की साधना के मध्य जो भी दुःख प्राप्त हों, उन्हें सहना चाहिए।
(19) न देहोऽधर्ममूलोऽसौ, धर्ममूलो न चाप्यसौ।
योजितो योजकेनासौ, धर्माधर्मकरो भवेत्।।
देह न अधर्म का मूल है और न धर्म का। योजक के द्वारा जिस प्रकार उसकी योजना की जाती है, उसी प्रकार वह धर्म या अधर्म का मूल बन जाता है।
(20) नास्य शक्तिः परिस्फीता, विकारोद्दीपनं सृजेत्।
तेनाऽसौ कृशतां नेयः, यावदुत्सहते मनः।।
बढ़ी हुई शारीरिक शक्ति विकारों का उद्दीपन न करे, जब तक मन का उत्साह बढ़ता रहे-वह अमंगल का चिंतन न करे, तब तक शरीर को तप के द्वारा कृश करना चाहिए।
(21) नात्मासौ शक्तिहीनानां, गम्यो भवति सर्वदा।
योगक्षेमौ हि तेनास्य, कार्यावपि मुमुक्षुणा।।
शक्तिहीन मनुष्यों के लिए यह आत्मा गम्य नहीं होता, यह शाश्वत सिद्धांत है, इसलिए मुमुक्षु व्यक्तियों के लिए शरीर का योग और क्षेम भी करणीय होता है।
(22) न केवलमसौ देहः, कृशीकार्यो विवेकिना।
न च बृंहणीयोस्ति, मतं संतुलनं मम।।
मेरा यह अभिमत है-विवेकी व्यक्ति न देह को ज्यादा कृश करे और न ज्यादा उपचित। देह का संतुलन ही सबसे अच्छा है।
(23) इंद्रियाणि प्रशान्तानि, विहरेयुर्यथा यथा।
तथा तथा प्रवृत्तीनां, दैहीनां संयमो मतः।।
उपशांत इंद्रियाँ जैसे-जैसे प्रवृत्त होती हैं, वैसे-वैसे ही मनुष्य की दैही-शारीरिक प्रवृत्तियाँ संयत होती चली जाती हैं।
(24) दोषनिर्हरणायेष्टा, उपवासाद्युपक्रमाः।
प्राणसंधारणायासौ, आहारो मम सम्मतः।।
दोषों को बाहर निकालने के लिए उपवास आदि उपक्रम विहित हैं। प्राण को धारण करने के लिए आहार भी मुझे सम्मत है।
(25) अहिंसाधर्मसंसिद्धौ, विवेको नाम दुष्करः।
तेन वत्स! मया धर्मः, घोरोऽसौ प्रतिपादितः।।
अहिंसा धर्म की संसिद्धि-साधना में विवेक होना बहुत दुष्कर है। वत्स! इसी दृष्टि से धर्म को मैंने घोर कहा है।
(26) नाज्ञानचेष्टितं वत्स! न च संक्लेशसंकुलम्।
नात्र्तध्यानदशां प्राप्तं, तपो ममास्ति सम्मतम्।।
वत्स! मैंने उसी तप का अनुमोदन किया है, जिसमें न अज्ञान संवलित चेष्टाएँ हैं, न संक्लेश है और न आत्र्तध्यान है।
(27) इंद्रियाणां मनसश्च, विषयेभ्यो निवर्तनम्।
स्वस्मिन् नियोजनं तेषां, प्रतिसंलीनता भवेत्।।
इंद्रिय और मन का विषयों से निवर्तन तथा अपने-अपने गोलक में उनका नियोजन प्रतिसंलीनता है।
प्रतिसंलीनता के चार प्रकार हैं-(1) इंद्रिय संलीनता-इंद्रियों के विषयों पर नियंत्रण करना। (2) कषाय संलीनता-कषायों पर विजय पाना। (3) योग संलीनता-मन, वचन और शरीर की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना। (4) विविक्त-शयन-आसन-एकांत स्थान में सोना-बैठना।
(क्रमशः)

