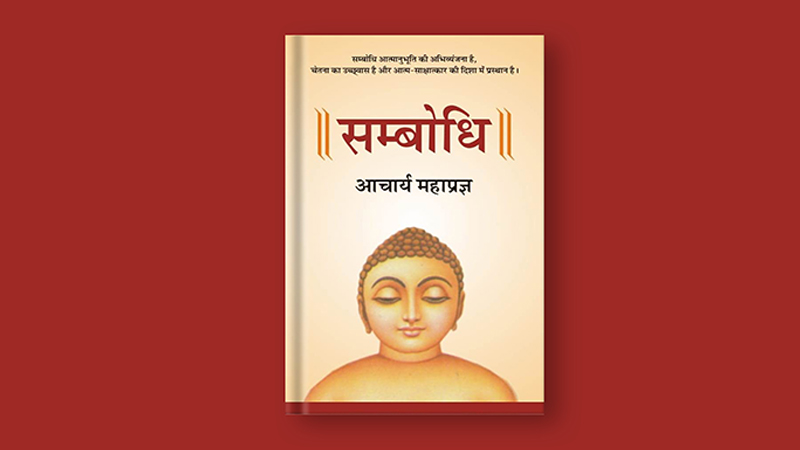
स्वाध्याय
संबोधि
बंध-मोक्षवाद
ज्ञेय-हेय-उपादेय
भगवान् प्राह
बारह भावनाएँ
(12) बोधि-दुर्लभ भावना-मनुष्य का जन्म दुर्लभ है और बोधि उससे अधिक दुर्लभ है। मौनीज यहूदी संत के मृत्यु की सन्निकट वेला थी। पुरोहित पास में खड़ा मंत्र पढ़ रहा था। उसने कहा-‘मूसा का स्मरण करो, यह अंतिम क्षण है।’ मौनीज ने आँखें खोली और कहा, ‘हटो यहाँ से। मेरे सामने नाम मत लो मूसा का।’ पुरोहित को आश्चर्य हुआ, सब देखते रहे, यह कैसी बात? पुरोहित ने कहा-‘जीवन भर जिनका गीत गुनगुनाया, हजारों लोगों को संदेश दिया और अब यह क्या कह रहे हो? जिंदगी की सारी प्रतिष्ठा धूल में मिला रहे हो?’ मैनीज ने कहा, ‘मैं जानता हूँ। किंतु अभी प्रश्न वैयक्तिक है। मूसा यह नहीं पूछेगा कि तुम मूसा क्यों नहीं हुए। वह पूछेगा कि तुम मौनीज क्यों नहीं हुए? स्वयं का होना बोधि है। जीवन में सब कुछ पाकर भी जिसने बोधि नहीं पाई, उसने कुछ नहीं पाया और बोधि पाकर जिसने कुछ नहीं पाया उसने सब कुछ पा लिया। मरने के बाद सब कुछ छूट जाता है, खो जाता है, वह हमारी अपनी संपत्ति नहीं है। संबोधि अपनी संपत्ति है, उसे खोजना है। अनेक-अनेक योनियों में पैदा हुए और मरे, किंतु स्वयं के अस्तित्व को नहीं पहचाना। जन्म के पूर्व और मरने के बाद भी जिसका अस्तित्व अखंड रहता है, उसकी खोज में निकलना बोधि भावना का अभिप्राय है। आचार्य शुभचंद्र ने लिखा है-‘भावनाओं में रमण करता हुआ साधक इसी जीवन में दिव्य मुक्तानंद का स्पर्श कर लेता है। कषायाग्नि शांत हो जाती है, पर-द्रव्यों के प्रति जो आसक्ति है वह नष्ट हो जाती है, अज्ञान का उन्मूलन होता है और हृदय में बोध-प्रदीप प्रज्वलित हो जाता है।’
बारह भावनाओं के अतिरिक्त चार भावनाओं का और उल्लेख मिलता है। वे है-(1) मैत्री, (2) प्रमोद, (3) करुणा, (4) उपेक्षा। बुद्ध ने इन चारों को ‘ब्रह्म विहार’ कहा है। पतंजलि ने-‘मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य-विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्।’ सुख, दुःख, पुण्य और पाप-इन भावों के प्रति क्रमशः मित्रता, करुणा, आनंद, प्रसन्नता और उपेक्षा का भाव धारण करने से चित्त प्रसन्न होता है, ऐसा कहा है।
(1) मैत्री भावना-मनुष्य के ज्ञात संबंधों की कड़ी बहुत छोड़ी है और अज्ञात की शंृखला बहुत प्रलंब है। ज्ञात स्पष्ट है और अज्ञात अस्पष्ट, इसलिए शत्रु-मित्र आदि की कल्पनाएँ खड़ी होती हैं। अज्ञात सामने आ जाए तो ये भाव स्वतः शांत हो सकते हैं। जन्म-मृत्यु की लंबी परंपरा कौन अपरिचित है? किंतु इसे साधारण लोग नहीं समझते। साधक आत्म-तुला के पथ पर अग्रसर होता है, उसे यह स्पष्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है, किंतु बहुत कम व्यक्तियों को अतीत ज्ञात होता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि मैं पहले भी था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। अतीत में था तो कहाँ था, कौन मेरे संबंधी थे, आदि प्रश्न स्वतः खड़े हो जाते हैं। इस दृष्टि से साधक का मन सबके प्रति मित्रभाव धारण कर लेता है। ‘मित्ति मे सव्वभूएसु, वेरं मज्झ न केणई’-मेरा सबके साथ मैत्री-भाव है। कोई मेरा शत्रु नहीं है।’ अंतश्चेतना से जैसे-जैसे यह भाव पुष्ट होता जाता है वैसे-वैसे साधक के मन में शत्रुता का भाव नष्ट होता जाता है। मित्र-मन सर्वत्र प्रसन्न रहता है और अमित्र-मन अप्रसन्न। शत्रु-मन अशांत, हिंसक, घृणायुक्त और क्लिष्ट रहता है। उसमें प्रतिशोध की आग निरंतर प्रज्वलित रहती है। मित्र-मन में ये सब दोष नष्ट हो जाते हैं। उसे भय नहीं रहता।
मैत्री-भावना का साधक स्वयं अपने को कष्ट में डाल सकता है, किंतु दूसरों को कष्ट नहीं देता। उसकी दृष्टि में पर-शत्रु जैसा कोई रहता ही नहीं। शत्रु का भाव ही अनिष्ट करता है। खलीफा अली अपने शत्रु के साथ वर्षों लड़ता रहा। एक दिन शत्रु हाथ में आ गया। उसकी छाती पर बैठ भाला मारने वाला ही था, इतने में शत्रु ने मुँह पर थूक दिया। अली को एक क्षण गुस्सा आया और बोला-‘आज नहीं लड़ेंगे।’ लोगों ने कहा, ‘कैसी मूर्खता कर रहे हैं?’ वर्षों से शत्रु हाथ आया और आप छोड़ रहे हैं।’ अली ने कहा-‘कुरान का वचन है-क्रोध में मत लड़ो।’ मुझे गुस्सा आ गया। शत्रु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा-‘इतने वर्षों क्या आप बिना क्रोध के लड़ रहे थे?’ अली ने उत्तर दिया-‘हाँ’। शत्रु चरणों में गिर पढ़ा। उसे पता ही आज चला कि बिना क्रोध के भी लड़ा जा सकता है। वह मित्र हो गया। लड़ने का हेतु भिन्न हो सकता है, किंतु क्रोध में नहीं लड़ना-यह मित्रता का परिचायक है। मैत्रीभाव का विराट् रूप जब सामने आता है तब द्वैत नहीं रहता। ‘आयतुले पयासु’-प्राणियों को अपने समान देखो-यह उसका फलितार्थ है।
(क्रमशः)

