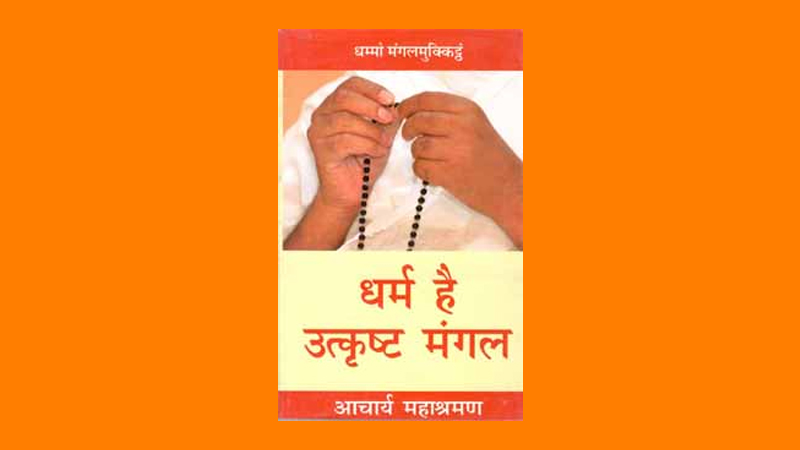
स्वाध्याय
धर्म है उत्कृष्ट मंगल
उपयोगिता अचेतन की
अजीव का अंतिम और अनस्तिकाय (जो अस्तिकाय नहीं है) द्रव्य है काल। उसे औपचारिक द्रव्य माना गया है, वह पर्याय है। चेतन और अचेतन पर उसका प्रभाव है। उसका गुण है वर्तमान-बीतता रहना। वह समक्षेत्र (मनुष्य क्षेत्र, अढ़ाई द्वीप) वर्ती माना गया है।
छः द्रव्य-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल। इनमें जीवास्तिकाय के अतिरिक्त जो पाँच द्रव्य हैं, वे अजीव हैं। उन्हें ‘अजीव के पाँच भेद’ कहा जाता है। केवल जीवास्तिकाय ही जीव है। वह द्रव्य से अनंत है। लोक ही उसका अस्तित्व का क्षेत्र है। छः द्रव्यों में काल के अतिरिक्त पाँच अस्तिकाय हैं। उन्हें ‘प×चास्तिकाय’ कहा जाता है। पाँचों के पीछे अस्तिकाय शब्द जुड़ा हुआ है। ‘अस्तिकाय’ एक समस्त पद है, दो शब्दों के योग से निष्पन्न शब्द है-अस्ति $ काय त्र अस्तिकाय। ‘अस्ति’ का अर्थ है प्रदेश (लघुतम और संयुक्त इकाई), काय का अर्थ है समूह, प्रदेश समूह को अस्तिकाय कहा जाता है। अस्तिकाय को सावयव (जिसके अवयव हैं) द्रव्य अथवा अवयवी भी कहा जा सकता है। अस्तिकाय का एक अर्थ और भी मिलता है-अस्ति अर्थात् जिसका अस्तित्व है और काय अर्थात् प्रदेश बहुलता। जिसका अस्तित्व है और जिसके बहुत प्रदेश हैं, वह अस्तिकाय है।
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय तीनोें द्रव्य की अपेक्षा एक-एक हैं। काल, पुद्गल और जीवास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा अनंत हैं। छः द्रव्यों में एक काल अप्रदेश है, शेष पाँच सप्रदेश हैं। छः द्रव्यों में एक पुद्गलास्तिकाय मूर्त (रूपी) है, शेष पाँच द्रव्य अमूर्त्त हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव-इनका प्रदेश-परिमाणतुल्य है, असंख्येय हैं। एक परमाणु जितने स्थान में अवगाहित होता है, समाविष्ट होता है वह एक आकाश-प्रदेश से अनंतरवर्ती दूसरे आकाश-प्रदेश में पहुँचने में जितनी कालावधि लगे, उसे समय (कालको लघुतम इकाई) कहा जा सकता है। एक आकाश-प्रदेश में एक परमाणु भी रह सकता है और अनंतप्रदेश पुद्गल-स्कंध भी उसमें समाविष्ट हो सकता है। एक जीव लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में भी रह सकता है और लोकव्यापी भी बन सकता है। संसार में जितने जीव और अचेतन पदार्थ अभी हैं, उतने ही सदा थे और उतने ही रहेंगे। उनमें किंचित् मात्र भी नैयून्य और आधिक्य नहीं हो सकता। एक ही आकाश-प्रदेश में छहों द्रव्यों का अंशरूपेण एक साथ समावेश हो सकता है। अपना-अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए वे एक साथ रहते हैं।
करणी बांझ न होय
जीव के दो प्रकार हैं-सिद्ध और संसारी। सिद्ध जीव अशरीर, अवाक् और अमन होते हैं। वे कृतकृत्य होते हैं। उन्हें क्रियात्मक रूप में कुछ भी करने की अपेक्षा भी नहीं होती और करने का वहाँ अवकाश भी नहीं होता। संसारी जीव शरीरधारी होते हैं। वे सर्वथा शरीरमुक्त कभी होते ही नहीं हैं। क्रिया वहीं होती है, जहाँ शरीर होता है। शरीर के बिना क्रिया हो ही नहीं सकती।
एक क्रिया संपन्न होने के बाद भी उसका प्रभाव कुछ समय तक आत्मा पर बना रहता है। इस प्रकार क्रियाकाल और प्रभावकाल-ये दो प्रकार के संसारी जीव से संबंधित काल हो जाते हैं। एक क्रिया संपन्न हो जाती है, परंतु उसका संस्कार पीछे छूट जाता है, आत्मा के साथ वह सम्बद्ध हो जाता है। बैल चला जाता है, किंतु उसका पद्चिÐ रह जाता है। उस संस्कार अथवा चिÐ को जैन पारिभाषिक शब्दावली में कर्म कहा जाता है। कर्म के कर्त्ता को उसका फल भी नियमानुसार मिलता है।
कर्म आठ हैं-(1) ज्ञानावरण, (2) दर्शनावरण, (3) अंतराय, (4) मोहनीय, (5) आयुष्य, (6) नाम, (7) गोत्र, (8) वेदनीय। इनमें प्रथम चार कर्म घाती और शेष चार कर्म अघाती कहलाते हैं। घाती कर्म आत्मगुणों (ज्ञान, दर्शन, अविकारता, शक्ति) का नाश अथवा घात (आच्छादन, अप्रकटन) करते हैं, इसलिए वे घाती एवं सर्वथा अशुभ कहलाते हैं। अघाती कर्म आत्मगुणों का नाश नहीं करते, इसलिए वे अघाती कहलाते हैं, वे केवल शुभ अथवा अशुभ रूप में फल देते हैं।
नव तत्त्वों में तीसरा तत्त्व पुण्य और चौथा तत्त्व पाप है। ये बंद्ध अवस्था में द्रव्य पुण्य-पाप तथा उदय-अवस्था में भाव पुण्य-पाप कहलाते हैं। आठ कर्मों में घाती कर्म केवल पाप कर्म होते हैं, अघाती कर्मों में प्रत्येक कर्म पुण्य और पाप दोनों प्रकार का होता है।
शुभ कर्म और अशुभ कर्म एक साथ एक ही समय में एक ही जीव के बंध सकते हैं। इसका हेतु अग्रलिखित है-आश्रव पाँच हैं-मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इनमें प्रथम चार आश्रव तो अशुभ ही होते हैं। उनसे अशुभ कर्मों का ही बंध होता है। योग आश्रव शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है। शुभ योग की विद्यमानता में निर्जरा के साथ पुण्यबंध होता है, यह तथ्य तो प्रसिद्ध है, किंतु उसी समय मिथ्यात्व आदि अन्य आश्रवों के कारण अशुभ कर्म का बंध भी होता है, यदि वे आश्रव रुद्ध नहीं हैं तो। एक सप्तम गुणस्थानवर्ती साधु अप्रमत्त अवस्था में ध्यानलीन है। उसके पुण्यबंध शुभयोग के कारण माना गया है, किंतु उसके उसी समय आश्रव के कारण पाप कर्म का बंध भी हो रहा है। दशम गुणस्थान में अशुभ कर्मों का बंध भी होता है। वहाँ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, नाम, गोत्र और अंतराय-इन छह कर्मों का बंध होता है। कषाय आश्रव अशुभ कर्मों को आकृष्ट करता है। आश्रव की भिन्नता के कारण कर्म की भिन्नता भी संभव बन जाती है। शुभ योग के कारण शुभ नाम व उच्च गोत्र का बंध होता है और कषाय आस्रव से ज्ञानावरणीय आदि अशुभ कर्मों का बंध होता है। कोई व्यक्ति क्रियारूप में क्रोध करता है-मन में गुस्सा, वाणी में आक्षेपात्मक शब्द और आँखें लाल, भृकुटि तनी हुई, डरावना चेहरा-यह स्थिति बन जाती है। किंतु इस प्रकार की क्रिया कषाय आश्रव नहीं, योग आश्रव है। इस प्रकार की स्थिति छठे गुणस्थान के बाद नहीं बनती।
(क्रमशः)

