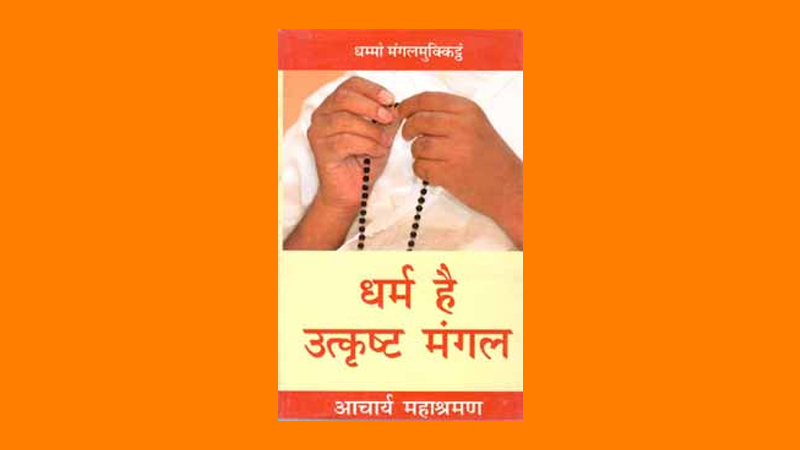
स्वाध्याय
धर्म है उत्कृष्ट मंगल
सम्यक्त्व के लिए न्यूनतम चारित्र का होना भी अनिवार्य है। उसके बिना सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार चारित्र के विकास के लिए भी दर्शन मोहनीय का विलय आवश्यक है। सम्यक्त्व प्राप्ति की यह अर्हता है कि उसमें (उस व्यक्ति में) चारित्र (अनन्तानुबंधी का विलय) भी एक सीमा तक हो। इसलिए सम्यक् दर्शन के लिए दर्शन मोह के विलय के साथ-साथ अर्हता स्वरूप न्यूनतम आचार (अनन्तानुबंधी कषाय का विलय) भी अनिवार्य है।
चारित्र मोहनीय के मुख्य भेद दो हैं-कषाय और नोकषाय। दर्शनमोहनीय एक ही है, वह है मिथ्यात्व मोहनीय। ताप डिग्री की तरतमता की भांति अथवा तीव्रता और मन्दता की अपेक्षा से उसके तीन भेद हो जाते हैं- सम्यक्त्व वेदनीय, मिश्र वेदनीय और मिथ्यात्व वेदनीय। दर्शन मोहनीय का सघन रूप मिथ्यात्व वेदनीय है, कुछ हल्का रूप मिश्र वेदनीय है और उससे भी हल्का रूप सम्यक्त्व वेदनीय है। मिथ्यात्व वेदनीय का क्षयोपशम होने से मिथ्यादृष्टि उज्ज्वल बनती है, परिणामस्वरूप जीव कुछ पदार्थों को सम्यक् श्रद्धा का विषय बना लेता है।
मिश्र वेदनीय का क्षयोपशम होने से सम्यक् मिथ्यादृष्टि उज्ज्वल बनती है, फलतः जीव बहुत पदार्थों को अपनी सम्यक् श्रद्धा का विषय बना लेता है। सम्यक्त्व वेदनीय का क्षयोपशम होने से जीव को क्षायोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है, पदार्थों पर सम्यक् श्रद्धान पुष्ट हो जाता है।
जब तक मिथ्यात्व वेदनीय का उदय रहता है, जीव को सम्यक् मिथ्यादृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक मिश्र वेदनीय का उदय रहता है, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक सम्यक्त्व वेदनीय का उदय रहता है, औपशमिक अथवा क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सकता।
मिथ्यादृष्टि, सम्यक् मिथ्यादृष्टि और सम्यक् दृष्टि- ये तीनों मोह-कर्म-विलय (क्षयोपशम आदि) जन्य भी हैं और मोहकर्म-उदय जन्य भी हैं। दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतिरूप यानी इन तीनों में जितना जितना विपरीत श्रद्धान अथवा यथार्थ श्रद्धान का अभाव है वह मोहकर्म-उदयजन्य है और जो सम्यक् श्रद्धान व विपरीत श्रद्धान का अभाव है वह मोहकर्म-विलय (क्षयोपशम आदि) जन्य है। यही कारण है कि मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियों, जो कि उदय रूप हैं, में भी इनका किसी रूप में उल्लेख है और मोहनीय कर्म की क्षयोपशमजन्य आठ उपलब्धियों में भी इनका उल्लेख है।
इसी प्रकार अज्ञान भी उदयभावजन्य और क्षयोपशमभावजन्य दोनों है। ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण ज्ञान-अभाव रूप जो अज्ञान है, वह उदयभावजन्य है और मिथ्यादृष्टि जीव का ज्ञान, जो कि मिथ्यात्व सहचारी होने के कारण अज्ञान कहलाता है, क्षायोपशमिक अज्ञान है। ज्ञान का हेतु ज्ञानावरण कर्म का विलय है। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि उसके पांच प्रकार हैं। सम्यक् चारित्र का संबंध चारित्रावरणीय मोह कर्म के विलय से है। उसके सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र आदि पांच प्रकार हैं एवं छठा प्रकार देशविरति है। 'सम्यक्' शब्द का अर्थ यथार्थ प्रशस्त अथवा संगत है।
ज्यों कोल्हू आदि के द्वारा तेल खलरहित होता है, मन्थनी के द्वारा घी छाछरहित होता है, अग्नि के द्वारा धातु मिट्टी रहित होती है, उसी प्रकार तप और संयम की साधना के द्वारा जीव का सर्वथा कर्मरहित होना मोक्ष है।
मोक्ष अवस्था को प्राप्त जीव मुक्त, सिद्ध, बुद्ध, परमात्मा, परमेश्वर आदि कहलाते हैं। वे संख्याित्ररांत यानी अनंत होते हैं। एकस्वरूप और एकाकार होने के कारण उन्हें 'एक' भी कहा जा सकता है। गुणों की दृष्टि से वे एक समान होते हैं, उनमें उपाधि जनित कोई भेद नहीं होता। वे अभेद के परम उदाहरण हैं। पूर्व (जिस स्थिति से वे मोक्ष को प्राप्त हुए हैं) अवस्था के अनुसार उनके अनेक भेद हो सकते हैं, जैसे- स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुषलिंग सिद्ध, नपुंसकलिंग सिद्ध, स्व-(जैन मुनिवेश)-लिंग सिद्ध, अन्य (जैनेतर मुनिवेश)-लिंग सिद्ध, गृहलिंग सिद्ध, उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध, मध्यम अवगाहना वाले सिद्ध, जघन्य अवगाहना वाले सिद्ध, ऊंचे लोक में मुक्त होने वाले सिद्ध, नीचे लोक में मुक्त होने वाले सिद्ध, तिरछे लोक में मुक्त होने वाले सिद्ध, समुद्र में मुक्त होने वाले सिद्ध, अन्य जलाशयों में मुक्त होने वाले सिद्ध आदि।
सर्वार्थसिद्ध विमान से बारह योजन ऊपर ईषत् प्राग्भारा नामक पृथ्वी है। वह छत्राकार में अवस्थित है। उसकी लम्बाई और चौड़ाई पैंतालीस लाख योजन की है। उसकी परिधि उस (लम्बाई-चौड़ाई) से तिगुनी है। मध्य भाग में उसकी मोटाई आठ योजन की है। वह क्रमशः पतली होती होती अंतिम भाग में मक्खी की पंख से भी अधिक पतली हो जाती है। वह श्वेत स्वर्णमयी, स्वभाव से निर्मल और उत्तान (सीधे) छत्राकार वाली है। उस 'सीता' नाम की ईषत् प्राग्भारा पृथ्वी से एक योजन ऊपर लोक का अन्त (अग्रभाग) है। उस योजन के उपरिवर्ती कोस के छठे भाग में सिद्धों की अवस्थिति होती है। सिद्ध अनादि-अनन्त भी होते हैं और सादि-अनन्त भी होते हैं। 'अनादि' का यह अर्थ नहीं कि वे कभी संसारी थे ही नहीं, सदा सिद्ध ही थे। बहुत काल की अपेक्षा वे अनादि कहलाते हैं।

