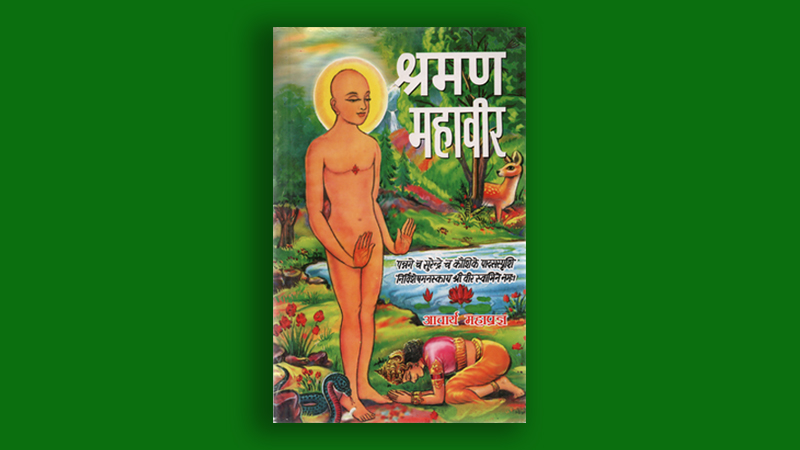
स्वाध्याय
असंग्रह का वातायन : अभय का उच्छ्वास
मैंने मृदु-मंद स्वर में कहा, 'यह शरीर धर्म का आद्य साधन है। शरीर ही धर्म का आद्य साधन नहीं है, वह शरीर धर्म का आद्य साधन है जो आसक्ति के नागपाश से मुक्त हो चुका है।'
हमारी यात्रा समस्वरता में सम्पन्न हो गई। भगवान् के शरीर पर वह दिव्य दूष्य उपेक्षा के दिन बिता रहा था। न भगवान् उसका परिकर्म कर रहे थे और न वह उनकी शोभा बढ़ा रहा था।
साधना का दूसरा वर्ष और पहला मास। भगवान् दक्षिण वाचाला से उत्तर वाचाला को जा रहे थे। दोनों सन्निवेशों के बीच में दो नदियां बह रह थीं– सुवर्णाबालुका और रूप्यबालुका। सुवर्णाबालुका के किनारे पर कंटीली झाड़ियां थीं। भगवान् उनके पास होकर गुजर रहे थे। भगवान् के शरीर पर पड़ा हुआ वस्त्र कांटों में उलझ गया। भगवान् रुके नहीं, वह शरीर से उतर नीचे गिर गया। भगवान् ने उस पर एक दृष्टि डाली और उनके चरण आगे बढ़ गए।
भगवान् के पास अपना बताने के लिए केवल शरीर था और
वास्तव में उनका अपना था चैतन्य। वह चैतन्य जिसके दोनों पाश्वों में निरन्तर प्रवाहित हो रहे हैं दो निर्झर। एक का नाम है आनन्द और दूसरे का नाम है वीर्य।
पहले शरीर के साथ प्रेम का सम्बन्ध था, अब उसके साथ विनिमय का सम्बन्ध है। पहले उधार का व्यापार चल रहा था, अब नकद का व्यापार चल रहा है। भगवान् का अधिकांश समय ध्यान में बीतता है। वे बहुत कम खाते हैं, उतना-सा खाते हैं जिससे यह गाड़ी चलती रहे।
शरीर के साथ उनके सम्बन्ध बहुत स्वस्थ थे। वे उसे आवश्यक पोषण देते थे और वह उन्हें आवश्यक शक्ति देता था। वे उसे अनावश्यक पोषण नहीं देते थे और वह उन्हें अनावश्यक (विकारक, उत्तेजक या उन्मादक) शक्ति नहीं देता था।
भगवान् का अपना कोई घर नहीं था। उनका अधिकतम आवास शून्यगृह, देवालय, उद्यान और अरण्य में होता था। कभी-कभी श्मशान में भी रहते थे। साधना के प्रथम वर्ष में वे कोल्लाग सन्निवेश से मोराक सन्निवेश पहुंचे। उसके बहिर्भाग में घुमक्कड़ तापसों का आश्रम था। वे वहां गए। आश्रम का कुलपति भगवान् के पिता सिद्धार्थ का मित्र था। वह भगवान् को पहचानता था। एक तापस ने भगवान् को आश्रम में आते हुए देखा। उसने कुलपति को सूचना दी। वह अपने साधना-कुटीर से बाहर आया। उसने महावीर को पहचान लिया। वह आतिथ्य के लिए सामने गया। दोनों ने एक-दूसरे का अभिवादन किया।
कुलपति के निवेदन पर महावीर एक दिन वहीं रहे। दूसरे दिन वे आगे के लिए प्रस्थान करने लगे। कुलपति ने कहा, 'मुनिवर! यह आश्रम आपका ही है। आप इसमें निःसंकोच भाव से रहें। अभी आप प्रस्थान के लिए प्रस्तुत हैं। मैं आपकी इच्छा में विघ्न उपस्थित नहीं करूंगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इस वर्ष का वर्षावास यहीं बिताएं।'
महावीर वहां से चले। कई महीनों तक आसपास के प्रदेश में घूमे। आश्रम से बंधकर गए थे, अतः वर्षावास के प्रारम्भ में पुनः वहीं लौट आए। इसे आश्चर्य ही मानना होगा कि अपनी धुन में अलख जगाने वाला एक स्वतंत्रता-प्रेमी साधक कुलपति के बंधन में बंध गया।
कुलपति ने महावीर को एक झोपड़ी दे दी। वे वहां रहने लगे। उनके सामने एक ही कार्य था और वह था ध्यान–भीतर की गहराइयों में गोते लगाना और संस्कारों की परतों के नीचे दबे हुए अस्तित्व का साक्षात्कार करना। वे अपनी झोपड़ी की ओर भी ध्यान नहीं देते तब आवासीय झोपड़ी की ओर ध्यान देने की उनसे आशा ही कैसे की जा सकती थी? महावीर की यह उदासीनता झोपड़ी के अधिकारी तापस को खलने लगी। उसने महावीर से अनुरोध किया, 'आप झोपड़ी की सार-संभाल किया करें।'
समय का चरण आगे बढ़ा। बादल आकाश में घिर गए। रिमझिम रिमझिम बूंदे गिरने लगीं। ग्रीष्म ने अपना मुंह वर्षा के अवगुंठन से ढक लिया। उसके द्वारा पुरस्कृत ताप शीत में बदल गया। भूमि के कण-कण में रोमांच हो आया। उसका हरित परिधान बरबस आखों को अपनी ओर खींचने लगा।

