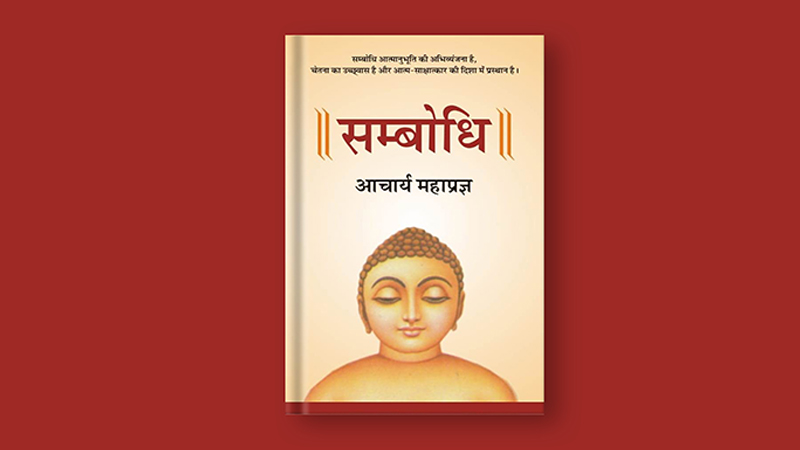
स्वाध्याय
संबोधि
अस्तित्व का बोध असीम है। शब्द ससीम है। ससीम में असीम को बांधने से भ्रम पैदा होता है। इसलिए सभी ने स्वरूप अस्तित्व को अवाच्य कहा है। 'अवाङ्गनसो गोचरम्' वाणी और मन का वह विषय नहीं बनता। 'नेति नेति' यह भी नहीं है, यह भी नहीं है– जो शेष रह जाता है वह 'अस्तित्व' है। 'लाओत्से' ने कहा है जो उसके संबंध में लिखूंगा तो वह झूठ होगा। जो लिखना है वह लिखा नहीं जाएगा। जब चीन के सम्राट ने लिखने को विवश कर दिया, तब यह लिखते हुए प्रारंभ किया कि 'बड़ी भूल हुई जा रही है–'जो कहना है वह कहा नहीं जाता और जो नहीं कहना है वह कहा जाएगा।' मैं जानकर लिखने बैठा हूं, इसलिए जो आगे पढ़ें वे जानकर पढ़ें कि सत्य बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता और जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं हो सकता।' महावीर ने सत्य को अवक्तव्य कहा है। इसमें भी यही कहा है कि यहां न मन पहुंचता है, न शब्द और न बुद्धि। अस्तित्व का न आकार है, न रूप है, न वह स्त्री, न पुरुष, न नपुंसक है, न जाति है आदि। बुद्ध ने इसके संबंध में प्रश्न करने से भी मना कर दिया कि कोई पूछे ही नहीं। वस्तुतः यह शब्द का विषय नहीं, अनुभूति का है। शब्दों को अनुभूति समझ ली जाए तो यात्रा रुक जाती है। शब्द सिर्फ संकेतवाहक हैं।
२३. ग्रामे वा यदि वाऽरण्ये, न ग्रामे नाप्यरण्यके।
रागद्वेषलयो यत्र, तत्र सिद्धिः प्रजायते ॥
सिद्धि गांव में भी हो सकती है और अरण्य में भी हो सकती है। वह न गांव में हो सकती और न अरण्य में। सिद्धि वहीं होती है, जहां राग और द्वेष का विलय हो जाता है।
साधना का घनिष्ठ संबंध आत्मा से है। इसलिए साधना आत्मा ही है। आत्मा की सिद्धि में बाहरी निमित्तों का खास महत्त्व नहीं है। लेकिन फिर भी वे बनते हैं क्योंकि वे सिद्धि में सहायक हैं। कहीं-कहीं हम साधनों का उल्टा प्रभाव भी देखते हैं। एकांत स्थान जहां आत्म-साधन में सहायक है वहां वह बाधक भी बन जाता है। इसलिए एकांततः हम किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकते। साधना के बाहरी निमित्तों पर बल देने की अपेक्षा आंतरिक पक्ष पर बल देना अधिक उपयोगी है।
साधना का आंतरिक पक्ष है– राग-द्वेष पर विजय। जो राग-द्वेष का विजेता है, उसके लिए गांव, नगर, उपवन, नदी, तट आदि सब समान हैं।
केवल बाह्य साधनों से साध्य सिद्ध नहीं होता। इस श्लोक में उन एकांतवासियों का खंडन है, जो यह कहते थे कि साधना जंगल में ही होती है या नगर में ही होती है। भगवान् महावीर ने दोनों का समन्वय कर साधना का क्षेत्र सबके लिए खोल दिया।
२४. न मुण्डितेन श्रमणः, न चोंकारेण ब्राह्मणः।
मुनिर्नारण्यवासेन, कुशचीरैर्न तापसः।।
सिर को मूंडा लेने मात्र से कोई श्रमण नहीं होता, ओंकार को जप लेने मात्र से कोई ब्राह्यण नहीं होता, अरण्य में निवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं होता और कुश के बने हुए वस्त्र पहनने मात्र से कोई तापस नहीं होता।
२५. श्रमणः समभावेन, ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणः।
ज्ञानेन च मुनिलेकि, तपसा तापसो भवेत्॥
श्रमण वह होता है, जो समभाव रखे। ब्राह्मण वह होता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करे। मुनि वह होता है, जो ज्ञान की उपासना करे और तापस वह होता है, जो तपस्या करे।
'बालः पश्यति लिङ्ग, मध्यमबुद्धिर्विचारयति वृत्तम् ।
आगमतत्त्वं तु बुद्धः, परीक्षते सर्वयत्नेन॥'
तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं-
(१) बाल-सामान्यजन, जो विवेक और बुद्धि से परिहीन है वह केवल बाह्य वेष-लिंग को देखता है। उसकी दृष्टि बाह्य आकार-प्रकार से दूर नहीं जाती।

