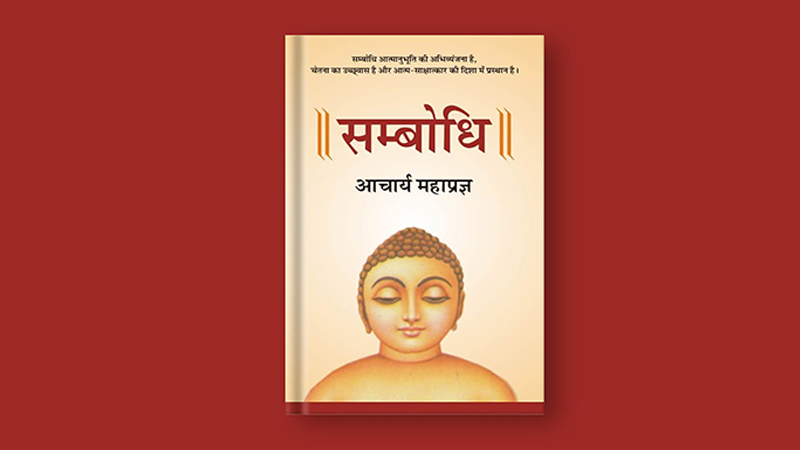
स्वाध्याय
संबोधि
(२) मध्यम बुद्धि– वह कुछ परिपक्व होता है। बुद्धि गहरी तो नहीं किंतु व्यावहारिक दृष्टि में पटु होती है। वह देखता है आचार-विचार को। वह देखता है कि रीति-रिवाज, नियमों का जो ढांचा बना हुआ है, उस चौखटे में पूरा ठीक बैठता है या नहीं।
(३) तीसरा जो ज्ञानी है, जिसने सत्य का स्पर्श किया है, जाना है कि बंधन राग-द्वेष है, अध्यात्म समता है, राग-द्वेष की परिक्षीणता आत्म-रमण है, उसका परीक्षण यही होता है कि साधक कहां तक पहुंचा है? उसका आकर्षण- बिन्दु-जगत् है या आत्मा? अविद्या का बंधन टूटा है या नहीं? वह यह नहीं देखता कि लिंग, चिह्न–वेष कैसा है? आचरण कैसा है? इनका महत्त्व बाह्य दृष्टि से है, अंतर्दृष्टि से नहीं।
महावीर की दृष्टि भी अंतःस्थित है। वेष से अधिक महत्त्व है उनकी दृष्टि में समता, ज्ञान-दर्शन और चारित्र का। वेष है और ज्ञान-दर्शन नहीं है तो महावीर की दृष्टि में यह केवल आत्मघाती है। इसलिए वे कहते हैं– केश-लुंचन या सिर को मुंडा लेने से कोई श्रमण नहीं होता। श्रमण वह होता है जो सर्वदा समस्त स्थितियों में संतुलन बनाए रखता है, राग और द्वेष की तरंगें जिसे प्रकंपित नहीं करती। ब्रह्म-आत्मा में निवास करने वाला ब्राह्मण होता है। मुनि वह होता है जो सम्यग् ज्ञान में स्थित है और तापस वह है जो स्वभाव की दिशा में अग्रसर होता है। चारों के चार मार्ग भिन्न नहीं हैं। शब्द भिन्न हैं, दिशा सबकी आत्मोन्मुखी है। एक दिशा का परिवर्तन ही जीवन का परिवर्तन है। वेष-भूषा है संत की और जीवन का मुख है संसार की तरफ तो उससे वांछित सिद्धि नहीं होती।
२६. कर्मणा ब्राह्मणो लोकः कर्मणा क्षत्रियो भवेत्।
कर्मणा जायते वैश्यः, शूद्रो भवति कर्मणा ॥
ब्रह्मविद्या का कर्म करने वाला ब्राह्मण, सुरक्षा का कर्म करने
वाला क्षत्रिय, व्यवसाय-कर्म करने वाला वैश्य और सेवाकर्म करने वाला शूद्र होता है।
२७. न जातिर्न च वर्णोऽभूद्, युगे युगलचारिणाम् ।
ऋषभस्य युगादेषा, व्यवस्था समजायत ।।
यौगलिक युग में न कोई जाति थी और न कोई वर्ण था। भगवान् ऋषभ के युग में जाति और वर्ण की व्यवस्था का प्रवर्तन हुआ।
२८. एकैव मानुषी जातिराचारेण विभज्यते।
जातिगर्वो महोन्मादो, जातिवादो न तात्त्विकः ॥
मनुष्य जाति एक है। उसका विभाग आचार अथवा वर्ण के आधार पर होता है। जाति का गर्व करना सबसे बड़ा उन्माद है क्योंकि जातिवाद तात्त्विक वस्तु नहीं है।
२९. जातिवर्णशरीरादि-बाद्यैर्भेदैर्विमोहितः ।
आत्माऽऽत्मसु घृणां कुर्याद्, एष मोहो महान् नृणाम् ।।
जाति, वर्ण, शरीर आदि बाह्य भेदों से विमूढ बनकर एक आत्मा दूसरी आत्मा से घृणा करे-यह मनुष्यों का महान् मोह है।
जाति व्यवहाराश्रित है और धर्म आत्माश्रित। आत्म-जगत् में प्रत्येक प्राणी समान है। वहां जातियों के विभाग इन्द्रियों के आधार पर हैं। धर्म के आधार पर व्यक्तियों का बंटवारा करना धर्म को कभी प्रिय नहीं है। धर्म के उपदेष्टा-ऋषियों ने कहा-प्रत्येक प्राणी को अपने जैसा समझो। उनकी दृष्टि में भाषा-भेद, वर्ण-भेद, धर्म-भेद, जाति-भेद आदि का महत्त्व नहीं था। जातियों की कल्पना केवल कर्म-आश्रित की गयी थी। 'मनुष्य जाति एक है' ऐसा कहकर सबमें भ्रातृत्व के बीज का वपन किया था। किन्तु मनुष्य इस इकाई सत्य को भूलकर अनेकता में विभक्त हो गया। वह जाति के मद में एक को ऊंचा और एक को नीचा देखने लगा। फलस्वरूप समाज में घृणा की भावना फैली।

