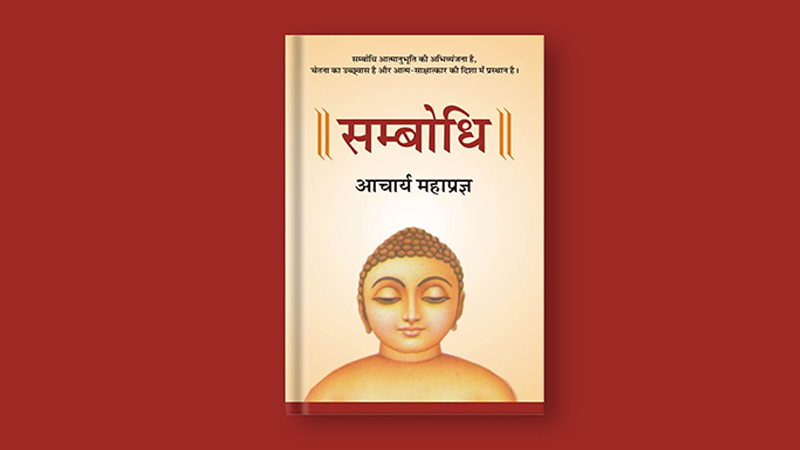
स्वाध्याय
संबोधि
भगवान् प्राह
२१. अर्थजानर्थजा चेति, हिंसा प्रोक्ता मया द्विधा।
अनर्थजां त्यजन्नेष, प्रवृत्तिं लभते सतीम्॥
भगवान् ने कहा-मैंने हिंसा के दो प्रकार बतलाए हैं-अर्थजा और अनर्थजा। गृहस्थ अनर्थजा-अनावश्यक हिंसा का परित्याग कर सकता है और
जितनी मात्रा में वह उसका त्याग करता है, उतनी मात्रा में उसकी प्रवृत्ति सत् हो जाती है।
२२. आत्मने ज्ञातये तद्वद्, राज्याय सुहृदे तथा।
या हिंसा क्रियते लोकैरर्थजा सा किलोच्यते।।
अपने लिए, परिवार, राज्य और मित्रों के लिए जो हिंसा की जाती है, वह अर्थजा हिंसा कहलाती है।
२३. परस्परोपग्रहो हि, समाजालम्बनं भवेत्।
तदर्थं क्रियते हिंसा, कथ्यते सापि चार्थजा॥
परस्पर एक-दूसरे का सहयोग करना समाज का आधारभूत तत्त्व है। इस दृष्टि से समाज के लिए जो हिंसा की जाती है, उसे भी अर्थजा हिंसा कहा जाता है।
२४. कुर्वन्नप्यर्थजां हिंसां, नासक्तिं कुरुते दृढाम्।
तदानीं लिप्यते नासौ, चिक्कणैरिह कर्मभिः॥
अर्थजा हिंसा करते समय जो प्रबल आसक्ति नहीं रखता, वह चिकने कर्म-परमाणुओं से लिप्त नहीं होता।
२५. हिंसा न क्वापि निर्दोषा, परं लेपेन भिद्यते।
आसक्तस्य भवेद् गाढोऽनासक्तस्य भवेन्मृदुः।।
हिंसा कहीं भी निर्दोष नहीं होती परन्तु उसके लेप में अंतर होता है। आसक्त का लेप गाढ़ और अनासक्त का लेप मृदु होता है।
हिंसा हिंसा है। वह कभी अहिंसा नहीं होती और अहिंसा कभी हिंसा नहीं होती। अहिंसा अबंधन है और हिंसा बंधन। अहिंसा में भावों की तरतमता नहीं होती। उसका सदा पवित्र भावनाओं से संबंध है। हिंसा में राग और द्वेष की नियतता है। देखना यही है कि राग और द्वेष का प्रवाह कितना तीव्र है। एक व्यक्ति साधारण कर्म करता हुआ भी उसमें अनुरक्त होता है और एक असाधारण कार्य करता हुआ भी उसमें आसक्त नहीं रहता।
महाराज जनक की एक घटना से यह स्पष्ट हो जाता है। एक बार जनक किसी अन्य राजा के अतिथि बने। वे कुछ दिन वहां रुककर जब जाने लगे तो राजा ने अतिथि से पूछा 'यहां आपको कैसा लगा?' जनक का भी संक्षिप्त-सा सहज उत्तर था-'बहुत बड़े भव्य महल में एक तुच्छ जीवन।' वहां से आते हुए मार्ग में एक साधु की कुटिया थी। कुछ दिन वहां रहने का भी सौभाग्य मिला। वे सत्संग, ध्यान, भजन आदि नियमित कार्यों में सतत भाग लेते रहे। जब वहां से विदा होने लगे तो संत ने सहज प्रश्न किया- 'यहां आपको कैसा लगा?' जनक का भी संक्षित उत्तर था 'एक छोटी-सी झोंपड़ी में एक महान् जीवन।'
जिस कार्य में आसक्ति की मात्रा अधिक होती है वहां कर्म का बंधन भी दृढ़ होता है, उसका फल भी कटुक होता है। जहां आसक्ति नहीं है वहां कर्म का बंधन गाढ़ नहीं होता और फल भी दारुण नहीं होता। असत् कर्म से बंधन अवश्य होता है, भले वह अनासक्तिपूर्वक हो या आसक्तिपूर्वक। जैन दर्शन में अनासक्ति का पूर्णरूप वहां निखार पाता है जहां सत् और असत् के प्रति भी आकांक्षा छूट जाती है। सत् कर्म में भी पुण्य कर्म प्रवाहित होता रहता है किन्तु उसका फल दारुण नहीं होता। आसक्ति की तीव्रता और अतीव्रता से उसके फल में वैसा ही रस पड़ता है।

