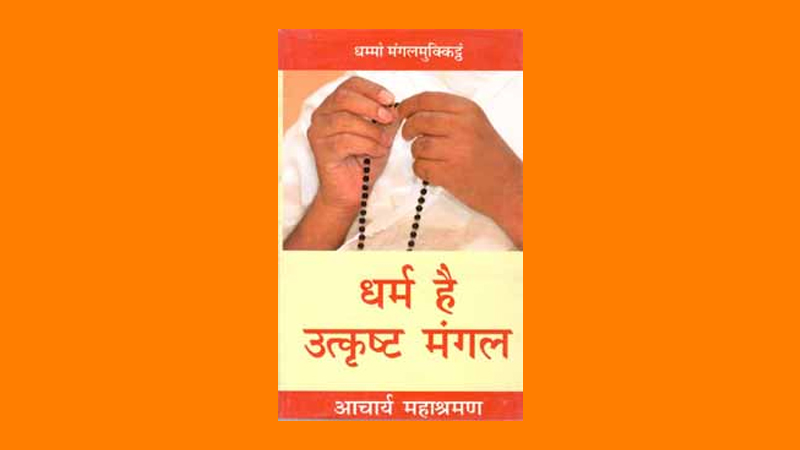
स्वाध्याय
धर्म है उत्कृष्ट मंगल
कायोत्सर्ग, अन्तर्यत्रा, दीर्घश्वास प्रेक्षा, चैतन्य केन्द्र प्रेक्षा आदि रक्षा ध्यान पद्धति के काल-प्रतिबद्ध प्रयोग हैं। एक निश्चित समय तक इनका अभ्यास किया जा सकता है, निरंतर नहीं किया जा सकता। समता, जागरूकता, निवृत्तियुक्त प्रवृत्ति ये प्रेक्षाध्यान के काल अप्रतिबद्ध प्रयोग हैं। इनका प्रयोग निरंतर किया जा सकता है।
समता का अर्थ है-राग द्वेषमुक्त क्षण में जीना। यही धर्म है, यही अहिंसा है और यही ध्यान है। प्रेक्षा के साधक की गमन, शयन, भोजन बातचीत आदि सभी क्रियाएं राग-द्वेष के विकल्पों से मुक्त और प्रेक्षा का साधक मृत क्रिया नहीं, सजीव क्रिया करता है। हर क्रिया के साथ उसकी चेतना जुड़ी हुई रहती है। वह चलते समय केवल चलने, बोलते समय केवल बोलने और खाते समय केवल खाने का अभ्यास करता है। यह भाव-क्रिया या जागरूकता का प्रयोग है।
प्रेक्षा का साधक निवृत्तिप्रधान प्रवृत्ति का अभ्यास करता है। उसकी हर प्रवृत्ति पर निवृत्ति का अंकुश रहता है। अनावश्यक न सोचना, अनावश्यक न बोलना, अनावश्यक शारीरिक चेष्टा न करना, निवृत्ति- प्रधान प्रवृत्ति का लक्षण है। कुछ साधक दिन में १-२ घंटे मौन का अभ्यास करते हैं। यह मौन का एक प्रकार है। मौन का दूसरा प्रकार है अनावश्यक न बोलना बिना जरूरत एक शब्द का भी प्रयोग न करना। आवश्यकतावश बोलते समय भी अनावश्यक जोर से न बोलना, धीरे बोलना।
काल-अप्रतिबद्ध प्रेक्षाध्यान के प्रयोग को अपनाकर हम दैनिक जीवन में प्रेक्षाध्यान को प्रतिष्ठित कर सकते हैं।
बन्धन-मुक्ति का प्रयोग
संसार-परिभ्रमण का कारण है आश्रव। उससे कर्म का संचय होता है। उसका विपरीत तत्त्व है निर्जरा। उससे कर्म-संचय रिक्त होता है। इन दोनों के मध्य एक तत्त्व और है, वह है संवर। उसका अर्थ है कर्म-संचय को रोकना। संसार-परिभ्रमण से मुक्ति पाने के लिए संवर और निर्जरा इन दोनों की आराधना आवश्यक है। संवरविहीन निर्जरा का बहुत मूल्य नहीं होता। उस निर्जरा की शक्ति प्रबल होती है। जिसकी आधारशिला संवर होता है।
आगम-साहित्य में निर्जरा के बारह भेद बतलाये गए हैं। उनमें बारहवां भेद है-व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग छोड़ने का प्रयोग है, त्याग का प्रयोग है, बन्धन-मुक्ति का प्रयोग है। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी तत्त्व है उसको छोड़ना व्युत्सर्ग है अथवा यह भी कहा जा सकता है कि व्युत्सर्ग अकेला बनने का प्रयोग है। वह परावलम्बन से मुक्त होकर स्वावलम्बन को स्वीकारने का प्रयोग है।
व्युत्सर्ग के मुख्य भेद दो हैं द्रव्य-व्युत्सर्ग और भाव-व्युत्सर्ग। द्रव्य व्युत्सर्ग का सम्बन्ध मुख्यतः स्थूल अथवा बाह्य जगत् से है। भाव व्युत्सर्ग का सम्बन्ध मुख्यतः सूक्ष्म अथवा आन्तरिक जगत से प्रतीत होता है। द्रव्य व्युत्सर्ग के चार प्रकार हैं-गण-व्युत्सर्ग, शरीर-व्युत्सर्ग, उपधि-व्युत्सर्ग और भक्तपान-व्युत्सर्ग। जैन परम्परा में दो प्रकार को साधना मान्य रही है वैयक्तिक साधना और संघबद्ध साधना। संघीय साधना को बहुत मूल्यवत्ता है। संघ के सहारे साधक बहुत आगे बढ़ सकता है। संघ में सारणा-वारणा हो सकती है। शारीरिक अस्वास्थ्य और मानसिक अस्वास्थ्य की स्थितियों में संघ का आश्वासन, सहारा और विश्वास प्राप्त होता है। यदि ऐसा न हो तो फिर संघीय साधना की मूल्यवत्ता पर प्रश्नचिह लग जाता है। साधना-जीवन में जहां संघ का महत्त्व है वहीं एक भूमिका में संघ को छोड़ने का भी महत्त्व है। एकाकी साधना का भी बड़ा मूल्य है। संघीय साधना के लिए जहां सामान्य योग्यता सम्पन्न व्यक्ति भी योग्य होता है, वहीं वैयक्तिक/एकाकी साधना के लिए विशिष्ट योग्यता अपेक्षित रहती है। उस योग्यता से सम्पन्न साधक गण-व्युत्सर्ग कर एकोऽहमस्मि–'मैं अकेला हूं' की विशिष्ट अनुभूति कर सकता है। रागमुक्तता व अप्रतिबद्धता की दिशा में सही ढंग से आगे बढ़ सकता है।
शरीर साधना का साधन है। उसके लिए शरीर का भरण-पोषण भी अपेक्षित है किन्तु शरीर के प्रति भी ममत्व नहीं होना वांछनीय है। उसकी साज-सज्जा व विभूषा का भाव त्याज्य है। एक भूमिका में साधना शरीर- निरपेक्ष बन जाती है।
अहमन्यः पुद्गलश्चान्यः 'मैं अलग हूं, शरीर अलग है' का भाव पुष्ट हो जाता है। शरीर की सार संभाल छोड़ देना ही वहां साधना बन जाती है। भगवान ऋषभ की स्तुति में चौबीसी में कहा गया है- 'इम तन सार तजी करी प्रभु केवल पाया'- इस प्रकार शरीर की सार-संभाल छोड़ कर प्रभु ने केवलज्ञान प्राप्त किया। शरीर की पकड़ को छोड़ ममत्व-मुक्त बनने को साधना, शरीर का शिथिलीकरण व स्थिरीकरण कायोत्सर्ग है। इस प्रकार की साधना शरीर के रहते हुए भी उसके व्युत्सर्ग की साधना है। वस्त्र आदि उपकरण साधना में सहायक बनते हैं। विशेष साधना में उनका विसर्जन भी किया जाता है। उपधि का सर्वथा उत्सर्जन साधना का विशेष प्रयोग है।

