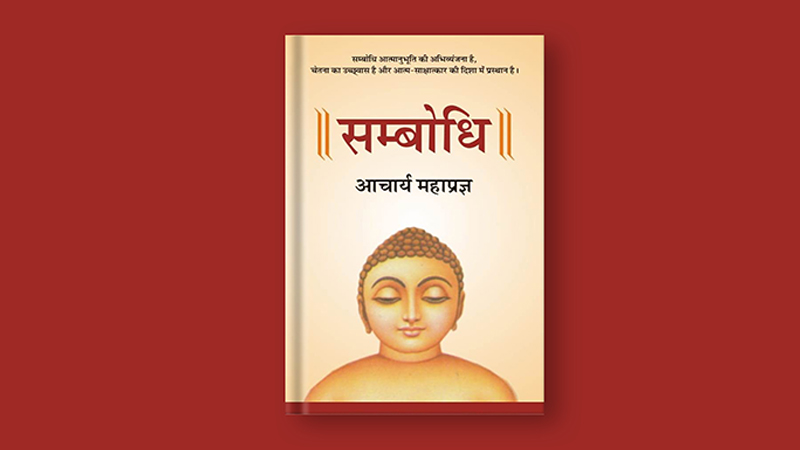
स्वाध्याय
संबोधि
वे ही क्रियाकांड महत्त्वपूर्ण और उपादेय हैं जो व्यक्ति को आत्मा के निकट ले जाते हैं। जिनसे आत्मा दूर होती है वे कैसे उपादेय हो सकते हैं। योगसार में कहा है-'गृहस्थ हो या साधु, जो आत्मस्थ होता है, वही सिद्धि सुख को प्राप्त कर सकता है, ऐसा जिन भाषित है।' परमात्म प्रकाश में कहा है- 'संयम, शील, तप, दर्शन और ज्ञान सब आत्म शुद्धि में है। आत्म शुद्धि से ही कर्मक्षय होता है, इसलिए आत्म शुद्धि प्रधान है।'
महावीर कहते हैं-गलत दिशा में चलकर कोई भी व्यक्ति अभीष्ट को प्राप्त नहीं कर सकता। इससे तो वह वहीं पहुंचता है जहां पहुंचना नहीं चाहता। साध्य और साधन दोनों की शुद्धि अत्यंत अपेक्षित है।
१७. आत्मानः सदृशाः सन्ति, भेदो देहस्य दृश्यते।
आत्मनो ये जुगुप्सन्ते, महामोहं व्रजन्ति ते॥
स्वरूप की दृष्टि से सब आत्माएं समान हैं। उनमें केवल शरीर
का अन्तर होता है। जो आत्माओं से घृणा करते हैं, वे महा-मोह में फंस जाते हैं।
१८. उच्चगोत्रो नीचगोत्रः, सामग्रया कथ्यते जनैः।
न हीनो नातिरिक्तश्च, क्वचिदात्मा प्रजायते॥
प्रशस्त सामग्री के प्राप्त होने से आत्मा उच्व गोत्र वाला और
अप्रशस्त सामग्री के प्राप्त होने से वह नीचगोत्र वाला कहलाता है। वस्तुतः कोई भी आत्मा किसी भी आत्मा से न उच्च है और न नीच।
१९. प्रज्ञामदं नाम तपोमदञ्च, निर्णामयेद् गोत्रमदञ्च धीरः।
अन्यं जनं पश्यति बिम्बभूतं, न तस्य जातिः शरणं कुलं वा॥
धीर पुरुष वह होता है जो बुद्धि, तप और गोत्र के मद का उन्मूलन करे। जो दूसरे को प्रतिबिम्ब की भांति तुच्छ मानता है, उसके लिए जाति या कुल शरणभूत नहीं होते।
जो धार्मिक हैं, किन्तु जिनके अज्ञान का आवरण हटा नहीं है, वे धार्मिक होते हुए भी वृत्तियों से धार्मिक नहीं होते। उनकी दृष्टि अभी बाहर स्थित है। वे बाह्य वातावरण से प्रभावित हैं तथा बाह्य वस्तुओं के संयोग-वियोग से महान् और क्षुद्र की कल्पनाएं करते हैं। धर्म का अभ्युदय होने पर बाह्य वस्तुओं का वैशिष्ट्य समाप्त हो जाता है। एक साथ दो चीजें नहीं रह सकती।

