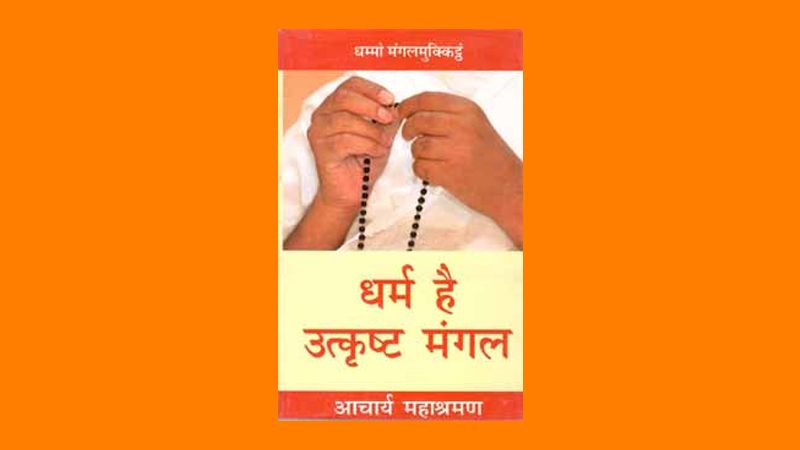
स्वाध्याय
धर्म है उत्कृष्ट मंगल
मोहकर्म को औदयिक प्रकृतियों– कोध, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष आदि को निषेधात्मक भाव तथा उसकी क्षायोपशमिक प्रकृतियों-क्षमा, विनम्रता, प्रमोद-भाव, अद्वेष आदि को विधायक भाव कहा जा सकता है।
उदय और क्षयोपशम भाव का संघर्ष चलता रहता है। उदय भाव का प्राबल्य होने पर क्षयोपशम शक्तिहीन हो जाता है और क्षयोपशम सबल होने पर उदय भाव पराभूत हो जाता है। क्षयोपशम भाव को पुष्ट करना और उदय-भाव को कृश करना-यही
है अध्यात्म-साधना।
इन पांच भावों में अतिरिक्त एक भाव और आगम-साहित्य में उपलब्ध होता है, वह है सान्निपातिक भाव। यह स्वतन्त्र भाव नहीं है। यह अनेक भावों के मिश्रण से निष्पन्न होता है। इसके द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुः संयोगी और पंचसंयोगी इस प्रकार अनेक वर्गीकरण उपलब्ध होते हैं।
जैसे- द्विसंयोगी– १. औदयिक, औपशमिक (मनुष्य और उपशांत मोह)
२. औदयिक, क्षायिक (मनुष्य और क्षीण कषाय) आदि-आदि।
त्रिसंयोगी– १. औदयिक, औपशमिक, क्षायिक (मनुष्य, उपशांत-मोह, क्षायिक, सम्यग दृष्टि)।
२. औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक (मनुष्य, उपशांत मोह और मतिश्रुतज्ञानी) आदि-आदि।
चतुः संयोगी– औदयिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक (मनुष्य, क्षायिक सम्यग्दृष्टि, पंचेन्द्रिय और जीव) आदि-आदि।
पंचसंयोगी– औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक (मनुष्य, उपशांतमोह, क्षायिक सम्यग्दृष्टि, पचेन्द्रिय और जीव)। क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव उपशम श्रेणी लेता है तब ग्यारहवें गुणस्थान में यह स्थिति बनती है।
विभिन्न विवक्षाओं से सान्निपातिक भाव के अनेक भेद बतलाए गए हैं।
नियति और पुरुषार्थ का समन्वय
सत्य के शोध में अनाग्रह और सत्य की साधना में आग्रह होना चाहिए। यथार्थ के आकाश में उड़ान भरने के लिए अनाग्रह और आग्रह इन दोनों पंखों की आवश्यकता रहती है। जिस व्यक्ति ने केवल अन्ध आग्रह करना ही सीखा है, उसने सत्य के प्रवेशद्वार को बन्द कर दिया। जिसने केवल अनाग्रह को ही सीखा है, उसमें दृढ़ता शून्यता रहती है। जिसने दोनों को सीखा है और दोनों का समुचित स्थान पर सम्यक् प्रयोग करता है, वह वस्तुस्थिति से अभिज्ञ बन सकता है। यह अनेकान्त का प्रयोग है।
नियति और पुरुषार्थ, ये दोनों वाद हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। अनेकांत के आलोक में इन्हें समझा जा सकता है। जैन दर्शन आत्मकर्तृत्व में विश्वास करता है। व्यक्ति के सुख-दुःख में कर्मवाद अथवा आत्मकर्तृत्व का सिद्धान्त लागू होता है। किन्तु कुछ स्थितियों में पुरुषार्थ व आत्मकृतित्व निष्प्रभावी रहता है।
जीव के भव्य और अभव्य होने में किसी कर्म का उदय अथवा विलय कारणभूत नहीं है। यह अनादिपारिणामिक भाव है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कोई भी पुरुषार्थ अभव्य को भव्य नहीं बना सकता। एक पदार्थ जीव है और एक पदार्थ अजीव है। जीव के जीव होने में और अजीव के अजीव होने में किसी कर्म का योगदान नहीं है, यह भी अनादिपारिणामिक भाव है, स्वाभाविक स्थिति है। यह कुछ भी कृत नहीं है, अकृत है। भव्य को अभव्य और अभव्य को भव्य, जीव को अजीव तथा अजीव को जीव बनाना पुरुषार्थ के वश की बात नहीं है। यहां पुरुषार्थ सार्थक नहीं हो सकता। यह पुरुषार्थ की सीमा से बाहर का क्षेत्र है, अपितु यह पुरुषार्थ-निरपेक्ष विशुद्ध नियति का क्षेत्र है। कोई भव्य है, यह उसकी नियति है। कोई अभव्य है, यह उसकी नियति है। यह पुरुषार्थ-अप्रभावी नियति है।

