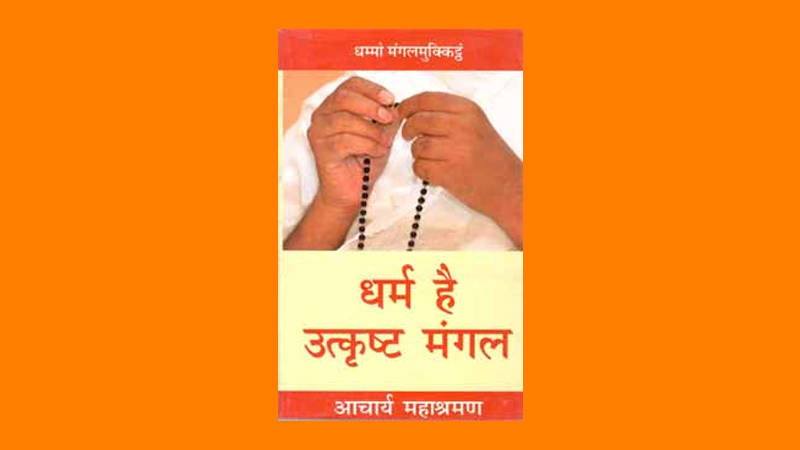
स्वाध्याय
धर्म है उत्कृष्ट मंगल
जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं, जस्स वऽत्थि पलायणं।
जो जाणे न मरिस्सामि सो हु कंरवे सुए सिया।।
एक वह जिसकी मौत के साथ दोस्ती हो गई है। दूसरा वह जो दौड़ने में कुशल हो, मौत आएगी तो मैं दौड़कर भाग जाऊंगा। वह मुझे पकड़ भी नहीं पाएगी, इस प्रकार सोचने वाला। तीसरा वह व्यक्ति जो जानता हो मैं कभी मरूंगा ही नहीं। ये तीन प्रकार के व्यक्ति बाद में धर्म करने की बात सोच सकते हैं। किन्तु ऐसा कभी हुआ नहीं, होगा भी नहीं कि मौत के साथ दोस्ती कर ले या मौत उसे माफ कर दे। यह Universal law (सार्वभौम नियम) है। इसका उल्लंघन कभी नहीं हो सकता। जो जन्मा है, उसकी मृत्यु निश्चित है। इन दुःखों के कारण ही मनुष्य में धर्म की प्रेरणा जागती है। मौत से बचने के लिए आदमी चाहे कुछ भी यत्न कर ले, पर मौत कभी भी उसे नहीं छोड़ती। जन्म लिया है तो उसे एक दिन मरना ही पड़ेगा। व्यक्ति चाहे पहाड़ पर चढ़ जाए, समुद्र को लांघ ले, सभी उपाय कर ले, फिर भी मौत उसका पीछा नहीं छोड़ेगी।
यह जानकर व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। जब आदमी को भयंकर बीमारियां घेर लेती हैं तब कौन उसे त्राण देता है? सेवा करने वाले सेवा कर सकते हैं पर पीड़ा को कौन कम करे, दूर करे? गृहस्थावस्था में अनाथी मुनि को जब आंख की वेदना हुई, बहुत से वैद्य बुलवाए गए। परिजन सब पास में बैठे थे पर वेदना दूर नहीं हो सकी? जब यह संसार की स्थिति देखी तब मन में संकल्प जागा अगर मेरी पीड़ा दूर हो जाए तो मैं मुनि बन जाऊंगा, दीक्षा ले लूंगा। यह संकल्प किया तो वेदना शांत होने लगी और वेदना शान्त होने के बाद वे साधु बन गए, साधना में लग गए।
भगवान बुद्ध के जीवन का उदाहरण है-
बुद्ध ने बीमार को देखा, बूढ़े को देखा, मुर्दे को देखा और साधु को देखा तो वैराग्य जाग गया और उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, साधना करने लगे। जब व्यक्ति के सामने संसार की वास्तविक स्थिति आती है तो वैराग्य जाग जाता है। किन्तु वैराग्य भी कई प्रकार का होता है। अपेक्षा इस बात की है जो वैराग्य जागे वह स्थायी बन जाए। आदमी को अपना जीवन निष्पाप, निष्कलंक और सादगीपूर्ण बिताना चाहिए। मैं पाप करूंगा तो पाप का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा और एक दिन संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर यह बात दिमाग में बैठ जाए तो व्यक्ति ज्यादा पाप कर नहीं सकता। इसलिए ऋषियों ने कहा-व्यक्ति जीवन की सच्चाई को समझे कि सबको मरना है, कर्म के फल भोगने हैं, इसलिए हम धर्मध्यान में लगें। धर्म दो प्रकार का होता है एक है काल-प्रतिबद्ध धर्म। दूसरा है कालातीत धर्म।
सामायिक करना, पौषध करना, व्याख्यान सुनना, उपवास करना ये सारे कालप्रतिबद्ध धर्म के अन्तर्गत आते हैं। क्षमा का अभ्यास करना, सरलता रखना, समता रखना, किसी के बारे में बुरा न सोचना, धोखा न देना ये सारे कालातीत धर्म के अन्तर्गत आते हैं। कालातीत धर्म का अर्थ है हर समय किया जाने वाला धर्म।
धर्म के सहारे ही व्यक्ति अपने जीवन को शान्ति और सुख से बिता सकता है। जो व्यक्ति अपने पवित्र जीवन की पवित्रता के प्रति जागरूक रहता है, वह पाप से बच सकता है, दुःख से बच सकता है। आगमों में कहा है-
कामाणुगिद्विप्पभवं खु दुक्खं, सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स।
जं काइयं माणसियं च किचि, तस्सन्तगं गच्छइ वीयरागो।।
चाहे मनुष्य हो या देवता हो, उनके जो भी शारीरिक या मानसिक दुःख होते हैं उसका मूल कारण है-राग। काम और भोग दो शब्द हैं। श्रोत्रेन्द्रिय और चक्षुइन्द्रिय के विषय काम कहलाते हैं। घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय इनके विषय भोग कहलाते हैं। अर्थात् जिनका शरीर के साथ जिनका सीधा संपर्क होता है उन्हें भोग कहते हैं। जिनका प्रकट रूप से सीधा संपक नहीं होता उन्हें काम कहते हैं। काम और भोग दोनों ही दुःख का कारण बनते हैं। आदमी की लालसा, इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। जिस वस्तु के साथ राग का संस्कार जुड़ जाता है, उसे छोड़ना कठिन हो जाता है। वैसे तो सभी प्राणी सुख को चाहने वाले होते हैं, दुःख कोई भी नहीं चाहता। जब तक आदमी सच्चे सुख का रास्ता नहीं खोजेगा तब तक उसे सच्चा सुख नहीं मिल सकता।

