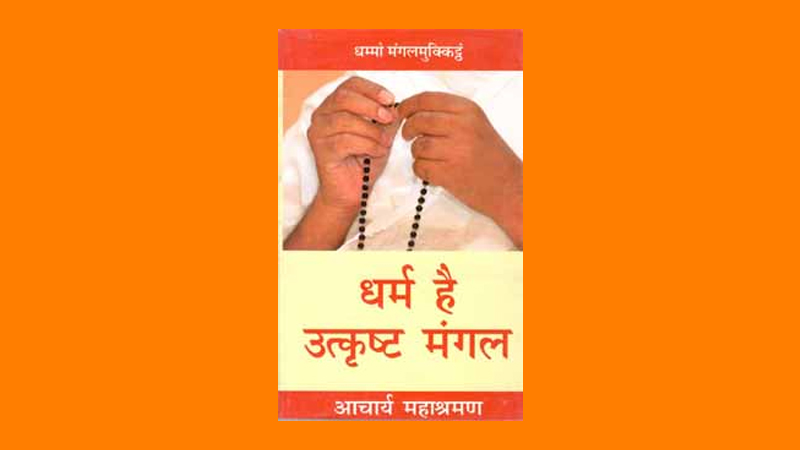
स्वाध्याय
धर्म है उत्कृष्ट मंगल
रास्ते दो प्रकार के हैं-एक है इच्छा का रास्ता, दूसरा है संतोष का रास्ता, संयम का रास्ता। इच्छाओं के असीमित होने से अन्त में जाकर आदमी दुःखी होता है। इसलिए महर्षियों ने कहा- सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संतोष धारण करना चाहिए। ज्यों-ज्यों आदमी की उम्र बढ़ती है फिर भी उसकी लालसा बूढ़ी नहीं होती। संस्कृत साहित्य में कहा है-
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः, तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः।
कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः।।
भोग क्या भोगे हैं हम स्वयं भोग लिये गए हैं। तपस्या नहीं की किन्तु आदमी लालसा में स्वयं तप गया। समय क्या बीता आदमी स्वयं बीत गया। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई किन्तु मनुष्य का शरीर जीर्ण हो गया। यह स्थिति है संसार की। बूढ़े आदमी का शरीर गल जाता है, जीर्ण-शीर्ण हो जाता है। मुंह दंतविहीन हो जाता है। लाठी के सहारे चलता है। इतना सब होने पर भी आशा कमजोर नहीं होती। इस स्थिति में कामनाओं को छोड़ना तो बहुत कठिन कार्य है। कहा भी है-कामे कमाहि कमियं खु दुक्खं।
अगर दुःख को दूर करना चाहते हो तो कामनाओं को दूर करो, इच्छाओं को दूर करो। अगर इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो आदमी अपने आप सुखी बन जाएगा। इच्छाएं और कामनाएं ज्यों-ज्यों बढ़ती जाएंगी दुःख भी बढ़ता जाएगा। कामना और इच्छाओं पर विजय पाना ही दुःख पर विजय पाना है। इच्छा आकाश के समान अनन्त होती है। उसकी सीमा नहीं होती। धन से आदमी सुखी नहीं हो सकता। धन जीवनयापन के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकता है किन्तु जब तक व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को सीमित नहीं करता, लालसा को कम नहीं करता, वह वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। जो वस्तु वर्षों से साथ रह जाती है, उसके प्रति इतना राग होता जाता है कि उसके छूटते ही व्यक्ति दुःख की अनुभूति करने लगता है।
यह संसार तो एक धर्मशाला है। यहां लोग आते हैं। कुछ दिन रहकर चले जाते हैं। जब तक मकान के प्रति, पदार्थ के प्रति, काम-भोग के प्रति-राग है, तब तक आत्मशांति या सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्योंही अपनेपन का भाव आता है, दुःख हो जाता है। अपनेपन की भ्रान्ति मिटती है तो दुःख मिट जाता है-
'एक सेठ-संतों के पास बैठा था। इतने में ही उसका बड़ा लड़का आया और बोला-पिताजी! अपने मकान में तो आग लग गई है। आप चलो, उसे संभालो। बस यह सुनते ही सेठ तो रोने लग गया। इतनें में ही उसका दूसरा लड़का आया, बोला-पिताजी! आप रोओ मत, जिस मकान में आग लगी है वह मकान तो हम बेच चुके हैं। इतना सुनते ही सेठ ने रोना बंद कर दिया। और वह सहजभाव में आ गया। इतने में ही तीसरा लड़का आया, उसने कहा पिताजी! जिस मकान में आग लगी है वह मकान अपना ही है। उसे बेचने की बात चली थी किन्तु अभी तक बेचा नहीं है। सेठ ने फिर रोना शुरू कर दिया। जब तक अपनेपन का भाव था तब तक सेठ को दुःख था। अपनेपन का भाव मिटा तो दुःख भी मिट गया। ऐसा क्यों हुआ? यह सब राग के कारण हुआ। जो व्यक्ति समता और वीतरागता की साधना करता है वही पूर्ण सुखी हो सकता है।
भयंकर बीमारियों का भी एक कारण है राग। इसलिए जीवन को शांत और सुखी बनाने के लिए राग को कम करना होगा तथा वीतरागता का अभ्यास करना होगा। सामान्य आदमी पूर्णतया वीतरागी नहीं हो सकता, फिर भी समता और वीतरागता की सामान्य साधना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। धन के प्रति भी ज्यादा आसक्ति या ज्यादा राग-भाव अगर है तो वह भी दुःखदायी ही है। जहां भी ज्यादा आसक्ति है वहां सुख नहीं हो सकता। राग-भाव साधना में बहुत बड़ी बाधा है। आवश्यकता है हम राग को कम करें, सुखी जीवन जीने का प्रयन करें।

