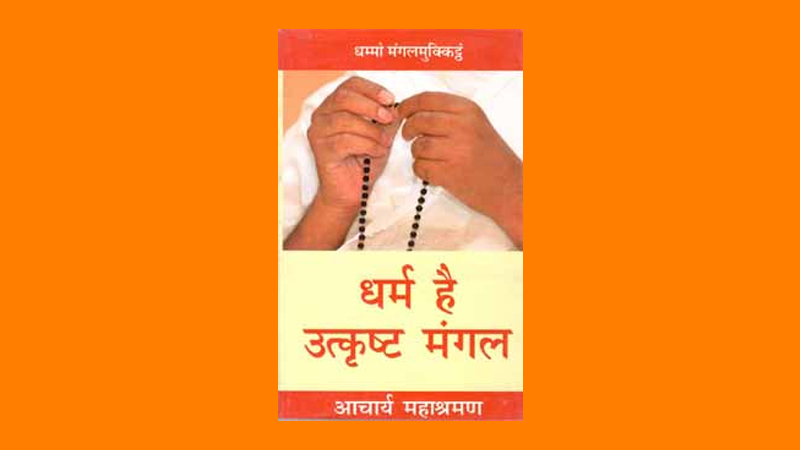
स्वाध्याय
धर्म है उत्कृष्ट मंगल
सातवें अध्याय में सात-सात को संख्यावाली स्थितियों का वर्णन है, जैसे-योनिसंग्रह के सात प्रकार, सात संस्थान, सात भयस्थान आदि। इसमें गण से अपक्रमण करने के कारण, छद्मस्थ व केवली की पहचान, मूल गोत्र, सात स्वर (षड्ज, ऋषभ आदि), सात कुलकर आदि का वर्णन है।
आठवें अध्याय में आठ-आठ की संख्यावाली स्थितियों का उल्लेख है, जैसे – आठ कर्म, आठ स्पर्श, आठ गणिसम्पदा आदि। इसमें समितियों, आलोचना देने की अहता, प्रायश्चित्त, वचन विभक्तियां, कृष्णराजि, केवली समुद्घात आदि का वर्णन है।
नवें अध्याय में नौ-नौ की संख्यावाली स्थितियों का उल्लेख है, जैसे-नौ ब्रह्मचर्य-गुप्तियां, नौ सद्भाव पदार्थ, नौ महानिधियां आदि। इसमें विकृतियां, पुण्यबन्ध, पुद्गल आदि का वर्णन है।
दसवें अध्याय में दस-दस की संख्यावाली स्थितियों का उल्लेख है, जैसे-दस प्रकार की लोकस्थिति, दस प्रकार का वैयावृत्त्य, दस प्रकार का प्रायश्चित्त आदि। इसमें शस्त्र, दोष, रुचि, संज्ञा आदि का वर्णन है।
ठाणं प्राकृत भाषा की एक निधि है। इसका ग्रंथ परिमाण ५१७० अनुष्ठप् श्लोक बताया गया है।
महावीर की अहिंसा
'सूयगडो' सूत्र में एक जगह आया है 'लोगुत्तमे समणे नायपुत्ते' अर्थात् श्रमण भगवान महावीर
लोक (दुनिया) में उत्तम हैं। लोकोत्तम कौन हो सकता है? लोकोत्तम वही व्यक्ति हो सकता है, जो अहिंसा का पुजारी होता है। श्रमण महावीर परम अहिंसक थे, इसीलिए सूत्रकार ने उन्हें लोकोत्तम विशेषण से
विशिष्ट किया है।
इस अवसर्पिणी काल में चौबीस तीर्थकर हुए हैं। माना जाता है कि उन तीर्थकरों के शरीर के दक्षिणांग में एक चिह था, जिसे ध्वज भी कहा जाता है। महावीर का ध्वज-सिंह है। यह कैसी विसंगति है। एक तरफ अहिंसा अवतार महावीर और दूसरी तरफ सिंह जो हिंसा का प्रतीक है। यह असमानता कैसे? क्या इसमें भी कोई राज है? हम दूसरे प्रकार से सोचेंगे तो पता चलेगा कि यह बेमेल नहीं, बल्कि बहुत उचित मेल है। सिंह-पौरुष और शौर्य का प्रतीक है। भगवान महावीर की अहिंसा शूरवीरों की अहिंसा है, कायरों की नहीं। पलायनवादी और भीरु व्यक्ति कभी अहिंसक नहीं हो सकता। अहिंसा की आराधना के लिए आवश्यक है- अभय का अभ्यास। सिंह जंगल का राजा होता है, वन्य प्राणियों पर प्रशासन व नियन्त्रण करता है, इसी तरह महावीर की अहिंसा है अपनी इन्द्रियों और मन पर नियंत्रण करना।
महावीर अगर अभय और पराक्रमी नहीं होते तो वे संगमदेव द्वारा उपस्थापित मारणान्तिक उपसर्गों को सहन नहीं कर सकते। वे चण्डकौशिक के डंक की पीड़ा को आनन्द में नहीं परिणमा पाते। जन-साधारण के समक्ष अगर कोई ऐसा उपसर्ग उपस्थित हो जाता है, तो घबड़ा कर भाग जाता है या कोई शक्तिशाली होता है तो उसे मिटाने की कोशिश करता है। महावीर पलायन और प्रतिशोध दोनों से ऊपर उठे हुए थे। महावीर चण्डकौशिक को देखकर घबड़ाये नहीं। सांप ने डंसा तो भी उनके मन में प्रतिशोध के भाव नहीं जागे। वे जानबूझ कर सलक्ष्य सर्प की बांबी के पास गये थे। उन्हें अपनी सुरक्षा का भय नहीं था। महावीर की अहिंसा थी सर्वत्र मैत्री। उनकी मैत्री संकुचित दायरे में आबद्ध नहीं थी। उनके मन में चण्डकौशिक सर्प के प्रति भी उतने ही मैत्री के भाव थे, जितने कि अन्य प्राणियों के प्रति।
श्रमण महावीर अपने नश्वर शरीर की सार-संभाल छोड़ चुके थे। परम अहिंसक वह होता है जो अपने शरीर की मूर्च्छा त्याग देता है, जिसे मृत्यु का भय व्यथित नहीं करता। भगवान महावीर ने इस संकल्प के साथ अभिनिष्क्रमण किया कि मैं अपने पूरे साधनाकाल में शरीर को सार-संभाल न करता हुआ, शरीर पर मूर्च्छा न करता हुआ विचरण करूंगा।
भगवान महावीर अहिंसा की अत्यन्त सूक्ष्मता में गये हैं। आज तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि वनस्पति सजीव है, पर महावीर ने आज से अढ़ाई हजार वर्ष पूर्व ही कह दिया था कि वनस्पति भी सचेतन है वह भी मनुष्य की भांति सुख-दुःख का अनुभव करती है। वनस्पति इतनी सुकोमल होती है कि उसका स्पर्श करने मात्र से उसे पीड़ा होती है। महावीर ने कहा- पूर्ण अहिंसा व्रतधारी व्यक्ति सजीव वनस्पति का स्पर्श भी नहीं कर सकता।

