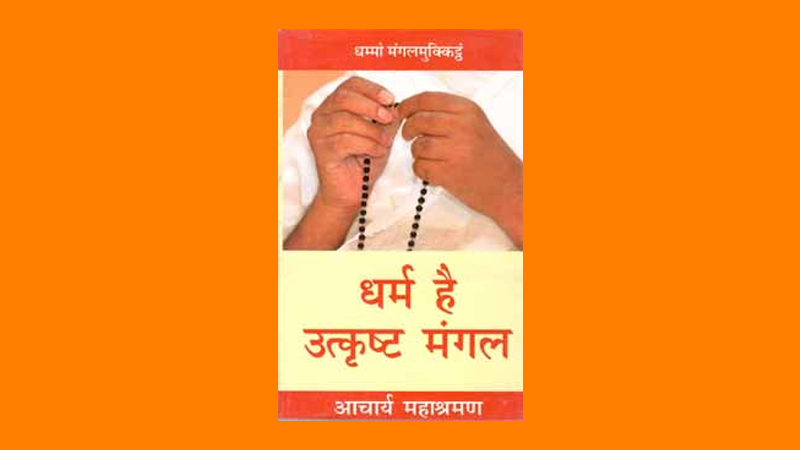
स्वाध्याय
धर्म है उत्कृष्ट मंगल
जहां संघ है वहां अनेक व्यक्ति हैं। जहां अनेक व्यक्ति हैं, वहां अनेक मस्तिष्क हैं। जहां अनेक मस्तिष्क हैं वहां विभिन्न मतियां होती हैं- 'मुण्डे-मुण्डे मतिर्भिन्ना'। एक मस्तिष्क में भी अनेक मति/विचार होते हैं तो अनेक मस्तिष्कों में तो वे और भी ज्यादा संभावित हो जाते हैं। विचार-भेद छद्मस्थ (अपरिपूर्ण-ज्ञानवाले) व्यक्तियों में ही हो सकता है। सर्वज्ञों में परस्पर कोई मतभेद नहीं होता और सर्वथा चिंतनशून्य व्यक्तियों में भी विचार भेद की स्थिति नहीं बनती है। यह भेद सर्वज्ञ और अज्ञ इन दोनों के मध्य की स्थिति वालों में ही पाया जाता है।
समुदायों में अनेक बार संघर्ष पैदा होते हैं और अनेक बार उन संघर्षों का कारण सिद्धान्त-भेद/विचार-भेद बताया जाता है। वह कभी-कभी हो भी सकता है। परंतु संभवतः बहुधा संघर्ष का मूल कारण विचार-भेद नहीं होता, अपितु स्वयं का तुच्छ स्वार्थ, अहंकार पर चोट व आकांक्षा की आपूर्ति होती है और उसे ही विचार-भेद का जामा पहना दिया जाता है। पूज्य गुरुदेवश्नी के आचार्य-काल में तेरापंथ धर्मसंघ में जो बड़े-बड़े आंतरिक संघर्ष पैदा हुए। उनमें भी मतभेद की अपेक्षा मनभेद ज्यादा सशक्त रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है।
किसी सिद्धान्त को लेकर शुद्ध मतभेद हो जाए तो वह बुरा नहीं होता, परंतु मन-भेद बुरा होता है। शुद्ध मतभेद समझ के कोण की भिन्नता से होता है। वह कोण परस्पर स्पष्ट हो जाए तो मतभेद समाप्त भी हो सकता है। सत्य और अनेकान्त के प्रति समर्पित तथा पूर्वाग्रह-मुक्त व्यक्तियों में और समग्रता से तत्त्व को समझने वाले व्यक्तियों में भी विचार-साम्य देखने को मिलता है। फिर चाहे वे भिन्न-भिन्न देश, भिन्न-भिन्न वेश और परिवेश में भी जीने वाले भी क्यों न हों? यदि दोनों ओर सामञ्जस्य की भावना हो और सत्यपरक दृष्टिकोण हो तो दुनिया में विचार-भेद को प्रायः-प्रायः समाप्त किया जा सकता है। फिर भी मति श्रुत ज्ञान के क्षयोपशम की तरतमता के कारण भी कोई मतभेद उत्पन्न हो सकता है।
तेरापंथ धर्मसंघ की विधान-धाराओं में एक है- 'श्रद्धा या आचार के बोल को लेकर गण में भेद न डाले। दलबंदी न करे। आचार्य व बहुश्रुत साधु जो कहे वह मान ले अथवा केवली गम्य कर दे।' संघ से किसी साधु-साध्वी के मन में श्रद्धा/ मान्यता के बारे में अथवा आचार (अमुक कार्य कल्पनीय है या नहीं) के विषय में कोई मतभेद पैदा हो सकता है। तेरापंथ की विधान-धाराओं में एक यह भी है—'जिसका मन साक्षी दे, भली-भांति साधुपन पलता जाने, गण में तथा अपने आप में साधुपन माने तो गण में रहे, किन्तु वंचनापूर्वक गण में न रहे।'
केवलीगम्य करने की धारा और संघ छोड़ देने की धारा दोनों परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं। यहां
विमर्श की अपेक्षा है। जहां मतभेद इस कोटि का हो कि किसी को यह लगे कि संघ में शुद्ध साधुपन है ही नहीं, वहां तो वंचनापूर्वक संघ में रहना ही गलत है। इसलिए संघ-त्याग की बात लागू होती है। स्वयं
आचार्य भिक्षु स्थानकवासी जैन परंपरा में दीक्षित मुनि थे। परंतु उनको ऐसा लगा कि संघ में शुद्ध साधुपन है ही नहीं, वैसी स्थिति में उनको संघ-त्याग का मार्ग ही स्वीकार करना पड़ा। जहां ऐसा मतभेद नहीं होता कि साधुत्व ही अनस्तित्व को प्राप्त हो, वहां 'केवलीगम्य करने' की बात प्रभावी होती है। मतभेद होने पर बहुश्रुत व्यक्तियों के साथ चर्चा की जाए, उनसे समझने का प्रयास किया जाए। उनसे संतोषजनक
समाधान न मिले तो आचार्य से चर्चा की जाए। फिर भी प्रश्न समाहित न हो तो व्यक्ति यह सोचे कि निश्चय में तो केवली जानते हैं, वही सत्य है। व्यवहार' में संघ में आचार्य जो स्थापना करते हैं, वह मुझे स्वीकार है। यह एक स्वस्थ तरीका है। परन्तु व्यक्ति किसी बोल को लेकर संघ में भेद डालने की चेष्टा करे तो वह संघ-द्रोही बन जाता है।
आचार्य भिक्षु की दृष्टि में आचार एवं विचार की विशुद्धि मुख्य थी। उस विशुद्धि के लिए अनुशासित संगठन आधार था। उस संगठन की सुटूढ़ता व चिरस्थायित्व के लिए उचित समझोता-वृत्ति भी आवश्यक है। साधक का जीवन निश्छलता से परिपूर्ण हो और सत्यपूर्ण हो, चिन्तन में अनाग्रह हो।
संघ में आचार-विचार सम्बन्धी नाना प्रश्न उठ सकते हैं। उस स्थिति में क्या किया जाए? इस समस्या के संदर्भ में आचार्य भिक्षु ने कहा-'बहुश्रुत साधुओं व आचार्य से समझने की चेष्टा की जाए! कोई बात समझ में न आए तो क्या करना चाहिए? क्या कुछ साधु-साध्वियों को अपनी तरफ आकर्षित करके संघ-त्याग और संघ-विद्रोह कर देना चाहिए?

