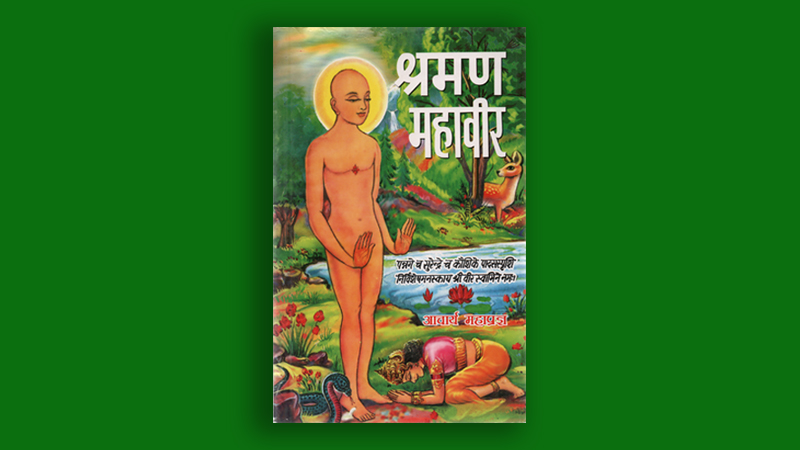
स्वाध्याय
श्रमण महावीर
५. भगवान् के संघ में अभिवादन की एक निश्चित व्यवस्था थी। उसके अनुसार दीक्षा-पर्याय में छोटे मुनि को दीक्षा-ज्येष्ठ मुनि का अभिवादन करना होता था। एक मुनि के सामने यह व्यवस्था समस्या बन गई। वह राज्य को छोड़कर मुनि बना था। उसका नौकर पहले ही मुनि बन चुका था। राजर्षि की आखों पर मद का आवरण आ गया। उसने उस नौकर मुनि का अभिवादन नहीं किया। यह बात भगवान् तक पहुंची। भगवान् ने मुनिपरिषद् को आमंत्रित कर कहा, 'सामाजिक व्यवस्था में कोई सार्वभौम सम्राट् होता है, कोई नौकर और कोई नौकर का भी नौकर । किन्तु मेरे धर्म-संघ में दीक्षित होने पर न कोई सम्राट् रहता है और न कोई नौकर। वे बाहरी उपाधिओं से मुक्त होकर उस लोक में पहुंच जाते हैं, जहां सब सम हैं, कोई विषम नहीं है। फिर अपने दीक्षा-ज्येष्ठ का अभिवादन करने में किसी को लज्जा का अनुभव नहीं होना चाहिए। सम्राट् और नौकर होने की विस्मृति होने पर ही आत्मा में समता प्रतिष्ठित हो सकती है।
राजर्षि का अहं विलीन हो गया। उनका नौकर अब उनका साधर्मिक भाई बन गया।
भगवान् ने अपने संघ को एक समता-सूत्र दिया। वह हजारों-हजारों कंठों से मुखरित होता रहा। उसने असंख्य लोगों के 'अहं' का परिशोधन किया। वह सूत्र है, 'यह जीव अनेक बार उच्च या नीच गोत्र का अनुभव कर चुका है। अतः न कोई किसी से हीन है और न कोई अतिरिक्त । यह जीव अनेक बार उच्च या नीच गोत्र का अनुभव कर चुका है- यह जान लेने पर कौन गोत्रवादी होगा और कौन मानवादी ।”
भगवान् ने अपने संघ में समता का बीज बोया, उसे सींचा, अंकुरित किया, पल्लवित, पुष्पित और फलित किया।
भगवान् ने समता के प्रति प्रगाढ़ आस्था उत्पन्न की। अतः उसकी ध्वनि सब दिशाओं में प्रतिध्वनित होने लगी।
जयघोष मुनि घूमते-घूमते वाराणसी में पहुंचे। उन्हें पता चला कि विजयघोष यज्ञ कर रहा है। वे विजयघोष की यज्ञशाला में गए। यज्ञ और जातिवाद का अहिंसक ढंग से प्रतिवाद करना महावीर के शिष्यों का कार्यक्रम बन गया था। इस कार्यक्रम में ब्राह्मण मुनि काफी रस ले रहे थे। जयघोष जाति से ब्राह्मण थे। विजयघोष भी ब्राह्मण था। एक यज्ञ का प्रतिकर्ता और दूसरा उसका कर्ता। एक जातिवाद का विघटक और दूसरा उसका समर्थक ।
श्रमण और वैदिक-ये दो जातियां नहीं हैं। ये दोनों एक ही जाति-वृक्ष की दो विशाल शाखाएं हैं। उनका भेद जातीय नहीं किन्तु सैद्धान्तिक है। श्रमण-धारा का नेतृत्व क्षत्रिय कर रहे थे और वैदिक धारा का नेतृत्व ब्राह्मण। फिर भी बहुत सारे ब्राह्मण श्रमण-धारा में चल रहे थे और बहुत सारे क्षत्रिय ब्राह्मण-धारा में। उस समय धर्म-परिवर्तन व्यक्तिगत प्रश्न था। उसका व्यापक प्रभाव नहीं होता था। यदि धर्म-परिवर्तन का अर्थ जाति-परिवर्तन होता तो समस्या बहुत गम्भीर बन जाती। किन्तु एक ही भारतीय जाति के लोग अनेक धर्मों का अनुगमन कर रहे थे, इसलिए उनके धर्म-परिवर्तन का प्रभाव केवल वैचारिक स्तर पर होता। जातीय स्तर पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता।
विजयघोष के मन में वैचारिक भेद उभर आया। उसने दर्प के साथ कहा-मुने ! इस यज्ञ-मंडप में तुम भिक्षा नहीं पा सकते। कहीं अन्यत्र चले जाओ। यह भोजन वेदविद् और धर्म के पारगामी ब्राह्मणों के लिए बना है।'
मुनि बोले, 'विजयघोष! मुझे भिक्षा मिले या न मिले, इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं। मुझे इसकी चिन्ता है कि तुम ब्राह्मण का अर्थ नहीं जानते।'
विजयघोष, “इसका अर्थ जानने में कौन-सी कठिनाई है? जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है, वह ब्राह्मण है।'
मुनि, “मैं तुम्हारे सिद्धान्त का प्रतिवाद करता हूं। जाति जन्मना नहीं होती, वह कर्मणा होती है।

