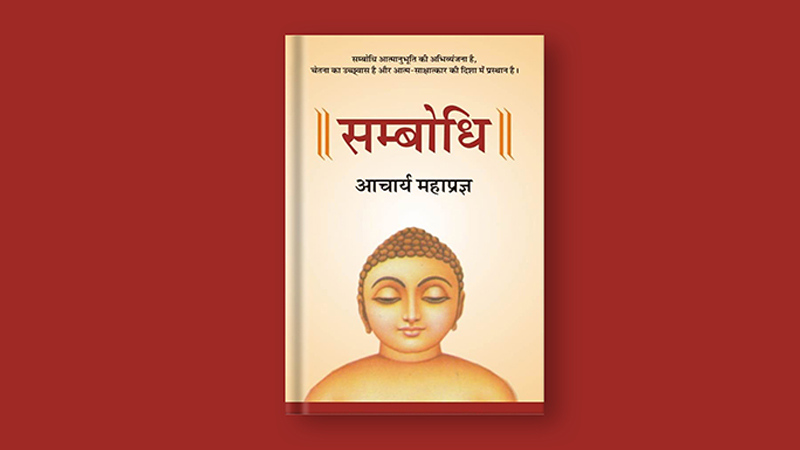
स्वाध्याय
संबोधि
ु आचार्य महाप्रज्ञ ु
आज्ञावाद
भगवान् प्राह
(43) आसक्तिं जनयत्याशु, वस्तुभोगो हि देहिनाम्।
जीवनं वस्तुसापेक्षं, समस्या महती ध्रुवम्॥
पदार्थ का भोग आसक्ति उत्पन्न करता है और जीवन पदार्थ-सापेक्ष है, यह महान् समस्या है।
(44) आसक्तिर्यावती पुंसां, तावान् भावात्मको ज्वर:।
भावात्मको ज्वरो यावान्, तावान् तापो हि मानस:॥
जितनी आसक्ति उतना भावनात्मक तनाव। जितना भावात्मक तनाव, उतना मानसिक तनाव या मानसिक दु:ख।
(45) चैतन्यानुभवो यावान्, अनासक्तिश्च तावती।
यावती स्यादनासक्ति:, तावान् भाव: प्रसादयुक्॥
जितनी चेतना की अनुभूति उतनी अनासक्ति, जितनी अनासक्ति उतनी भावात्मक प्रसन्नता।
(46) यावान् भावप्रसाद: स्याद्, तावद् मनो हि निर्मलम्।
नैर्मल्यं मनसो यावद्, तावत् स्याद् सहजं सुखम्॥
जितनी भावनात्मक प्रसन्नता है, उतनी मानसिक निर्मलता है। जितनी मानसिक निर्मलता है, उतना सहज सुख है।
धर्म का तत्त्व सहज, सुगम होते हुए भी जटिल बना हुआ है। इसका कारण हैउसे बुद्धि के द्वारा व्याख्यात किया जाता है, मन और बुद्धि के द्वारा ही सुना जाता है और ग्रहण किया जाता है। यह है अनुभूति द्वारा गम्य या प्रज्ञा के द्वारा ज्ञेय है। बुद्धि स्वयं अस्थिर हैवह विकल्पों को पैदा करती है। धर्म है निर्विकल्प। धर्म को जानने के लिए सब बुद्धि के द्वारा प्रयत्न करते हैं। इसलिए उसका सही समाधान नहीं होता।
मेघ की जिज्ञासा भी इसी की द्योतक है। धर्म क्या है? धर्म की अनिवार्यता क्यों और धर्म का लाभ क्या है?
धर्म क्या है? इसका उत्तर अलग-अलग रूपों में मिलता है। लौकिक धर्म की व्याख्या भिन्न है और अलौकिक-आध्यात्मिक धर्म की परिभाषा अलग है। फिर भी दोनों का सम्मिश्रण हो जाता है। सम्मिश्रण के कारण संशय उत्पन्न होता है। यदि दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट हो तो यह भ्राँति नहीं रहती किंतु यह भी कम संभव है। सामान्य लोगों के लिए यह अंतर सहजगम्य होना भी मुश्किल है। भगवान् महावीर ने धर्म की संक्षेप परिभाषा देते हुए कहाचैतन्य का अनुभव धर्म है। जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व का अनुभव कर सके, वह धर्म है। अपना अनुभव, अपना बोध, अपना ज्ञान धर्म है। धर्म का समग्र बल इस पर है कि व्यक्ति अपने को जाने ‘मैं कौन हूँ?’ इसका प्रथम चरण हैव्रत। व्रत का कार्य हैअपने भीतर आने वाले विजातीय तत्त्व के द्वार को रोकना। जैसे-जैसे विजातीय तत्त्व का द्वार बंद हो जाता हैवैसे-वैसे व्यक्ति अपने निकट पहुँचता चला जाता है। विजातीय तत्त्व का आवागमन इतनी तीव्रता से होता रहता है कि साधारण-असाधारण व्यक्तियों की समझ से परे ही रहता है। आदमी के संस्कार उसे भीतर आने से दूर ही रखता है। वह राग और द्वेष इन दो प्रवृत्तियों में ही उलझा रहता है। चैतन्य के अनुभव में ये दोनों परम बाधक हैं। व्रत-संयम और तप इन दोनों को नियंत्रित करते हैं। राग का अर्थ हैआसक्ति और द्वेष का अर्थ हैअप्रिय पदार्थों के प्रति घृणा, अरुचि। प्रिय विषयों में रुचि राग है। जीवन पदार्थों से मुक्त नहीं हो सकता है। वह पदार्थ सापेक्ष है। पदार्थों का भोग आसक्ति उत्पन्न करता है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने आसक्ति को और अधिक बद्धमूल करने में अपनी भूमिका निभाई है और निभा रही है। आकर्षक पदार्थों के निर्माण के पीछे व्यक्ति के भीतर छिपे राग-आसक्ति को उत्तेजित करना ही है। नए-नए रूपों में जिस प्रकार पदार्थों की संयोजना हो रही है उसी प्रकार व्यक्ति का मन भी दूषित व प्रलुब्ध हो रहा है। इससे न शांति और न सुख हाथ लगता है। पदार्थों की सामग्री व उनके प्रति आकर्षण से शांति और सुख का कहीं वास्ता नहीं है। पदार्थ-सापेक्ष शांति व सुख का स्थायित्व भी कितना होता है? और उस सुख से मिलने वाला सुख भी कितना होता है? इससे यह स्पष्ट समझा जा सकता है कि शाश्वत, स्थायी सुख का संबंध पदार्थों से नहीं है। नश्वर पदार्थ स्थायी सुख का हेतु भी कैसे बन सकता है? इस अनुभूति ने ही अनासक्ति को जन्म दिया। भगवान ने इस समस्या के समाधान में कहा कि तुम पदार्थों से निरपेक्ष नहीं हो सकते, किंतु आसक्ति से मुक्त हो सकते हो। पदार्थों के साथ जुड़ना-बंधना या न बंधना यह तुम्हारे हाथ में है। तुम इस कला में पारंगत हो जाओ कि पदार्थों का भोग करते हुए भी उनके साथ लगाव नहीं रखना। दु:ख पदार्थों के साथ लगाव का ही है। जितना गहरा लगाव या अटेचमेंट-जुड़ना है उतना ही अधिक तनाव, ताप तथा ऊष्मा है। (क्रमश:)

