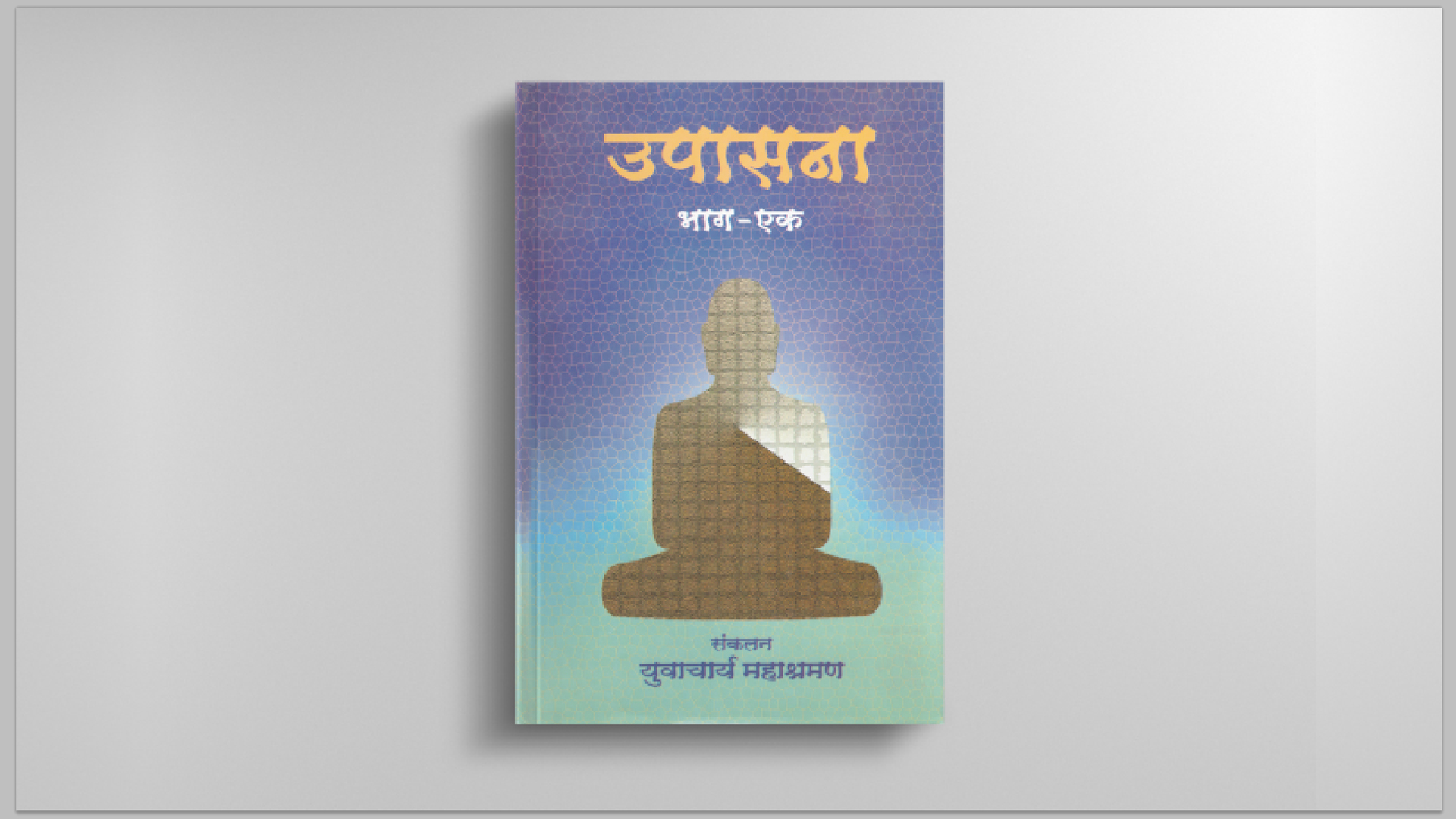
स्वाध्याय
उपासना
उपासना
(भाग - एक)
आचार्य तुलसी
श्वेतांबर से दिगंबर-शाखा निकली, यह भी नहीं कहा जा सकता। दिगंबर से श्वेतांबर-शाखा का उद्भव हुआ, यह भी नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक संप्रदाय अपने को मूल और दूसरे को अपनी शाखा बताता है। पर सच तो यह है कि साधना की दो शाखाएँ समन्वय और सहिष्णुता के विराट् प्रकांड का आश्रय लिए हुई थीं, वे उसका निर्वाह नहीं कर सकीं, काल-परिपाक से पृथक् हो गईं। अथवा यों कहा जा सकता है कि एक दिन साधना के दो बीजों ने समन्वय के महातरु को अंकुरित किया और एक दिन वही महातरु दो भागों में विभक्त हो गया। किंवदंती के अनुसार वीर-निर्वाण 609 वर्ष पश्चात् दिगंबर-संप्रदाय का जन्म हुआ, यह श्वेतांबर मानते हैं और दिगंबर-मान्यता के अनुसार वीर-निर्वाण 606 में श्वेतांबर-संप्रदाय का प्रारंभ हुआ।
सचेलत्व और अचेलत्व का आग्रह और समन्वयदृष्टि
जब तक जैन शासन पर प्रभावशाली व्यक्तित्व का अनुशासन रहा, तब तक सचेलत्व और अचेलत्व का विवाद उग्र नहीं बना। कुंदकुंद के समय यह विवाद तीव्र हो उठा था। बीच-बीच में इसके समन्वय के प्रयत्न भी होते रहे हैं। यापनीयसंघ श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं का समन्वित रूप था। इस संघ के मुनि अचेलत्व आदि की दृष्टि से दिगंबर-परंपरा का अनुसरण करते थे और मान्यता की दृष्टि से श्वेतांबर थे। वे स्त्री-मुक्ति को मानते थे और श्वेतांबर-सम्मत आगम-साहित्य का अध्ययन करते थे।
समन्वय की दृष्टि और भी समय-समय पर प्रस्फुटित होती रही है। कहा गया हैµ‘कोई मुनि दो वस्त्र रखता है, कोई तीन, कोई एक और कोई अचेल रहता है। वे परंपरा एक-दूसरे की अवज्ञा न करें; क्योंकि यह सब जिनाज्ञा-सम्मत है। यह आचार-भेद शारीरिक शक्ति और धृति के उत्कर्ष और अपकर्ष के आधार पर होता है। इसलिए सचेल मुनि अचेल मुनियों की अवज्ञा न करें और अचेल मुनि सचेल मुनियों को अपने से हीन न मानें। जो मुनि महाव्रत धर्म का पालन करते हैं और उद्यत-विहारी हैं, वे सब जिनाज्ञा में हैं।’
चैत्यवास परंपरा
वीर-निर्वाण की नवीं शताब्दी (850) में चैत्यवास की स्थापना हुई। कुछ शिथिलाचारी मुनि उग्र-विहार छोड़कर मंदिरों के परिपाश्र्व में रहने लगे। वीर-निर्वाण की दसवीं शताब्दी तक इनका प्रभुत्व नहीं बढ़ा। देवर्द्धिगणी के दिवंगत होते ही इनका संप्रदाय शक्तिशाली हो गया। विद्याबल और राज्यबल, दोनों के द्वारा इन्होंने उग्र-विहारी श्रमणों (संविग्नपाक्षिकों) पर पर्याप्त प्रहार किया। हरिभद्रसूरि ने ‘संबोध-प्रकरण’ में इनके आचार-विचार का सजीव वर्णन किया है।
अभयदेवसूरि देवर्द्धिगणी के पश्चात् जैन शासन की वास्तविक परंपरा का लोप मानते हैं।
चैत्यवास से पूर्व गण, कुल और शाखाओं का प्राचुर्य होते हुए भी उनमें पारस्परिक विग्रह या अपने गण का अहंकार नहीं था। वे प्रायः अविरोधी थे। अनेक गण होना व्यवस्था-सम्मत था। गणों के नाम विभिन्न कारणों से परिवर्तित होते रहेत थे। भगवान् महावीर के उत्तराधिकारी सुधर्मा के नाम से गण को सौधर्म गण कहा गया। समन्तभद्रसूरि ने वनवास स्वीकार किया, इसलिए उसे वनवासी गण कहा गया है।
चैत्यवासी शाखा के उद्भव के साथ एक पक्ष संविग्न, विधिमार्ग या सुविहितमार्ग कहलाया और दूसरा पक्ष चैत्यवासी।
स्थानकवासी
इस संप्रदाय का उद्भव मूर्ति-पूजा के अस्वीकार पक्ष में हुआ। विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में लोंकाशाह में मूर्ति-पूजा का विरोध किया और आचार की कठोरता का पक्ष प्रबल किया। ये गृहस्थावस्था में ही थे। इनकी परंपरा में ऋषि लवजी, आचार्य धमसिंहजी और आचार्य धर्मदासजी प्रतिभाशाली आचार्य हुए। आचार्य धर्मदासजी के निन्यानबे शिष्य थे। उन्होंने अपने बाईस विद्वान् शिष्यों को आचार्य बनाया और विभिन्न प्रांतों में उन्हें धर्म-प्रचार करने के लिए भेजा। उसके बाद लोंकाशाह का संप्रदाय ‘बाईस टोला’ या बाईस-संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर स्थानकों की मुख्यता के कारण यही ‘स्थानकवासी’ संप्रदाय के नाम से पहचाना जाने लगा।
(क्रमशः)

