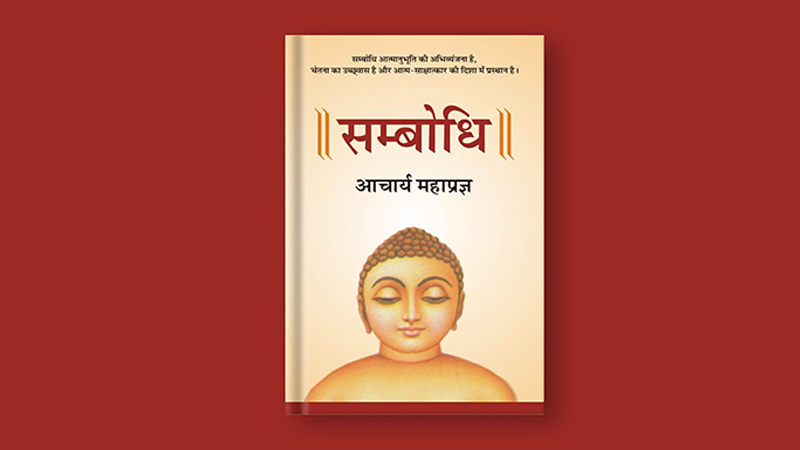
स्वाध्याय
संबोधि
बंध-मोक्षवाद
ज्ञेय-हेय-उपादेय
भगवान् प्राह
(पिछला शेष)
स्वाध्याय का तीसरा लाभ-
सत्य की दिशा में अनुगमन करना। ‘अनुप्रेक्षा’ उसका माध्यम है। शब्द और अर्थ की अनुप्रेक्षा करता हुआ व्यक्ति अंतिम गहराई में प्रवेश कर पदार्थ का सत्यबोध कर स्वयं में प्रविष्ट हो जाता है। उस स्वाध्याय के मौलिक स्वरूप का दर्शन करें, जो कि हमारे जीवन को आमूल-चूल बदलने में सक्षम है। वही यथार्थ तप है। स्वाध्याय का अर्थ है-स्व-आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा को पढ़ना। दूसरों को पढ़ना सरल है, स्वयं को पढ़ना नहीं। इसलिए इसे तप कहा है। दूसरे के अध्ययन में व्यक्ति जितना व्यग्र है उतना स्वयं के अध्ययन में उत्सुक नहीं है। दृष्टि का दूसरों पर अवलंबित होना धर्म नहीं, धर्म है स्वयं को देखना। स्वदर्शन जो सहज है, वह आज के मानव के लिए असहज हो गया। इसलिए आज स्वाध्याय तप की जितनी उपेक्षा है, पहले उतनी नहीं रही। बड़े-बड़े तपस्वियों के लिए यह तप दुर्धर्ष है। धर्म का जीवंत-रूप इसके बिना संभव नहीं है।
सही स्वाध्याय
स्वाध्याय का पहला चरण होगा कि हम अपने आमने-सामने खड़े होकर अपने को पढ़ें। दूसरों की धारणाओं को हटा दें। दूसरे लोग आपके संबंध में क्या कहते हैं-इस ओर पीठ कर दें। लोगों की अपनी-अपनी दृष्टि होती है, और अपने-अपने बटखरे होते हैं, और अपने-अपने माप होते हैं। आप उनकी चिंता करेंगे तो अपने असली चेहरे को कभी प्रगट नहीं कर सकेंगे। आपको अपना चेहरा उनके साँचे में ढालना होगा। इससे आपकी आत्मा मर जाएगी और आप संभवतया सर्वत्र सफल भी नहीं हो सकेंगे। इसलिए आप दूसरों से हटकर अपने में आएँ और देखें-बड़ी ईमानदारी से कि आप कैसे हैं? आपके भीतर क्या है? जो है-उससे डरें नहीं, देखते जाएँ।
दूसरे चरण में-आप अकेले बैठें और सहजतापूर्वक अपनी वृत्तियों का दर्शन करते जाएँ। एक-एक को प्रकट होने दें। जो हैं उन्हें अस्वीकार कैसे करेंगे? कैसे उनसे अपरिचित रहेंगे? यहाँ बहुत सावधानता, निर्भयता और धैर्य की अपेक्षा होगी। काम, क्रोध, घृणा, ईष्र्या, वासना आदि प्रवृत्तियाँ आपमें पहले भी विद्यमान थीं, किंतु उनका दर्शन नहीं था, अब आप उनको देख रहे हैं और उनको प्रकाश में ला रहे हैं। इसके साथ-साथ आज तक का जो आपका विकृत रूप था उसे आप स्वीकार भी करते जाइए, लेकिन एक बात का और ध्यान रखें कि आप ऐसे नहीं हैं। आपके भीतर एक विराट् शुद्धरूप और छिपा है। ये सब आपकी प्रमत्तता के कारण प्रविष्ट हो गए थे। आप ये नहीं हैं। जैसे-जैसे आप अपने को जानने लगेंगे तो आपमें बदलाहट होनी शुरू हो जाएगी। अपने को जानना और स्वीकार करना इस वृत्ति से छूटने का अमोघ उपाय है। महावीर की भाषा में यह सम्यग्-ज्ञान है। सम्यग् ज्ञान की स्थिति में अन्यथा होना अशक्य है। ज्ञान शक्ति है। स्वाध्याय की साधना का यही मुख्य लक्ष्य है।
(33) एकाग्रचिन्तनं योगनिरोधो ध्यानमुच्यते।
धम्र्यं चतुर्विधं तत्र, शुक्लं चापि चतुर्विधम्।।
एकाग्र चिंतन एवं मन, वचन और काया के निरोध को ध्यान कहते हैं। धम्र्यध्यान के चार प्रकार हैं और शुक्लध्यान के भी चार प्रकार हैं।
(34) अर्हता देशितां दृष्टिं, आलम्ब्य क्रियते यदा।
पदार्थचिन्तनं यत्तत्, आज्ञाविचय उच्यते।।
अर्हत् के द्वारा उपदिष्ट दृष्टि-अतीन्द्रिय विषयों को आलंबन बना कर जो पदार्थ का एकाग्र चिंतन किया जाता है, वह आज्ञा विचय है। यह धम्र्यध्यान का पहला प्रकार है।
(35) सर्वेषामपि दुःखानां, रागद्वेषौ निबंधनम्।
ईदृशं चिन्तनं यत्तत्, अपायविचयो भवेत्।।
राग और द्वेष सब दुःखों के कारण हैं-इस प्रकार का जो एकाग्र चिंतन किया जाता है, वह अपायविचय है। यह धम्र्यध्यान का दूसरा प्रकार है।
(36) सुखान्यपि च दुःखानि, विपाकः कृतकर्मणाम्।
किं फलं कस्य चिन्तेति, विपाकविचयो भवेत्।।
सुख और दुःख कर्मों के विपाक-फल हैं। किस कर्म का क्या फल है, इस प्रकार का जो एकाग्र चिंतन किया जाता है, वह विपाक-विचय है। यह धम्र्यध्यान का तीसरा प्रकार है।
(37) लोकाकृतेश्च तद्वर्तिभावानां आकृतेस्तथा।
चिन्तनं क्रियते यत्तत्, संस्थानविचयो भवेत्।।
ध्यान का अर्थ है-चिंतनीय विषय में मन को एकाग्र करना, एक विषय पर मन को स्थिर करना, अथवा मन, वचन और काया की प्रवृत्तियों का निरोध करना (देखें-आठवें श्लोक की व्याख्या)। ध्याता ध्यान के द्वारा अपने ध्येय को प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसमें सफल भी होता है। ध्येय की इष्टता व अनिष्टता के आधार पर ध्यान भी इष्ट व अनिष्ट बन जाता है। सामान्यतः ध्येय अपरिमित है। जितने मनुष्य हैं, उन सबकी एकाग्रता भिन्न-भिन्न होती है। उनका प्रतिपादन करना असंभव है। संक्षेप में उसके चार प्रकार किए गए हैं। अनात्माभिमुखी जितनी एकाग्रता है। वह सब आत्र्त व रौद्र ध्यान है। आत्माभिमुखी जितनी एकाग्रता है, वह सब धर्म व शुक्ल ध्यान है।
आत्र्त और रौद्र ध्यान संसार के कारण हैं, अतः हेय हैं। धर्म और शुक्लध्यान मोक्ष के कारण हैं, अतः उपादेय हैं।
(38) उन्मादो न भवेद् बुद्धेः, अर्हद्वचनचिन्तनात्।
अपायचिन्तनं कृत्वा, जनो दोषाद् विमुच्यते।।
अर्हत् की वाणी के एकाग्र चिंतन से बुद्धि का उन्माद अथवा अहंकार नहीं होता, यह आज्ञाविचय का फल है। राग और द्वेष के परिणाम का एकाग्र चिंतन करने से मनुष्य दोष से मुक्त बनता है, यह अपायविचय का फल है।
अयथार्थता में दोषों का परिपालन और उद्भव होता है। जब मनुष्य सत्य को निकट से देख लेता है तब सहसा असत्य के पैर लड़खड़ा जाते हैं। आत्म-हितैषी व्यक्ति फिर अहित का अनुसरण नहीं करता। आज्ञाविचय आदि ध्यानों में रमण करने वाला यथार्थ का स्पर्श कर लेता है। उसकी मति-मूढ़ता सहज ही नष्ट हो जाती है। वह क्रमशः मुक्ति की ओर अग्रसर होता रहता है।
(क्रमशः)

