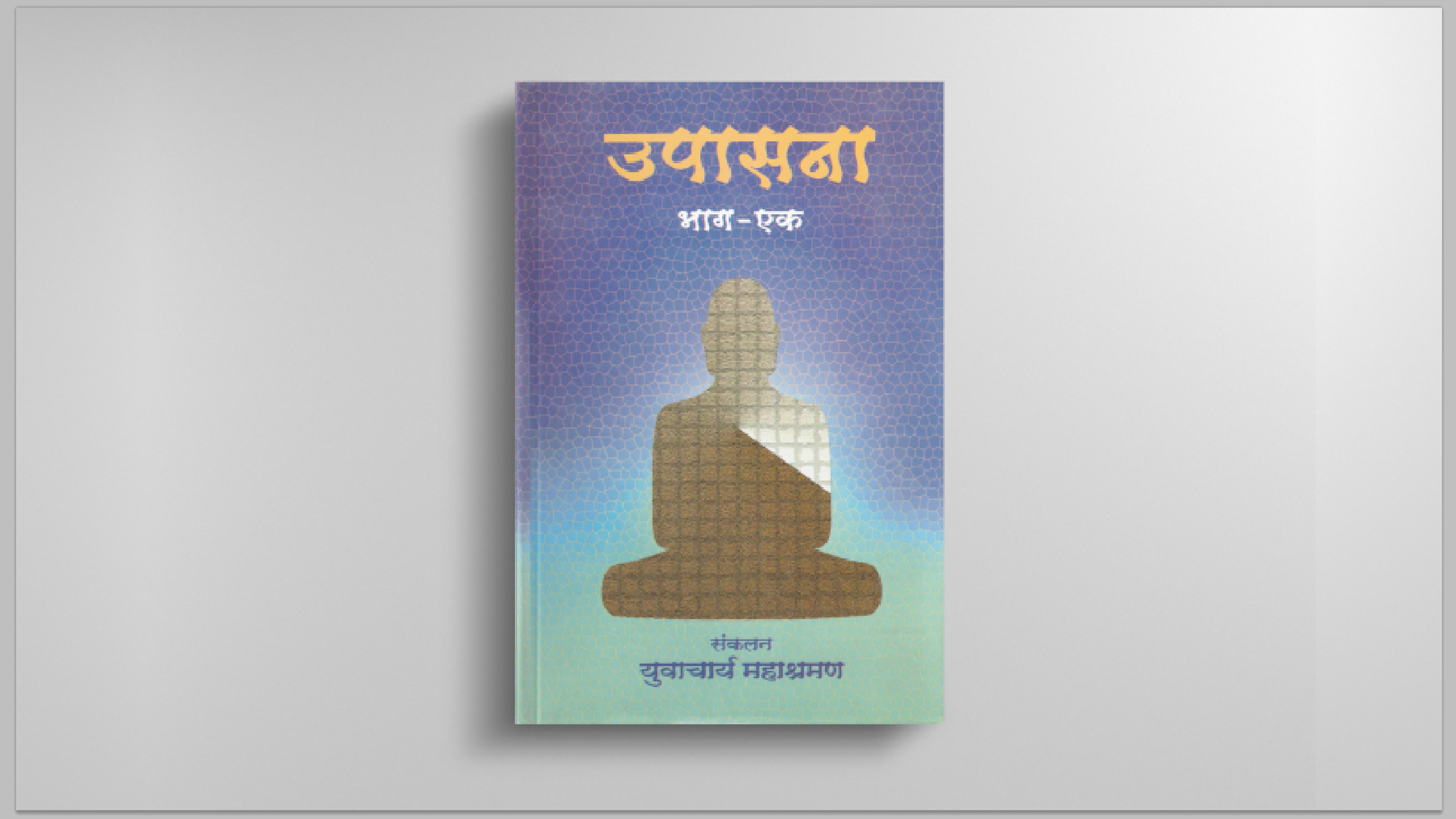
स्वाध्याय
उपासना
(भाग - एक)
प्रस्तुति
मैत्री
मैत्री का विराट् दर्शन
कहा जाता है-‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ वसुधा एक कुटुम्ब है, परिवार है। यह प्रत्यक्ष दर्शन की बात है। किंतु अतीत में जाएँ तो इसका अर्थ होगा-इस जगत् में जो प्राणी है, वह कभी न कभी तुम्हारे कुटुम्ब या परिवार का सदस्य रहा है। इसी तथ्य को उपाध्याय विनयविजयजी ने इस भाषा में प्रस्तुत किया-
सर्वे पितृभ्रातृपितृव्यमातृपुत्राङ्गजास्त्रीभगिनीस्तुषात्वम्।
जीवाः प्रपन्नाः बहुशस्तदेतत् कुटुम्बमेवेति परो न पश्चित्।।
सभी प्राणी अनेक बार तुम्हारे पिता, भ्राता, चाचा, माता, पुत्र, पत्नी, बहन और पुत्रवधू बन चुके हैं इसलिए यह जगत् तुम्हारा ही कुटुम्ब है, पराया या दूसरा नहीं है।
यह मैत्री का विराट् दर्शन है। हम वर्तमान संबंधों को बहुत सीमित बना लेते हैं। व्यक्ति मानता है-मेरे परिवार के दस, बीस अथवा पचास लोग हैं। वह उनके प्रति न्याय करता है और दूसरों के प्रति अन्याय करता है। पारिवारिक संबंधों के कारण वह अनेक अकृत्य कार्य कर डालता है। यदि वह कुछ गहरे में उतरकर देखे, तो मैत्री का यह विराट् दर्शन प्रस्तुत होता है-चारों तरफ तुम्हारे सगे-संबंधी हैं, निजी लोग हैं, कोई पराया नहीं है। तुम किसके साथ अन्याय और अत्याचार करते हो? तुम किसके साथ वैर-विरोध और शत्रुता का भाव रखते हो? शत्रुता के लिए कोई अवकाश ही नहीं बचता।
पवित्र भूमिखंड
महाभारत का प्रसंग है। मृत्युशय्या पर पड़े भीष्म ने कहा-देखो! मेरी दाहक्रिया उस पवित्र भूमिखंड पर करना, जहाँ आज तक किसी को जलाया नहीं गया हो। कहा जाता है-उसी समय एक देववाणी हुई, आकाश से ध्वनि प्रकट हुई-‘आप कौन से स्थान की बात कर रहे हैं? जहाँ आप उपस्थित हैं, मृत्युशय्या पर लेटे हैं, वहाँ सौ भीष्मों को जलाया जा चुका है। इसी स्थान पर तीन सौ पांडवों को तथा हजारो द्रोणाचार्यों को जलाया जा चुका है। कर्णों की तो कोई गिनती ही नहीं है। न जाने कितने कर्ण इस भूमिखंड पर जलाए गए हैं। भूमि का कोई खंड ऐसा नहीं मिलेगा, जहाँ यह सारा न हुआ हो। आप किस पवित्र स्थान की बात कर रहे हैं?’
अत्र भीष्मशतं दग्धं, पाण्डवानां शतत्रयम्।
द्रोणाचार्यसहस्रं तु कर्णसंख्या न विद्यते।।
इतना विराट् है हमारा जगत् और उसमें कितना चिरकालीन है जीव का परिभ्रमण, संबंध का ताना-बाना।
मैत्री का आधार
जैन साहित्य में कहा गया-ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है, ऐसा कोई कुल नहीं है, ऐसी कोई योनि नहीं है जहाँ कोई जीव अनेक बार या अनंत बार पैदा न हुआ हो।
न सा जाई न सा जोणी, न तं ठाणं न तं कुलं।
न जाया न माया, जत्थ सव्वे जीवा अणंतसो।।
जीव के परिभ्रमण, संसार-चक्र, जन्म-मरण के संबंधों पर टिका है मैत्री का दर्शन। यह ऐसा दर्शन है, जहाँ शत्रुता के लिए कोई अवकाश और स्थान नहीं है। यह मैत्री का महत्त्वपूर्ण आधार है।
विधायक भाव है मैत्री
मैत्री एक विधायक भाव है। क्रोध, घृणा, ईष्र्या, भय, द्वेष, चुगली, दोषारोपण, ये सारे निषेधात्मक भाव है। निषेधात्मक भाव के द्वारा आत्मा का पतन होगा और व्यक्तित्व का संकुचन हो जाएगा। संकोच और विकोच-ये दो अवस्थाएँ हैं। निषेधात्मक भाव से ग्रस्त व्यक्ति का व्यक्तित्व सिकुड़ जाता है, वह कभी बड़ा नहीं बनता। जिस व्यक्ति ने विधायक भावों का सृजन कर लिया, उसका व्यक्तित्व गुलाब के फूल की भाँति विकस्वर हो जाता है। जैसे ही मैत्री का भाव प्रस्फुटित होता है, व्यक्ति आनंद में निमज्जन करने लग जाता है। जैसे ही मैत्री का संवेग प्रबल होता है, ग्रंथियों का स्राव शुरू हो जाता है। यह माना जाता है-विशेष प्रकार के भाव जब जागृत होते हैं, ग्रंथियों का स्राव शुरू हो जाता है। जब विधायक भावों का संवेग होता है, तब लाभदायी, कल्याणकारी परिवर्तन लाने वाला स्राव शुरू हो जाता है। जब निषेधात्मक भावों का संवेग होता है, तब अहितकर स्राव शुरू हो जाता है। मैत्री का पुष्ट आधार है विधायक भाव से होने वाले परिणाम।
मैत्री की प्रक्रिया
मैत्री की प्रक्रिया को समझना भी आवश्यक है। जब तक हम मैत्री की प्रक्रिया को नहीं जान लेते, मैत्री के भाव का विकास नहीं किया जा सकता। उत्तराध्ययन सूत्र में मैत्री की बहुत सुंदर प्रक्रिया बतलाई गई है। मेत्तिं भूएसु कप्पए-सबके साथ मैत्री करो, यह प्रतिपादन मात्र नहीं किया, किंतु मैत्री की समग्र प्रक्रिया का निर्देश किया है। मैत्री की प्रक्रिया के तीन अंग हैं-क्षमापना, प्रह्लादभाव और मैत्री। मैत्री का परिणाम है भाव-विशुद्धि और निर्भयता। इसमें मैत्री का पूरा परिवार है। जब जीव सहन करता है, तब प्रह्लादभाव को पैदा करता है। क्षमा नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, तो मैत्रीभाव का विकास नहीं किया जा सकता। मैत्रीभाव का विकास करने के लिए सहिष्णु होना अत्यंत अनिवार्य है। जो सहिष्णु है, वह मैत्री का अनुशीलन कर सकता है। मैत्री बाद में है, पहले है क्षमा का अभ्यास। जो सहन करना नहीं जानता, मैत्री हो नहीं सकती। चाहे भाई-भाई का संबंध हो, मैत्री रह नहीं सकती। सबसे पहले सहन करने की शक्ति का विकास करना आवश्यक है।
मैत्री और प्रमोद
सहिष्णुता की शक्ति का परिणाम है-प्रह्लादभाव। प्रमोदभाव के बिना मैत्री फलित नहीं होती। यद्यपि प्राचीन आचार्यों ने, महर्षि पतंजलि ने, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य ने भी मैत्री और प्रमोद-इन दो भावनाओं का पृथक्करण किया है। उन्हें अलग-अलग माना है, किंतु वास्तव में प्रमोद मैत्री से पृथक् नहीं है, वह मैत्री का जनक है। सहिष्णुता पैदा होगी तो प्रमोद भावना पैदा होगी, दूसरों की विशेषताओं, अच्छाइयों के प्रति मन में प्रमोद भावना उभरेगी, एक सुखानुभूति और आह्लाद का भाव प्रकटेगा। प्रह्लादभाव की अवस्था में ही मैत्री का भाव विकसित होगा, सब प्राणियों के प्रति मैत्री जागेगी।
मैत्री वह है
यदि हम सीधे मैत्री करना चाहें तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। क्षमा और प्रमोदभाव-इन दो गुणों का विकास होगा, तब सबके प्रति मैत्री होगी। कितना सुंदर कहा गया है-मैत्री मनुष्य के साथ, मैत्री अपने पास रहने वाले के साथ, मैत्री सब जीवों के साथ। मैत्री किसी एक के साथ नहीं होती। यदि प्राणीमात्र के प्रति आपमें मैत्री का विकास हुआ है तो वह मैत्री है। यदि किसी एक के प्रति हुआ है तो वह और कुछ है। मैत्री एक के साथ नहीं हो सकती। वह होती है तो सबके साथ होती है, अन्यथा मैत्री होती ही नहीं है।
मैत्री का परिणाम है-भाव विशुद्धि। जिसमें मैत्रीभाव का विकास होगा, उसमें विधायक भाव का विकास होगा। जहाँ भाव विशुद्धि है, वहाँ अभय है। जहाँ भाव अशुद्धि है, वहाँ भय बना रहता है। आज भय की समस्या बहुत विकट है। व्यक्ति चोर और डाकू से डरता है, उग्रवाद से डरता है और वह कभी-कभी पत्नी से भी डरने लग जाता है।
भय का निदर्शन
एक आदमी हमेशा आॅफिस से आते ही जेब से रुपये निकाल कर अलमारी में रखता है और बाहर ताला लगा देता है। उसे सदा भय रहता है कि पत्नी कोट से रुपया निकाल न ले। एक दिन वह जल्दी में था। कोट से रुपया निकालना भूल गया। दूसरे दिन कोट पहना। उसने देखा-रुपये सुरक्षित हैं। पत्नी से पूछा-क्या आज कोट की सफाई नहीं की?
‘मैंने की तो थी।’
‘ऐसा लगता है-सफाई नहीं की है।’
‘नहीं, मैंने कोट की सफाई की है।’
‘यह कैसे हो सकता है कि कोट की सफाई हो और जेब की सफाई न हो? इसमें रुपये वैसे के वैसे पड़े हैं, इसलिए लगता है कि सफाई नहीं हुई होगी।’
यह भय की समस्या का निदर्शन है। व्यक्ति दूसरों से ही नहीं डरता, अपने आप से ही बहुत डरता है। आज के मनोवैज्ञानिकों ने भय के नब्बे प्रकार बतलाए हैं। व्यक्ति कुत्ते से डरता है, बिल्ली से डरता है, अनेक प्रकार के प्राणियों से डरता है। जब मैत्री घटित हो जाती है, भाव विशुद्धि होती है, व्यक्ति अभय और निर्भय बन जाता है।
अहिंसा और मैत्री
अहिंसा का विराट् रूप मैत्री के दर्शन में प्रकट हुआ है। अहिंसा एक नकारात्मक शब्द है-किसी को मत मारो। अनेक लोगों ने कहा-हमें नकारात्मक नहीं, सकारात्मक चाहिए, विधायक चाहिए। मैत्री अहिंसा का सकारात्मक रूप है। चाहे अहिंसा कहें या मैत्री-दोनों एक ही बात है। यह मैत्री का विशाल दर्शन किसी कटघरे में बंधा हुआ नहीं है। नकारात्मक रूप है अहिंसा और सकारात्मक रूप है मैत्री। यदि जागरूकता नहीं है, प्रतिक्रिया-विरति नहीं है तो मैत्री की दिशा में चरण आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि संवेगात्मक प्रतिक्रियाएँ होती रहती हैं, माया, कपटपूर्ण व्यवहार चलता है तो मैत्री की संभावना नहीं की जा सकती। व्यवहार में यह देखा जाता है कि माया का आचरण भी बहुत प्रतिष्ठित हो गया है। व्यक्ति बहुत छलना करता है। छलना की प्रवृत्ति ऐसी बन गई है कि आदमी किसी का विश्वास नहीं करता। मैत्री परम विश्वास का स्रोत है। मैत्री होगी तो उसके पीछे कोई प्रतिक्रियात्मक वृत्ति नहीं होगी। जहाँ प्रतिक्रियात्मक वृत्तियाँ नीचे रह जाती हैं, वहाँ मैत्री घटित होती है। माया विश्वास की जड़ को उखाड़ देती है।
जहाँ ये संवेगात्मक प्रतिक्रियाएँ होती हैं, संबंध और रिश्ते टूटते रहते हैं, विश्वास भी समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में आध्यात्मिक मैत्री का विकास कैसे हो सकता है? व्यावहारिक मैत्री कामचलाऊ बात है। आध्यात्मिक मैत्री से उसकी तुलना नहीं की जा सकती।
कहा गया-तू सत्य की खोज कर, तुम्हें पता चलेगा-इस विराट् संसार में मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने जो संबंध बनाए हैं, उन संबंधों की दुनिया इतनी छोटी नहीं है, वह बहुत बड़ी है। क्या यह संभव है-दो दिन का संबंध संबंध बन जाए, हजारों-हजारों वर्षों का संबंध संबंध न रहे। संबंधों का एक पूरा चक्र है, शंृखला है। इस सच्चाई को समझकर इस सूत्र का उच्चारण करो-‘मेत्तिं भूएसु कप्पए।’ यदि हम इस समग्र बात को छोड़ देते हैं, केवल एक तत्त्व को पकड़ लेते हैं तो मैत्री का दर्शन समझ में नहीं आएगा। (क्रमशः)

