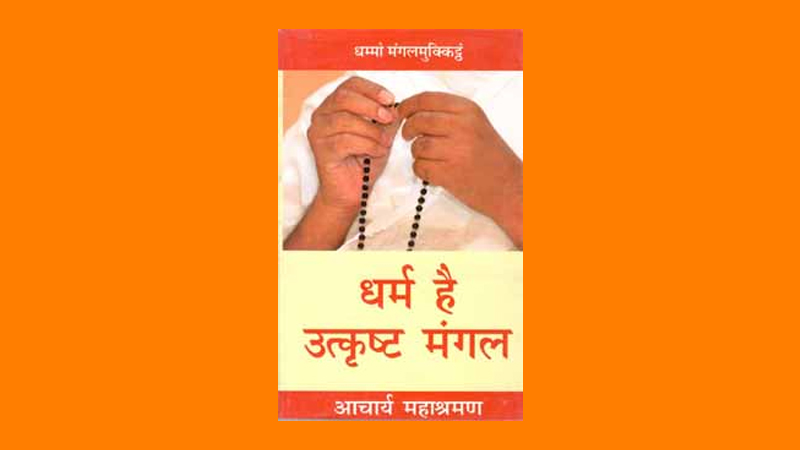
स्वाध्याय
धर्म है उत्कृष्ट मंगल
करणी बांझ न होय
दशम गुणस्थान में छह कर्मों का बंध होता है और ग्यारहवें गुणस्थान में केवल सात वेदनीय कर्म का ही बंध होता है, वह भी मात्र दो समय की स्थिति (ड्युरेशन) वाला होता है। यह ऐर्यापथिक बंध कहलाता है। प्रश्न है कि यहाँ सात वेदनीय बंध हो सकता है तो शुभ नाम और उच्च गोत्र का बंध क्यों नहीं हो सकता? वे भी तो पुण्य कर्म हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का बंध तो इसलिए नहीं हो सकता कि ये कर्म अशुभ हैं और अशुभ कर्म के कारणभूत कषाय और अशुभ योग आश्रव वहाँ उपलब्ध नहीं रहते हैं। कितु शुभ नाम और उच्च गोत्र के बंधन में क्या कठिनाई है?
विचार करने पर ज्ञात होता है-वीतराग अवस्था में जो कर्म बंधता है, वह ठहर नहीं सकता, बंधा कि झड़ने की तैयारी। बंधा, भुगता और झड़ा। नाम कर्म और गोत्र कर्म की बंध स्थिति इस प्रकार की नहीं है। उनकी जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त की होती है। दूसरी बात आठ कर्मों में सात कर्म सांपरायिक स्वभाव के ही होते हैं। संपराय का अर्थ है कषाय। यानी कषाययुक्त आत्मा के ही उनका बंध होता है। वेदनीय कर्म सांपरायिक स्वभाव का तो होता ही है। सात वेदनीय और असात वेदनीय दोनों सांपरायिक स्वभाव के होते हैं, किंतु उनमें सात वेदनीय कर्म ऐर्यापथिक स्वभाव का भी होता है। वह ऐर्यापथिक स्वभाव वाला सात वेदनीय कर्म ही वीतराग के (ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें गुणस्थान में) बंधता है।
दशम गुणसथान के पश्चाद्वर्ती गुणस्थानों में कषाय का अभाव होने के कारण सात कर्मों का बंध हो नहीं सकता, केवल सात वेदनीय, जो ऐर्यापथिक स्वभाव का होता है, का बंध होता है तथा इतनी अल्प स्थिति वाला कर्म केवल सात वेदनीय ही होता है इसलिए भी वहाँ (वीतराग-अवस्था में) अन्य कर्मों का बंध नहीं हो सकता। वहाँ केवल योग (प्रवृत्ति) के कारण बंध होता है, कषाय वहाँ होता नहीं और कषाय के अभाव में दीर्घकालिकता हो नहीं सकती। केवलयोग से होने वाला बंध ऐर्यापथिक बंध कहलाता है। यह बंध अबंध से सदृश अथवा नाममात्र का सा बंध होता है। चौदहवें गुणस्थान में योग भी नहीं होता। वहाँ सर्वथा अयोग की स्थिति होती है, कोई भी आश्रव नहीं होता, इसलिए चौदहवाँ गुणस्थान सर्वथा अबंध रहता है, नया बंधन नहीं होता, पुराने बंधे हुए चार अघाती कर्म ही रहते हैं।
जैन दर्शन नियंता (कर्त्तारूप ईश्वर) को नहीं मानता, किंतु वह नियति (सार्वभौम नियम, युनिवर्सल लॉ) को स्वीकार करता है। नियति का वैसा रूप भी जैन दर्शन को मान्य है, जिसमें आत्मकर्तृत्व (कर्म, पुरुषार्थ) भी अस्वीकृत हो जाता है। एक जीव अभव्य (मोक्ष जाने के अयोग्य) है। यह अभव्यता आठ कर्मों में से कौन से कर्म के उदय से है? यह किसी भी कर्म के उदय से नहीं है। यह पारिणामिक भाव का स्वतंत्र क्षेत्र है। इसमें किसी भी कर्म का हस्तक्षेप मान्य नहीं है। अभव्य है, तो है; भव्य है, तो है; प्रकृति या नियति से वैसा है क्यों है? इस ‘क्यों’ का उत्तर मेरे पास नहीं है। सब बातें कर्माधारित नहीं होती हैं, कर्मातीत स्थितियाँ भी होती हैं। इस पारिणामिक भाव को हम आत्मकर्तृत्व नहीं कह सकते, यह पारिणामिक भाव जैन दर्शन का निरपेक्ष नियतिवाद है।
दुःख का मूल
संसार में दुःख है-यह एक प्रत्यक्ष सच्चाई है। दुःख का कारण भी दिखाई देता है। दुःखमुक्ति भी संभव मानी गई है और दुःखमुक्ति का मार्ग भी है। दुःख, दुःख-हेतु, दुःखमुक्ति और दुःखमुक्ति-हेतु-ये चार सच्चाइयाँ हैं। नव तत्त्वों में इन चारों सच्चाइयों को खोजें तो इस प्रकार उत्तर मिलता है-पाप तत्त्व दुःख है। आश्रव उसका हेतु है। मोक्ष दुःखमुक्ति है। संवर दुःखमुक्ति का मूल मार्ग है। जैन दर्शन का सार इस रूप में प्रतिपादित है-
आश्रवों भवहेतुः स्यात्, संवरो मोक्षकारणम्।
इतीयमार्हती दृष्टिः, शेषमस्याः प्रप×चनम्।।
आश्रव संसार-भ्रमण का हेतु है और संवर संसार-मुक्ति का। यही आर्हत (जैन) दर्शन है। शेष जो कुछ है इसी का विस्तार है।
नव तत्त्वों में पाँचवाँ तत्त्व है आश्रव। इसे आश्रवद्वार भी कहा जाता है। पुण्य-पाप का कारण आश्रव है। जैसे मकान में प्रवेश के लिए द्वार, कुंड के नाला और नौका के छिद्र होता है, वैसे ही कर्म के जाने (आत्मा के चिपकने) का रास्ता आश्रव होता है। आश्रव के पाँच प्रकार हैं-मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। ‘शांतसुधारस भावना’ में प्रमाद की पृथक् विवक्षा के अभाव में आश्रव चार ही बतलाए गए हैं-मिथ्यात्वाविरति कषाययोगसंज्ञाश्चत्वारः सुकृतिभिराश्रवाः प्रदिष्टाः। विस्तार की विवक्षा में आश्रव के बीस भेद भी हो जाते हैं। यह विस्तार योग आश्रव के भेदों से हुआ है। अति संक्षेप में जाएँ तो, मुझे लगता है, आश्रव दो ही रह जाएँगे-कषाय और योग। कर्म-बंधन के दो ही कारण हैं। कषाय और योग। मिथ्यात्व अव्रत और प्रमाद-ये तीनों कषाय की ही विभिन्न अवस्थाएँ हैं। प्रथम और तृतीय गुणस्थान में मिथ्यात्व आदि पाँच आश्रव, दूसरे व चौथे गुणस्थान में अव्रत आदि चार आश्रव, पाँचवें गुणस्थान में अपूर्ण अव्रत तथा प्रमाद आदि तीन आश्रव, छट्ठे गुणस्थान में प्रमाद आदि तीन आश्रव, सातवें से दसवें गुणस्थान तक कषाय और शुभ योग आश्रव, ग्यारहवें से तेरहवें गुणस्थान तक मात्र शुभ योग आश्रव होता है। चौदहवाँ गुणस्थान अनाश्रव होता है, अबंध होता है। छट्ठे गुणस्थान में अशुभ (सावद्य) योग वर्जनीय है, किंतु मोहवश हो भी सकता है। ग्यारहवें गुणस्थान में मोह (कषाय) की विद्यमानता रहती है परंतु वह सर्वथा उपशांत रहता है। वह वहाँ न विपाकोदय में और न ही प्रदेशोदय में रहता है, इसलिए कर्म का आश्रवण उससे हो नहीं सकता।
(क्रमशः)

