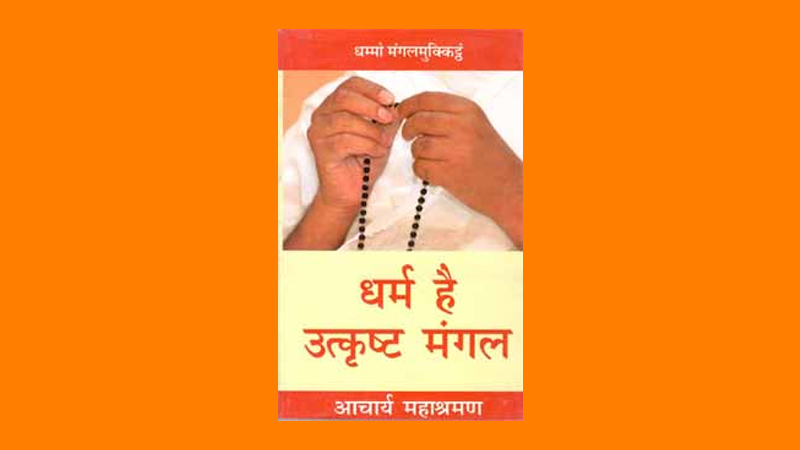
स्वाध्याय
धर्म है उत्कृष्ट मंगल
करणी बांझ न होय
संसार (जीव जगत्) की विचित्रता का आधार व कारण कर्म है। कर्म का कारण आश्रव है। इसलिए संसार की विचित्रता का मूल आधार आश्रव है। मिथ्यात्व आदि चार आश्रव और अशुभ योग आश्रव तो दुःख-हेतु हैं ही। शुभयोग आश्रव को सीधा दुःखहेतु नहीं कहा जा सकता, किंतु जब तक वह रहता है, पूर्ण दुःख-मुक्ति नहीं हो सकती। शुभयोग से अशुभ कर्म निर्जरण तथा शुभकर्म आश्रवणµये दो कार्य होते हैं। निर्जरण अपने आपमें सुख है, सुख का मार्ग है।
विशुद्ध (केवल) योग में बंधन की दीर्घकालिकता व अनुभागतीव्रता की क्षमता नहीं होती। उसके साथ परिणाम जुड़ता है, उसके आधार पर निष्पत्ति आती है। एक समान क्रिया की, दृष्टिकोण और परिणाम की भिन्नता के कारण, निष्पत्ति भिन्न-भिन्न प्रकार की हो जाती है। दो व्यक्ति ध्यानस्थ बैठे हैं। बाहर से दोनों समान अनुष्ठान में संलग्न हैं, परंतु एक मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ रहा है और एक बंधन की दिशा में। एक के मन में कर्मनिर्जरा का भाव है, दूसरे के मन में दिखावे की भावना है।
दो व्यक्ति साधुओं के स्थान पर एक साथ जा रहे हैं। गतिक्रिया दोनों की समान है। एक संयमयुक्त चल रहा है, उसका उद्देश्य है साधुओं का प्रवचन-श्रवण। दूसरा असंयम से चल रहा है, उसका उद्देश्य है साधुओं के स्थान पर आने वाले दर्शनार्थियों के जूतों को चुराना। अब तक पहले ने प्रवचन नहीं सुना है, दूसरे ने जूतों को चुराया नहीं है। दोनों चल रहे हैं। फिर भी एक कर्मनिर्जरा कर रहा है और दूसरा पापकर्मबंधन कर रहा है। एक ही व्यक्ति एक ही क्रिया में स्थित है, किंतु परिणामों की भिन्नता के कारण कभी वह पाप कर्म बाँध लेता है और कभी कर्मों को क्षीण कर देता है।
राजर्षि प्रसन्नचंद्र साधना में लीन थे। परंतु भावों से युद्धस्थल में पहुँच गए, हिंसा के संस्कार सक्रिय हो गए, वे नरक में जाने के योग्य बन गए। परिणामों की दिशा बदली, हिंसा से अहिंसा व संयम के भावों में स्थित हुए, वहीं उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो गया। शरीर से साधना में स्थित थे। परंतु परिणाम की भिन्नता ने भिन्न-भिन्न निष्पत्ति ला दी। दृष्टिकोण का मिथ्यात्व और दूषित परिणाम व्यक्ति को भटकाते हैं।
आश्रव को कर्मकर्त्ता माना गया है। नव तत्त्वों में एक आश्रव तत्त्व ही कर्मों का कर्त्ता है। कर्मों का कर्त्ता छह द्रव्यों में जीव और नव तत्त्वों में जीव तथा आश्रव माना गया है। यहाँ जीव को कर्मकर्त्ता के रूप में स्वीकार किया गया है, वह जीव का आश्रवात्मक परिणाम ही है, उससे भिन्न और कुछ नहीं है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आश्रव ही कर्मकर्त्ता है। कर्म का अकर्त्ता छह द्रव्यों में कौन और नौ तत्त्वों में कौन? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म का अकर्त्ता छह द्रव्यों में छहों तथा नौ तत्त्वों में आठ तत्त्व आश्रव को छोड़कर।
आचार्य भिक्षु ने ‘तेरहद्वार’ में आश्रव और कर्म की भिन्नता को स्पष्ट किया है। कर्म आगंतुक है और आश्रव आगमन-मार्ग है। मकान का द्वार अलग है और आगंतुक मनुष्य अलग है। ठीक इसी प्रकार कर्म अलग है और आश्रव अलग है।
एक व्यक्ति जीव-हिंसा करता है। उसके पाप कर्म का बंधन होता है। यहाँ तीन तथ्य हैं। जिस कर्म के उदय से व्यक्ति जीव-हिंसा में प्रवृत्त होता है, उस कारणभूत कर्म को ‘प्राणातिपातपापस्थान’ कहा जाता है। जीव को मारता है, वह मारना प्राणातिपात क्रिया है, प्राणातिपात आश्रव है, उससे जो पाप कर्म का बंध होता है, वह प्राणातिपात पाप-बंध है।
साधना का विकास-क्रम है आश्रव से अनाश्रव की दिशा में प्रस्थान। ज्यों-ज्यों व्यक्ति आश्रवमुक्त बनता है, त्यों-त्यों वह दुःख के मूल को खत्म कर डालता है।
(5) संवरो मोक्षकारणम्
जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ जैन दर्शन ईश्वर को नियन्ता अथवा सृष्टि के कर्ता-हर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता। हमारे सुख-दुःख के जिम्मेदार के रूप में भी वहाँ ईश्वर को नहीं माना गया है। नियन्ता को न मानने पर भी जैन दर्शन नियति (सार्वभौम, सार्वकालिक अटल नियम) को किसी सीमा तक अवश्य मान्य करता है। नियति को सर्वथा छोड़कर जीवन और जगत् की व्याख्या नहीं की जा सकती। आत्म-कर्तृत्व की भी सीमा है। कुछ ऐसे पहलु भी हैं जहाँ आत्मकर्तृत्व का सिद्धांत लागू नहीं होता। एक जीव जीव है, क्यों? वह अजीव क्यों नहीं? एक अजीव पदार्थ अजीव है, क्यों? वह जीव क्यों नहीं? इस ‘क्यों’ का उत्तर यही हो सकता है कि यही नियति है, प्रकृति है, प्रारिणामिक भाव है। भव्य अभव्य की स्थिति में भी किसी आत्मकर्तृत्व का हाथ नहीं है। यह सारा विशुद्ध नियति अथवा पारिणामिक भाव का क्षेत्र है। धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों का अस्तित्व भी पारिणामिक भाव है। उन द्रव्यों को प्रवृद्ध और नष्ट नहीं किया जा सकता।
छह द्रव्यों में आत्मा (जीवास्तिकाय) भी एक द्रव्य है। उसकी दो अवस्थाएँ होती हैंµस्वाभाविक अवस्था और वैभाविक अवस्था। वैभाविक अवस्था से मुक्त हो स्वाभाविक अवस्था में स्थित होना ही अध्यात्म और धर्माराधना का उद्देश्य होता है। उसके लिए आश्रवनिरोध आवश्यक होता है।
नव तत्त्वों में छठा तत्त्व है संवर। यह स्वभावतः आश्रव से ठीक विपरीत होता है। आश्रव (कर्म-आगमन के द्वार) को रोकना ही संवर है। उसके मुख्य पाँच प्रकार हैंµसम्यक्त्व संवर, व्रत संवर, अप्रमाद संवर, अकषाय संवर और अयोग संवर। विस्तार में उसके बीच भेद भी किए जा सकते हैं। (क्रमशः)

