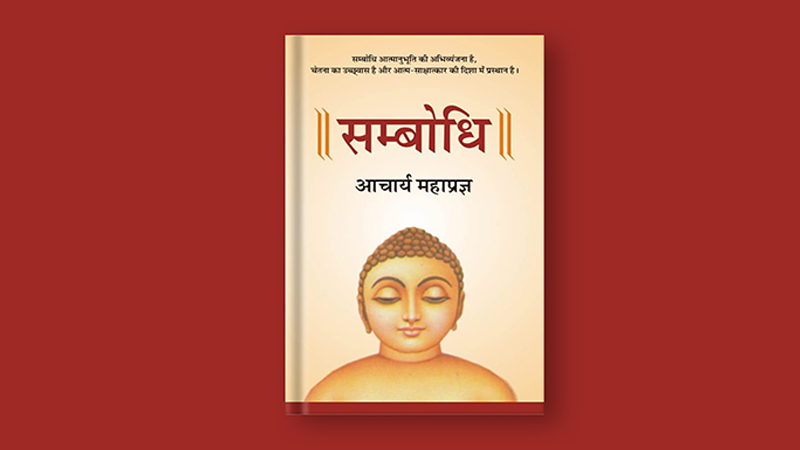
स्वाध्याय
संबोधि
(िपछला शेष)
९०- संहरेत् हस्तपादौ च, मनः पंचेन्द्रियाणि च ।
पापकं परिणामञ्च, भाषादोषञ्च तादृशम् ॥
मेधावी पुरुष हाथ, पांव, मन, पांच इन्द्रियों, असद् विचार और वाणी के दोष का उपसंहार करे।
९१- कृतञ्च क्रियमाणञ्च भविष्यन्नाम पापकम् ।
सर्वं तन्नानुजानन्ति, आत्मगुप्ताः जितेन्द्रियाः ॥
जो पुरुष आत्मगुप्त और जितेन्द्रिय हैं, वे अतीत, वर्तमान और भविष्य के पापों का अनुमोदन नहीं करते ।
पाप अशुभ प्रवृत्ति है। अशुभ प्रवृत्ति में व्यक्ति पहले अपने को सताता है और जो स्वयं को दुःख देता है वही दूसरे को सताता है, इस दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि पाप है अपने को दुःख देना । जो आत्मस्थ हैं, स्वयं में स्थित हैं और जिनकी इन्द्रियां शांत हो गई हैं वे स्वयं में प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। सुखी व्यक्ति न स्वयं को सताता है और न दूसरों को कष्ट देता है। इसलिए पाप का अनुमोदन उसके द्वारा संभाव्य नहीं होता। अध्यात्म की साधना है - स्वयं में प्रतिष्ठित होना। पाप से बचने की अपेक्षा स्वयं में स्थित होने का प्रयत्न अधिक सशक्त है। अपने से बाहर जाना ही पाप है ।
मेघः प्राह
९२- प्रभो ! प्रसादमासाद्य, चेतः पुलकितं मम ।
वाणी सुधारसासिक्ता, संतापं हरते नृणाम् ॥
मेघ बोला- प्रभो ! आपका प्रसाद प्राप्त कर मेरा मन पुलकित हो उठा।
आपकी सुधारस से सिक्त वाणी मनुष्यों के संताप का हरण कर लेती है ।
मन्दिर में प्राप्त होने वाला प्रसाद स्थूल है और गुरु सान्निध्य में प्राप्त होने वाला भिन्न है। एक सीधा और शीघ्र प्रभावकारी होता है। 'गुरु' शब्द में ही कुछ विशिष्टता है, उस विशिष्टता से युक्त व्यक्ति ही गुरु होता है। जो 'गु' अंधकार से 'रु' प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु होता है। 'गु' अर्थात् ग्रंथातीत और 'रु' यानी रूपातीत-जो शिष्य का तीन गुणों व नाम रूप के मिथ्या जगत् से सम्यग् बोध देकर मुक्ति की दिशा में अग्रसर करता है, वह गुरु होता है। ऐसे ही गुरु की उपासना संताप का उन्मूलन करती है, दिव्यदृष्टि प्रदान करती है और अज्ञान-तम को विध्वंस करती है। जिस स्वरूप- बोध के अभाव में अनंत दुःखों को भोगा, दुःखों में ही अनंत जीवन गुजरे, गुरु उस स्वरूप-बोध को देकर दुःखों की जड़ें हिला देते हैं और सुख का स्रोत भीतर प्रकट कर देते हैं। शिष्य जब इस स्थिति को प्राप्त करता है, तब उसके आनंद की सीमा नहीं रहती। स्वतः ही उसके मुख से अनिर्वचनीय शब्द फूट पड़ते हैं। मेघ का स्वर इसी सत्य का द्योतक है।
इति आचार्यमहाप्रज्ञविरचिते संबोधिप्रकरणे
हेय - ज्ञेय - उपादेयनामा द्वादशोऽध्यायः ।

