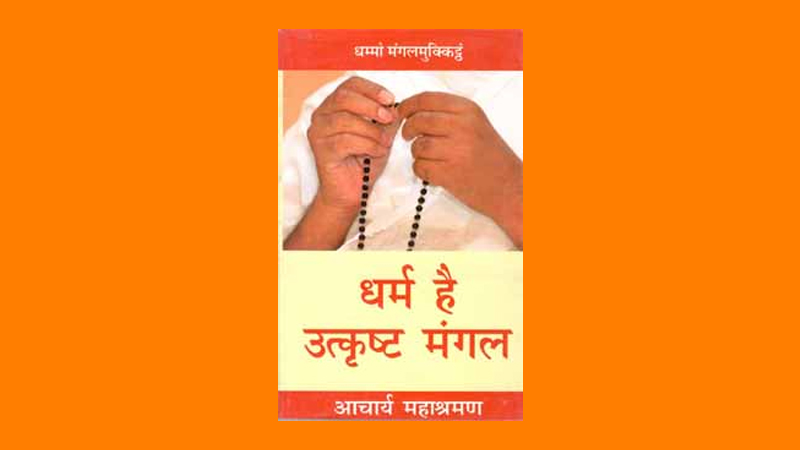
स्वाध्याय
धर्म है उत्कृष्ट मंगल
अनादिपारिणामिक भाव विशुद्ध नियति का क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर हमारे जीवन-व्यवहार में नियति और पुरुषार्थ दोनों का योग रहता है। किसी एक को एकान्त रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता। जहां तक मैं समझ पाया हूं नियतिवादी को भी पुरुषार्थ का प्रयोग तो करना ही होता है। क्या नियतिवादी क्षुधा शान्ति के लिए हाथ से कवल ग्रहण कर मुंह में नहीं रखता? कया वह शौचार्थ शौच स्थान पर नहीं जाता है? क्या वह अपने शरीर की सफाई नहीं करता है? क्या नियतिवादी अन्य कार्य नहीं करता है? यदि वह करता है तो इसका अर्थ हुआ कि उसे (नियतिवादी को) पुरुषार्थ का सहारा तो लेना ही पड़ता है। हां, यह ठीक है कि जैसा सर्वज्ञ ने जाना-देखा है, वैसा ही हुआ, होता है और होगा। किन्तु इस तथ्य के आधार पर सर्वथा पुरुषार्थहीन नहीं बना जा सकता।
भगवान ऋषभ ने जान लिया कि उनका पौत्र मरीचि इस अवसर्पिणी काल का, भरत क्षेत्र का अन्तिम तीर्थकर होगा। जैसा जाना, वैसा ही होना था, वह हो गया, किन्तु भगवान ऋषभ ने यह भी तो जाना होगा कि मरीचि साधनामय पुरुषार्थ करेगा, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बन्धन करेगा तब कहीं तीर्थंकर बनेगा। यदि ऋषभ मरीचि के जीव के इस प्रकार के भावी पुरुषार्थ को नहीं देखते तो मरीचि के तीर्थंकर होने की स्थिति को क्या वे अपने ज्ञान से देख पाते? नियति की पृष्ठभूमि में आमतौर से पुरुषार्थ का योग भी किसी न किसी रूप में रहता ही है। पुरुषार्थ का होना भी एक नियति है, ऐसा तो माना जा सकता है, किन्तु पुरुषार्थ को सर्वथा नकारा नहीं जा सकता।
नियति से जो होना है, वह तो होगा ही। भले ही आदमी नियतिवाद को माने या न माने। नियति हमारे हाथ की चीज नहीं है। हमारे हाथ की चीज पुरुषार्थ हो सकता है। इसलिए आदमी को यथासंभव सत्पुरुषार्थ करना चाहिए। सत्पुरुषार्थ का फल अच्छा ही होता है। इस प्रकार नियतिवाद और पुरुषार्थ वाद-दोनों की आसेवना हो जाती है। नियति से जो होना है, वह तो होता ही है, उसमें कुछ करने की अपेक्षा नहीं। पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ देवता की भी आराधना हो जाता है। इसलिए व्यक्ति पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ to do (टु डू) है, नियति to be (टु बी) है। इसलिए पुरुषार्थी व्यक्ति के जीवन में नियति और पुरुषार्थ दोनों का समन्वय हो सकता है। नियति और पुरुषार्थ की सीमा का अवबोध आवश्यक है। 'नियति' शब्द का प्रयोग मैंने भवितव्यता के अर्थ में किया है और 'पुरुषार्थ' शब्द का प्रयोग प्रयत और पराक्रम के अर्थ में किया है।
पूर्वाभ्यास जिनकल्प साधना का
अध्यात्म साधना के उन्मुक्त विकास के लिए साधु-दीक्षा का स्वीकरण बहुत उपयोगी है। साधु लम्बे समय तक केवल दो ही गुणस्थानों में रहता है, वे हैं-छठा (प्रमत्त संयत) गुणस्थान और तेरहवां (सयोगी केवली) गुणस्थान। तेरहवें गुणस्थान में विद्यमान सभी साधु ज्ञान, दर्शन और चारित्र की दृष्टि से समान होते हैं, उनमें कोई तारतम्य नहीं होता। एक तीर्थंकर और एक सामान्य केवली इस दृष्टि से एक समान हैं। किन्तु छठे गुणस्थान में विद्यमान साधुओं में निर्मलता की दृष्टि से बड़ा तारतम्य होता है। अतिमुक्तक जैसा चंचल कुमारश्रमण पानी में पात्र को प्रवाहित कर क्रीडारत हो जाने वाला मुनि भी छठे गुणस्थान में हो सकता है और गजसुकुमाल जैसा बारहवीं भिक्षु प्रतिमा की कठोर साधना में स्थित मुनि भी छठे गुणस्थान में हो सकता है। पुलाक निर्गंथ भी, जो दोषों का सेवन कर लेता है, छठे गुणस्थान में और छद्मस्थ तीर्थंकर भगवान महावीर भी छठे गुणस्थान में। इन उदाहरणों से छठे गुणस्थान की व्यापकता और अन्तनिर्हित तरतमता स्पष्ट हो जाती है।
प्राचीनकाल में साधना के विभिन्न आयाम थे जिनके माध्यम से साधु साधना की गहराई में बैठते थे। वर्तमान समय में आमतौर से पहले की अपेक्षा ज्ञान, दर्शन और चारित्र का ह्रास हुआ है, शारीरिक बल और धृति का भी ह्रास हुआ है। फिर भी आज के युग में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है, पूर्णता न भी मिले तो पूर्णता का सामीप्य तो साधा ही जा सकता है। अपेक्षा है कि छठे गुणस्थान में ठहराव न आए और अनपेक्षित निराशा न आए। प्राचीन काल में (भगवान महावीर के बाद तक) साधना का एक प्रयोग था 'जिनकल्प'। यह अपने आप में एक कठोरतम साधना थी। इसके लिए हर कोई मुनि पात्र नहीं होता था, विशेष योग्यता सम्पन्न मुनि ही इसे स्वीकार कर सकता था। स्वीकार करने से पूर्व अपने आपको उसके अनुरूप ढालना पड़ता था, उसके लिए पूर्वाभ्यास करना होता था। उस पूर्वाभ्यास को जानने मात्र से जिनकल्प की महत्ता अनुमानित हो जाती है। वृहत्कल्प भाष्य में उसका वर्णन प्राप्त है। जिनकल्प को स्वीकार करने वाले भिक्षु के लिए पांच भावनाएं बतलाई गई हैं-तप भावना, सत्त्व भावना, सूत्र भावना, एकत्व भावना और बल भावना।

