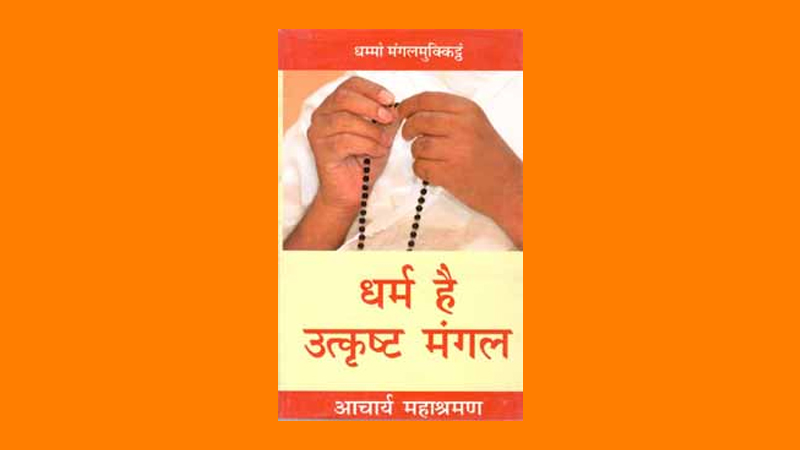
स्वाध्याय
धर्म है उत्कृष्ट मंगल
महावीर की अहिंसा है– 'आयतुलेपयासु' परम अहिंसक वह होता है जो संसार के सब जीवों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, जो सब जीवों को अपने समान समझता है। इस आत्मतुला को जाननेवाला और इसका आचरण करनेवाला ही महावीर की परिभाषा में अहिंसक है। उनकी अहिंसा की परिभाषा में किसी प्राणी का प्राण-वियोजन करना ही हिंसा नहीं है, किसी के प्रति बुरा चिन्तन करना भी हिंसा है।
परम अहिंसक वह होता है जो अपरिग्रही बन जाता है। हिंसा का मूल है परिग्रह। परिग्रह के लिए हिंसा होती है। आज विश्व में परिग्रह की समस्या है। एक महिला जिसके पैरों में सोने के कड़े हैं, उसके पैर काट लिये जाते हैं। एक औरत जिसके कानों में स्वर्ण के कुण्डल हैं, उसके कान काट लिये जाते हैं। ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं? परिग्रह के लिए। परिग्रह में आसक्त व्यक्ति निरपराध प्राणी की भी नृशंस हत्या कर डालता है। एक व्यक्ति धन आदि के प्रलोभन में आकर किसी के कहने से किसी की हत्या कर डालता है। बड़ी-बड़ी डकैतियां और चोरियां होती हैं, इन सब अपराधों का केन्द्र-बिन्दु है-परिग्रह। भगवान महावीर ने दुनिया को अपरिग्रह का संदेश दिया वे स्वयं अकिंचन बने। उन्होंने घर, परिवार राज्य, वैभव सब कुछ छोड़ा, यहां तक कि वे निर्वस्त्र बने। कुछ लोग उन अपरिग्रही महावीर को भी अपने जैसा परिग्रही बना देते हैं। कई जैन मन्दिरों में महावीर की प्रतिमा बहुमूल्य आभूषणों से आभूषित मिलती है। यह महावीर का सही चित्रण नहीं है। हम स्वयं अपरिग्रही न बन सकें तो कम से कम महावीर को तो अपरिग्रही रहने दें, उन्हें तो परिग्रही न बनाएं। भगवान महावीर गृहवासियों के लिए 'इच्छा-परिमाण' अणुव्रत दिया। एक श्रावक अपने परिग्रह को असीम न बनाये, एक सीमा से अधिक परिग्रह को न बढ़ाए।
महावीर की अहिंसा है समता। समता के बिना अहिंसा नहीं सधती। समता का अर्थ है-हर स्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना। हिंसा का मूल है-राग-द्वेष। समता की भूमिका में ये समाप्त हो जाते हैं। जितना-जितना समता का विकास होता है, उतना-उतना राग-द्वेष का विनाश होता चला जाता है। महावीर का पूरा साधना-काल समता की साधना में बीता। उनके सामने अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के परिषह उत्पन्न हुए। उन्होंने अपनी सहिष्णुता के द्वारा उन परिषहों को निरस्त किया। उनकी समता की साधना थी–
लाभालाभे सुहे दुक्खे जीविए मरणे तहा।
समोनिंदा पसंसासु, तहा माणावमाणओ।।
लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, निन्दा-प्रशंसा तथा मान-अपमान के द्वन्द्वों में सम रहना।
आगम में कहा– ''सव्वे पाणा ण हंतव्वा, एस धम्मे धुए णिइए सासए।''
किसी प्राणी की हिंसा न करना, यह अहिंसा धर्म ही सबसे अधिक पुराना है, ध्रुव, नित्य और शाश्वत है।
महावीर की अहिंसा केवल उपदेशात्मक और शब्दात्मक नहीं हैं उन्होंने उस अहिंसा को जीया और फिर अनुभव की वाणी में दुनिया को उपदेश दिया। आज विश्व हिंसा की ज्वाला में झुलस रहा है। अहिंसा के शीतल सलिल से ही संसार को राहत मिल सकती है।
लक्ष्मण रेखाएं
भगवान महावीर ने दो प्रकार की साधना-पद्धति का निरूपण किया। वैयक्तिक और संघबद्ध । वैयक्तिक साधना दुष्कर होती है। इसलिए हर कोई साधक उसे स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो सकता। विशिष्ट ज्ञानवान व शक्ति-सम्पन्न साधक गुरु की अनुमति प्राप्त होने पर ही वैयक्तिक साधना पद्धति में प्रवेश कर सकता है। संघबद्ध साधना प्रणाली में विशिष्ट ज्ञानवत्ता का होना अनिवार्य नहीं है। सामान्य तत्ववेत्ता व्यक्ति भी संघीय साधना का पथ स्वीकार कर सकता है।
एकांकी साधना-पद्धति में व्यवस्थागत मर्यादाओं की अपेक्षा नहीं रहती। क्योंकि वहां साधक अकेला होता है, अपनी इच्छानुसार कर सकता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। संघीय साधना में साधनागत और व्यवस्थागत दोनों प्रकार की मर्यादाएं आवश्यक होती हैं। भगवान महावीर ने साधुओं के लिए पांच महाव्रतों की व्यवस्था दी और महाव्रतों की सुरक्षा के लिए आठ प्रवचन-माताओं का विधान किया। ये तेरह नियम साधुओं की मूल-भूत साधनागत मर्यादाएं हैं। इन मर्यादाओं का पालन करना दोनों साधना-पद्धतियों में समान रूप से अनिवार्य है।

