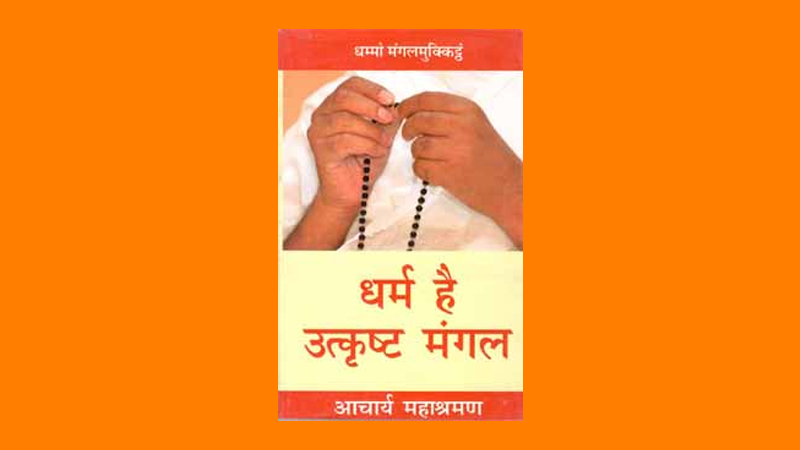
स्वाध्याय
धर्म है उत्कृष्ट मंगल
उनके प्रशस्त विवेक का प्रभाव उनकी चर्या पर पड़ा। उनकी चर्या भी प्रशस्त और विवेकपूर्ण थी। प्रशस्तता में विशवास होता है। उनका विश्वास जितना प्रत्यक्षतः फलित था उतना ही परोक्षतः भी फलित था। अतः उनके प्रति शिकायत का प्रायः कोई अवकाश ही नहीं था।
जब कालूगणी बालवय में थे। एक मुनि मघवागणी के पास आये और कहने लगा, 'मुनि कालू प्रतिलेखन में प्रमाद करता है।'
मघवागणी ने कहा, 'मैं इसे नहीं मान सकता। वह तुम्हारे से अच्छा प्रतिलेखन करता है क्योंकि वह सदा मेरे पास करता है और मैंने कई बार उसे प्रतिलेखन करते हुए देखा है।'
शिकायत करने वाला मुनि कुछ बोल नहीं सका और चला गया। वस्तुतः कालूगणी आत्मानुशासी थे। उनका आत्मानुशासन इतना प्रबल था कि प्रमाद उनसे दूर ही रहता था। ऐसी जागृत, अप्रमत्त, विवेकशील और परिपक्व पुण्यात्मा के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके गुणों को आत्मसात् करने का प्रयत्न करेंगे।
समाज-सुधार के सूत्रधर : गुरुदेव श्री तुलसी
हिन्दुस्तान की सन्त परमपरा गौरवपूर्ण एवं महिमामण्डित रही है। भारतीय संस्कृति में साधु-समाज को सम्मानपूर्ण स्थान मिला है। सन्त की मूलभूत पहचान है-पवित्रता। व्यवहार के दर्पण में पवित्रता को परखा जा सकता है। निम्नांकित संस्कृत श्लोक में मुनि के चार लक्षण प्रस्तुत है—
वदनं प्रसाद-सदनं, सदयं हृदयं सुधामुधो वाचः।
करणं परोपकरणं, येषां केषां नते वन्द्याः ।।
१. सहज प्रसन्नता
२. प्राणीमात्र के प्रति दयाभाव
३. अमृतमयी वाणी
४. परोपकारिता
भारत को वसुन्धरा ने अमूल्य सन्त-रत्नों को प्रसूत किया है। उन्होंने उपरिनिर्दिष्ट चार मूल्य-मानकों का उपदेश ही नहीं दिया, उन्हें आत्मसात् कर जीया है। समय-समय पर उन्होंने प्रशासक वर्ग का भी योग्य आध्यात्मिक नेतृत्व किया है। देश के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में उनका तपः-पूत दिशा-दर्शन और अविश्रान्त श्रम रहा है।
अणुव्रत अनुशास्ता पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। परमाराध्य गुरुप्रवर की पुनीत प्रज्ञा को हम अनेकानेक विशेषणों से विशिष्ट कर सकते हैं। उनके वर्चस्वी व्यक्तित्व को हम विविध भागों में विभक्त कर सकते हैं। उनके ऊर्जस्वल कर्तृत्व को विभिन्न उपमाओं से उपमित कर सकते हैं। गुरुवर की बहुमुखी क्रियाशीलता में समाज-सुधार का भी प्रमुख स्थान है। आध्यात्मिकता के अवतरण के लिए सामाजिक सुधार भी अत्यन्त आवश्यक है। धार्मिक और आध्यात्मिक कहलाने वाले समाज भी अगर अर्थशून्य रूढ़ियों और अन्धविश्वासों को पनपाते रहें तो उस समाज की आध्यात्मिकता और धर्म-परायणता प्रशनचिहांकित बन जाती है।
हिन्दुस्तान की धर्म-प्रधान धरती पर अनेक समाज-सुधारक महापुरुषों ने जन्म लिया है। उन्होंने अपने निष्णात चिन्तन के द्वारा मानव-जाति को अभिनव पथ प्रदान किया है। उन महान् विभूतियों की प्रलम्ब श्रृंखला में बीसवीं सदी के देदीप्यमान नक्षत्र, प्रसिद्ध जैनाचार्य तेरापंथ धर्म संघ के नवमाधिशास्ता स्वनाम धन्य गुरुदेव श्री तुलसी का नाम भी गौरव के साथ लिया जाता है।
हिन्दुस्तान आजाद हुआ, नेतागण ने देश के बहुमुखी विकास का स्वप्न ले रखा था। उसी समय भारत के महान् सन्त आचार्यश्री तुलसी के चिन्तन-क्षितिज पर एक विचार उभरा-यदि देश का चारित्रिक विकास और आध्यात्मिक शक्ति का संवर्धन, जो कि मूल प्राण है, नहीं हुआ तो अन्यान्य विकास-योजनाएं बहुत फलदायी नहीं होंगी। धर्म और अध्यात्म आत्मावलोकन का साधन और सुख-समाधि- पूर्वक जीवन-यापन का एक तरीका है। किन्तु बहुलांश धार्मिक वर्ग ने धर्म के क्रियाकाण्डात्मक और उपासनापरक पक्ष को दृढ़ता से पकड़ा उसके आचरणात्मक पक्ष का समुचित मूल्यांकन नहीं किया। फलस्वरूप धार्मिक का जीवन भी हिंसा, क्रूरता, धोखाधड़ी आदि अनैतिक आचरणों से अछूता नहीं रहा। धर्म तथा धार्मिक की इस करुणदशा से पूज्य गुरुदेव का सदय हृदय द्रवित हो उठा। एक धर्म-क्रान्ति की अपेक्षा अनुभूत हुई। देश के चारित्रिक विकास और धर्म-क्रान्ति की समुत्कण्ट ने २ मार्च, १९४९ को एक व्यापक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वह अणुव्रत आन्दोलन के नाम से विख्यात हुआ।

