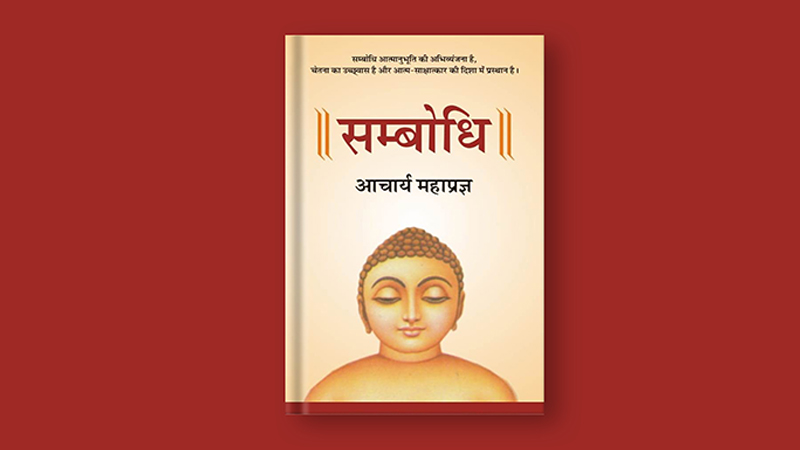
स्वाध्याय
संबोधि
रस वस्तुओं में नहीं है, किन्तु वस्तुएं रस का निमित्त बनती हैं, इसलिए रस को बाह्य तप में रखा है। साधना की पूर्व-भूमिका में रस-विजय की अपेक्षा है। साधना की प्रखरता, उच्च भूमिका तथा सिद्धि के पश्चात् उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जहां कामना-वासना ही शान्त हो जाती है वहां फिर वस्तुओं का क्या महत्त्व रहता है? वस्तुओं में जहां से रस अभिव्यक्त होता है, जीतना उसे है। जैसे बाहर रस है वैसे भीतर भी रस है। बुद्ध ने कहा-अमृत बरस रहा है। कबीर कहते हैं- 'इस गगन गुफा में अजर झरै', क्या यह बाहर दिखाई दे रहा है? यह किसी दूसरी दुनिया की झलक है। वह सबसे भीतर है। उसे पाना है। उसके सामने पदार्थों के रस स्वतः तुच्छ हो जाते हैं। गीता में कहा है- 'रसवर्ज रसोप्यस्य, परं दृष्ट्वा निवर्तत'- परम तत्व के दर्शन का रसास्वादन कर लेने के बाद अन्य रसों से साधक निवृत्त हो जाता है।
रस-विजय के लिए रस के केन्द्र पर ध्यान देना चाहिए। इन्द्रियां सिर्फ संवाद सम्प्रेषण करती हैं। वे संवाद मस्तिष्क में पहुंचते हैं। मस्तिष्क का संबंध किसी अन्य से है। फिर उनमें प्रियता और अप्रियता का भाव प्रकट होता है। जैसा है वैसा जान लेना, प्रिय में राग नहीं करना और अप्रिय से घृणा नहीं करना, सिर्फ शांत होकर देखते रहना, जो-जो तरंगें उठत्ती हैं, उनके उठने और गिरने को बस, देखना है। मन का योग विषयों से नहीं जोड़ना है, किन्तु उसे देखने वाले (द्रष्टा) के साथ जोड़ना है। द्रष्टा की घनीभूत अवस्था में रसों की अनुभूति का महत्त्व नहीं रहता।
रस का अनुभव क्षणिक है, किन्तु उसकी स्मृतियां व्यक्ति को दीर्घकाल तक सताती रहती हैं। कण्ठ से नीचे उतरने के बाद सब कुछ भोजन मिट्टी हो जाता है, इसे सिर्फ दोहराने या कथन करने से नहीं, अपितु प्रत्यक्ष अनुभव में उतारना है। जिस दिन यह सत्यता स्पष्ट हो जाती है, उस दिन केवल जीवन-निर्वाह के लिए भोजन रह जाता है। साधक ध्येय को सतत अविस्मृत रखते हुए पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को देखे।
(5) कायक्लेश
इसका सीधा सरल अर्थ है-काया-कष्ट । मन शरीर का ही सूक्ष्म अंश है। जितने कष्ट उत्पन्न होते हैं सब काया में होते हैं। उत्पत्ति कष्ट है। उसके पीछे मृत्यु संलग्न है। जो पैदा होता है, वह मरणधर्मा है। हिमालय पर शिवजी के सामने अचानक कोई धमाका हुआ, तब सामने स्थित नन्दी ने पूछा- 'भगवन्!' यह किसकी ध्वनि हुई?

