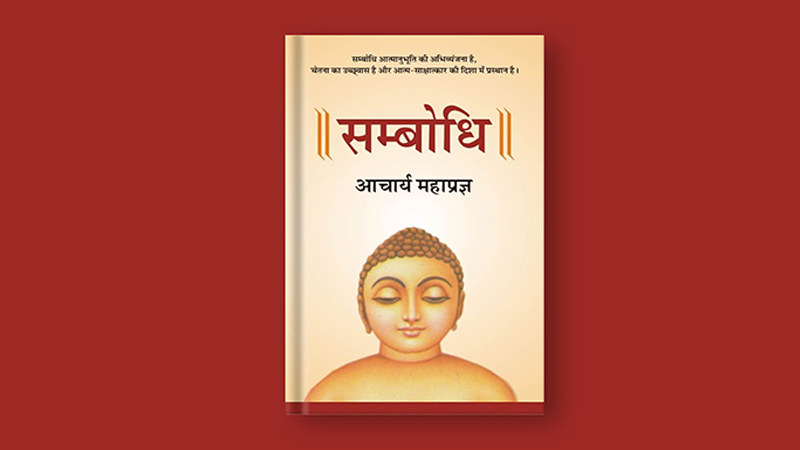
स्वाध्याय
संबोधि
संबोधि
आचार्य महाप्रज्ञ
बंध-मोक्षवाद
मिथ्या-सम्यग्-ज्ञान-मीमांसा
भगवान् प्राह
(53) यदा लोकमलोकं च, जिनो जानाति केवली।
आयुषोऽन्ते निरुन्धानः, योगान् कृत्वा रजः क्षयम्।।
(54) अनन्तामचलां पुण्यां, सिद्धिं गच्छति नीरजाः।
तदा लोकमस्तकस्थः, सिद्धो भवति शाश्वतः।। (युग्मम्)
(पिछला शेष) जीव और अजीव के बोध से ही जीवों की विविध गतियों का बोध होता है। कौन जीव कहाँ जाता है? कैसे जाता है? क्यों जाता है? तिर्यंच गति, मनुष्य गति, नरक गति और देव गति के निमित्त क्या-क्या बनते हैं? इसके बोध से पुण्य और पाप का ज्ञान होता है। पुण्य शुभ कर्म है और पाप अशुभ कर्म। पुण्य व्यक्ति को उत्कर्ष के पथ पर ले जाता है और पाप अपकर्ष के पथ पर। पुण्य की महिमा से मंडित व्यक्ति पूज्य, आदेय, श्लाघ्य, कीर्तिमान बनता है और पापोदय के कारण हीन, अश्लाघ्य आदि। ऐसे अनेक अभिनयों के पीछे पुण्य-पाप की छाया है। पुण्य और पाप के साथ उसके बंधन और मुक्ति की क्रिया भी जुड़ी है। जब संसार की विचित्रता सामने आती है तब मन सहज ही सांसारिक विषय-भोगों से उद्विग्न हो जाता है, भोगों से विरक्ति हो जाती है। भोग सिर्फ रोग ही नहीं देते हैं अपितु दुःख भी देते हैं। मन की विरक्त दशा में सभी प्रकार के मानवीय, दैवीय भोग क्षुद्रतम प्रतीत होने लगते हैं। बारह से वितृष्ण मन अंतरंग सुख में निमग्न होने लगता है। सांसारिक संबंध भी मिथ्या दिखाई देने लगते हैं। मन संयोगों से मुक्त होने के लिए तरसने लगता है। जब तक संयोगों के प्रति चित्त आकृष्ट रहता है तब तक परमतत्त्व से भी प्रीति नहीं होती। बाहर का राग भीतर से विराग पैदा करता है और भीतर का राग बाहर से विराग पैदा करता है।
संसार संयोगों की देन है। संयोग कर्म हेतुक हैं। कर्म से पुनः कर्म का ही अनुबंध होता है। कर्म आंतरिक संयोग है। आंतरिक संयोगों के बने रहने पर बाह्य संयोगों के त्याग का वास्तविक अर्थ नहीं रहता। वस्तुतः आंतरिक संयोगों को ही त्यागना है। अन्यथा त्याग कर भी कुछ नहीं त्यागा जाता है। मन ममत्व की परिक्रमा करता ही रहता है। इसे सम्यक् समझकर ही साधक बाह्य और आभ्यंतरिक दोनों संयोगों से मुक्त होने के लिए तत्पर होता है। यह संयोग-मुक्ति का संकल्प उसे मुनिपद पर आरूढ़ करता है। वह सबको संन्यास दे देता है। सही माने में अनगारता राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह आदि वृत्तियों व बाह्य रूप से सांसारिक वृत्तियों के परित्याग से ही सिद्ध होती है। संन्यस्त व्यक्तिµमुनि ही संवर धर्म का स्पर्श करता है।
संवर विजातीय तत्त्व का अवरोधक है। आत्मा के असंख्य द्वार खुले हैं, जिनसे सतत कर्म तत्त्व का प्रवाह गतिमान रहता है। कर्म पौद्गलिकµविजातीय हैं। जब तक इसके द्वार को रोकाµबंद नहीं किया जाता है तब तक आत्मा का भव-भ्रमण चलता रहता है। जब साधक आत्मा के साथ एकत्व स्थापित करने लगता है, एकत्व घनीभूत होने लगता है तब उत्कृष्ट संवर की आराधना प्रारंभ हो जाती है। खुले हुए द्वार सहज ही अवरुद्ध होने लगते हैं, फलतः अबोधि-अज्ञान द्वारा अर्जित अनंत जन्मों के कलुषित कर्म प्रकंपित होने लगते हैं। पंछी जैसे अपने शरीर पर लगे रजकणों को पंखों को फड़फड़ाकर झटका देता है, वैसे ही साधना के द्वारा साधक के कर्म रज प्रकंपित होकर आत्मा से विलग हो जाते हैं। कर्मों का अलगाव ही आत्मा के सौंदर्य को प्रकट कर देता है। अनंत जन्मों का तम प्रकाश की एक किरण से विलीन हो जाता है। कर्म के क्षीण होते ही ज्ञान-दर्शन जो आत्मा का स्वभाव है वह व्यक्त हो जाता है। यह ज्ञान शास्त्रीयµबौद्धिक ज्ञान से भिन्न है। इसमें किसी माध्यम की अपेक्षा नहीं रहती है, न इसमें निकटता या दूरी का व्यवधान रहता है। यह ज्ञान अमर्यादित-असीम होता है, विश्व-लोक के इस छोर और उस छोर की परिधि भी वहाँ नहीं रहती। वस्तु के अनंत धर्मों का अवलोकन अविलंब हो जाता है। इसे केवलज्ञान कहते हैं। यही कैवल्य अवस्था है। ज्ञान और दर्शनµये दो शब्द सिर्फ वस्तु के बोध की अवस्था मात्र है। दर्शन में वस्तु का सामान्य बोध होता है और ज्ञान में वस्तु का अनंत धर्मों-पहलुओं का ज्ञान होता है। एक सामान्य जानकारी देता है और एक विशिष्ट। इस ज्ञान के अधिकारी व्यक्ति को जिनµकेवली कहते हैं। लोक व अलोक के दर्शन में केवली ही सक्षम होते हैं।
(क्रमशः)

